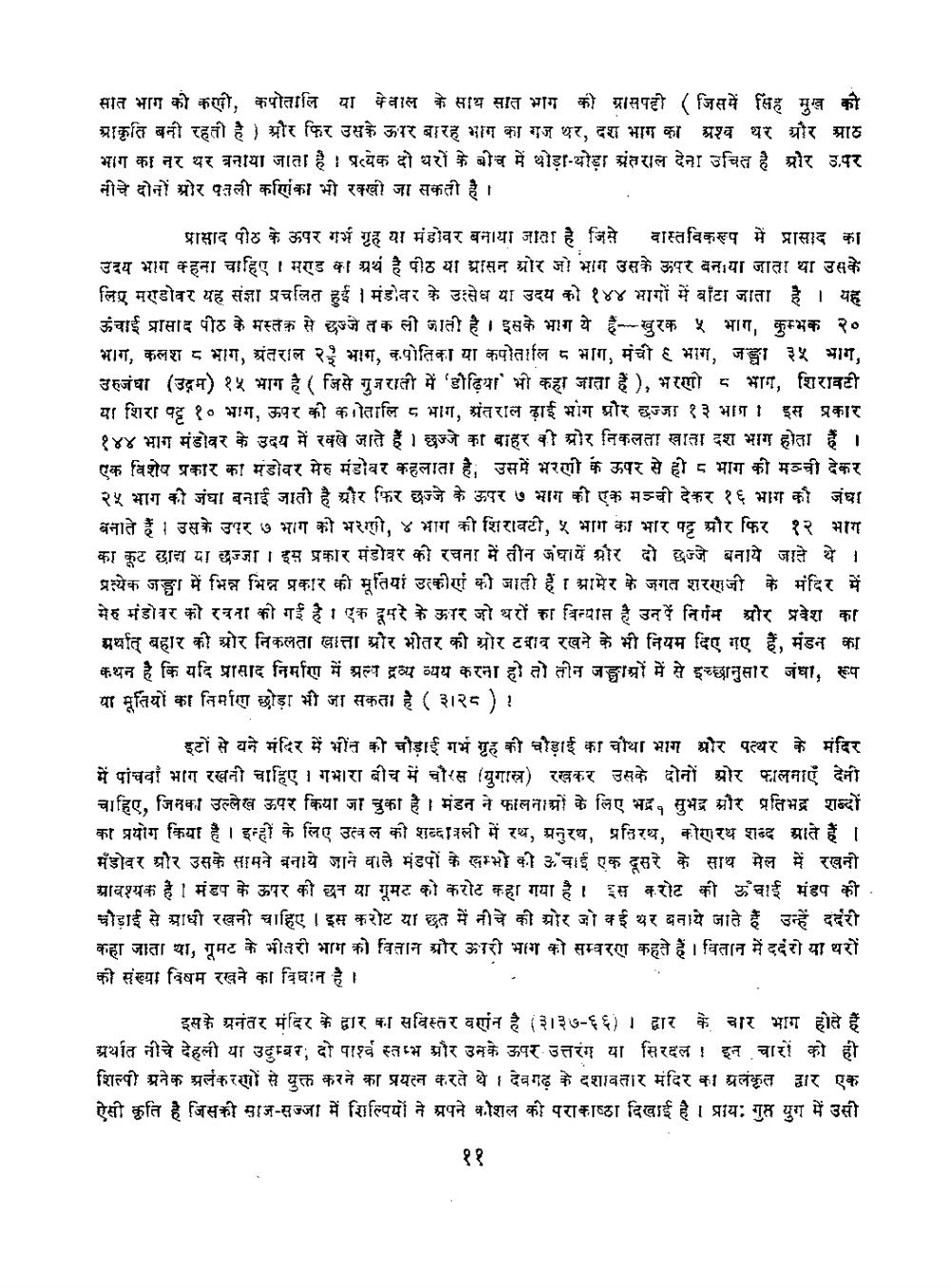________________
सात भाग को कपी, कपोतालि या केवाल के साथ सात भाग को ग्रासपही ( जिसमें सिंह मुख को प्राकृति बनी रहती है । और फिर उसके ऊपर बारह भाग का गज थर, दश भाग का अश्व थर और पाठ भाग का नर थर बनाया जाता है। प्रत्येक दो घरों के बीच में थोड़ा-थोड़ा अंतराल देना उचित है और उ.पर नीचे दोनों ओर पतली कर्णिका भी रक्खी जा सकती है ।
प्रासाद पीठ के ऊपर गर्भ गृह या महोवर बनाया जाता है जिसे वास्तविकरूप में प्रासाद का उदय भाग कहना चाहिए । मण्ड का अर्थ है पीठ या प्रासन और जो भाग उसके ऊपर बनाया जाता था उसके लिए मएडोवर यह संज्ञा प्रचलित हुई । मंडोवर के उत्सेध या उदय को १४४ भागों में बाँटा जाता है । यह ऊंचाई प्रासाद पीठ के मस्तक से छज्जे तक ली जाती है। इसके भाग ये हैं...-खुरक ५ भाग, कुम्भक २० भाग, कलश ८ भाग, अंतराल २३ भाग, क.पोतिका या कपोतालि ८ भाग, मंची ६ भाग, जङ्घा ३५ भाग, उरुजंघा (उद्गम) १५ भाग है ( जिसे गुजराती में 'डोढ़िया' भी कहा जाता है), भरणो ८ भाग, शिरावटी या शिरा पट्ट १० भाग, ऊपर की कोतालि ८ भाग, अंतराल ढ़ाई भोग और छज्जा १३ भाग। इस प्रकार १४४ भाग मंडोवर के उदय में रक्खे जाते हैं। छज्जे का बाहर की ओर निकलता खाता दश भाग होता हैं । एक विशेष प्रकार का मंडोवर मेरु मंडोवर कहलाता है। उसमें भरणी के ऊपर से ही ८ भाग की मची देकर २५ भाग की जंघा बनाई जाती है और फिर छज्जे के ऊपर ७ भाग की एक मञ्ची देकर १६ भाग को जंघा बनाते हैं। उसके उपर ७ भाग को भरगी, ४ भाग की शिरावटी, ५ भाग का भार पट्ट और फिर १२ भाग का कूट छाद्य या छज्जा । इस प्रकार मंडोवर की रचना में तीन जंघायें और दो छज्जे बनाये जाते थे । प्रत्येक जड़ा में भिन्न भिन्न प्रकार की मूर्तियां उत्कीरणं की जाती हैं । आमेर के जगत शरण जी के मंदिर में मेरु मंडोवर को रचना की गई है। एक दूसरे के कार जो थरों का विन्यास है उनमें निर्गम और प्रवेश का मर्थात् बहार की ओर निकलता खात्ता और भीतर की ओर दबाव रखने के भी नियम दिए गए हैं, मंडन का कथन है कि यदि प्रासाद निर्माण में अल्प द्रव्य व्यय करना हो तो तीन जडानों में से इच्छानुसार जंधा, रूप या मूर्तियों का निर्माता छोड़ा भी जा सकता है ( ३।२८)!
इटों से बने मंदिर में भींत को चौड़ाई गर्भ गृह की चौड़ाई का चौथा भाग और पत्थर के मंदिर में पांचवा भाग रखनी चाहिए। गमारा बीच में चौरस (युगात्र) रखकर उसके दोनों ओर फालनाएं देनी चाहिए, जिनका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। मंडन ने फालनामों के लिए भद्र, सुभद्र और प्रतिभद्र शब्दों का प्रयोग किया है । इन्हीं के लिए उत्कल की शब्दावली में रथ, अनुरथ, प्रतिरथ, कोण रथ शब्द प्राते हैं । मँडोवर और उसके सामने बनाये जाने वाले मंडपों के खम्भो की ऊँचाई एक दूसरे के साथ मेल में रखनी प्रावश्यक है। मंडप के ऊपर की छत या गूमर को करोट कहा गया है। इस करोट की ऊंचाई मंडप की . चौड़ाई से प्राधी रखनी चाहिए । इस करोट या छत में नीचे की ओर जो कई थर बनाये जाते हैं उन्हें दर्दरी कहा जाता था, गुमट के भीतरी भाग को वितान और ऊपरी भाग को सम्बरण कहते हैं । वितान में दर्दरो या थरों की संख्या विषम रखने का विधान है।
इसके अनंतर मंदिर के द्वार का सविस्तर वर्णन है।३।३७-६६) । द्वार के चार भाग होते हैं अर्थात नीचे देहली या उदुम्बर; दोपार्श्व स्तम्भ और उनके ऊपर उत्तरंग या सिरदल। इन चारों को ही शिल्पी अनेक अलंकरणों से युक्त करने का प्रयत्न करते थे। देवगढ़ के दशावतार मंदिर का अलंकृत द्वार एक ऐसी कृति है जिसकी साज-सज्जा में शिल्पियों ने अपने कौशल की पराकाष्ठा दिखाई है। प्रायः गुप्त युग में उसी