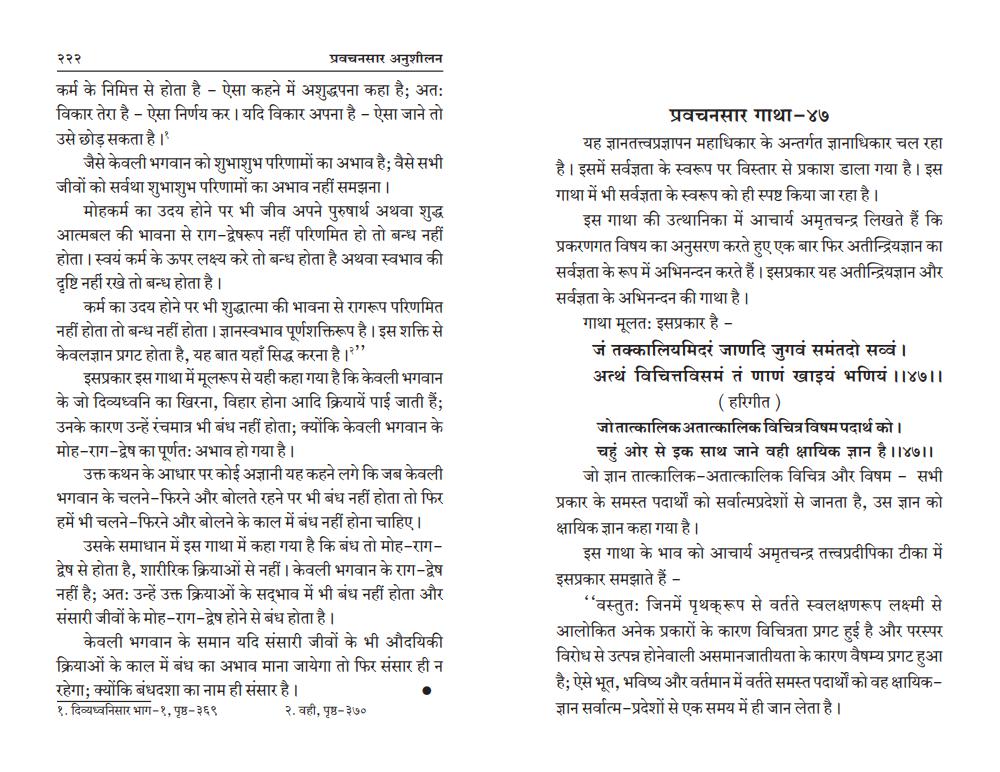________________
२२२
प्रवचनसार अनुशीलन कर्म के निमित्त से होता है - ऐसा कहने में अशुद्धपना कहा है; अत: विकार तेरा है - ऐसा निर्णय कर । यदि विकार अपना है - ऐसा जाने तो उसे छोड़ सकता है।
जैसे केवली भगवान को शुभाशुभ परिणामों का अभाव है; वैसे सभी जीवों को सर्वथा शुभाशुभ परिणामों का अभाव नहीं समझना। ___ मोहकर्म का उदय होने पर भी जीव अपने पुरुषार्थ अथवा शुद्ध
आत्मबल की भावना से राग-द्वेषरूप नहीं परिणमित हो तो बन्ध नहीं होता । स्वयं कर्म के ऊपर लक्ष्य करे तो बन्ध होता है अथवा स्वभाव की दृष्टि नहीं रखे तो बन्ध होता है। ___ कर्म का उदय होने पर भी शुद्धात्मा की भावना से रागरूप परिणमित नहीं होता तो बन्ध नहीं होता । ज्ञानस्वभाव पूर्णशक्तिरूप है। इस शक्ति से केवलज्ञान प्रगट होता है, यह बात यहाँ सिद्ध करना है।"
इसप्रकार इस गाथा में मूलरूपसे यही कहा गया है कि केवली भगवान के जो दिव्यध्वनि का खिरना, विहार होना आदि क्रियायें पाई जाती हैं; उनके कारण उन्हें रंचमात्र भी बंध नहीं होता; क्योंकि केवली भगवान के मोह-राग-द्वेष का पूर्णत: अभाव हो गया है।
उक्त कथन के आधार पर कोई अज्ञानी यह कहने लगे कि जब केवली भगवान के चलने-फिरने और बोलते रहने पर भी बंध नहीं होता तो फिर हमें भी चलने-फिरने और बोलने के काल में बंध नहीं होना चाहिए।
उसके समाधान में इस गाथा में कहा गया है कि बंध तो मोह-रागद्वेष से होता है, शारीरिक क्रियाओं से नहीं । केवली भगवान के राग-द्वेष नहीं है; अत: उन्हें उक्त क्रियाओं के सदभाव में भी बंध नहीं होता और संसारी जीवों के मोह-राग-द्वेष होने से बंध होता है।
केवली भगवान के समान यदि संसारी जीवों के भी औदयिकी क्रियाओं के काल में बंध का अभाव माना जायेगा तो फिर संसार ही न रहेगा; क्योंकि बंधदशा का नाम ही संसार है। १. दिव्यध्वनिसार भाग-१, पृष्ठ-३६९ २. वही, पृष्ठ-३७०
प्रवचनसार गाथा-४७ यह ज्ञानतत्त्वप्रज्ञापन महाधिकार के अन्तर्गत ज्ञानाधिकार चल रहा है। इसमें सर्वज्ञता के स्वरूप पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है। इस गाथा में भी सर्वज्ञता के स्वरूप को ही स्पष्ट किया जा रहा है।
इस गाथा की उत्थानिका में आचार्य अमृतचन्द्र लिखते हैं कि प्रकरणगत विषय का अनुसरण करते हुए एक बार फिर अतीन्द्रियज्ञान का सर्वज्ञता के रूप में अभिनन्दन करते हैं। इसप्रकार यह अतीन्द्रियज्ञान और सर्वज्ञता के अभिनन्दन की गाथा है। गाथा मूलत: इसप्रकार हैजं तक्कालियमिदरं जाणदि जुगवं समंतदो सव्वं । अत्थं विचित्तविसमं तं णाणं खाइयं भणियं ।।४७।।
(हरिगीत) जोतात्कालिक अतात्कालिक विचित्र विषम पदार्थ को। चहुं ओर से इक साथ जाने वही क्षायिक ज्ञान है ।।४७।।
जो ज्ञान तात्कालिक-अतात्कालिक विचित्र और विषम - सभी प्रकार के समस्त पदार्थों को सर्वात्मप्रदेशों से जानता है, उस ज्ञान को क्षायिक ज्ञान कहा गया है।
इस गाथा के भाव को आचार्य अमृतचन्द्र तत्त्वप्रदीपिका टीका में इसप्रकार समझाते हैं -
"वस्तुत: जिनमें पृथक्प से वर्तते स्वलक्षणरूप लक्ष्मी से आलोकित अनेक प्रकारों के कारण विचित्रता प्रगट हुई है और परस्पर विरोध से उत्पन्न होनेवाली असमानजातीयता के कारण वैषम्य प्रगट हुआ है; ऐसे भूत, भविष्य और वर्तमान में वर्तते समस्त पदार्थों को वह क्षायिकज्ञान सर्वात्म-प्रदेशों से एक समय में ही जान लेता है।