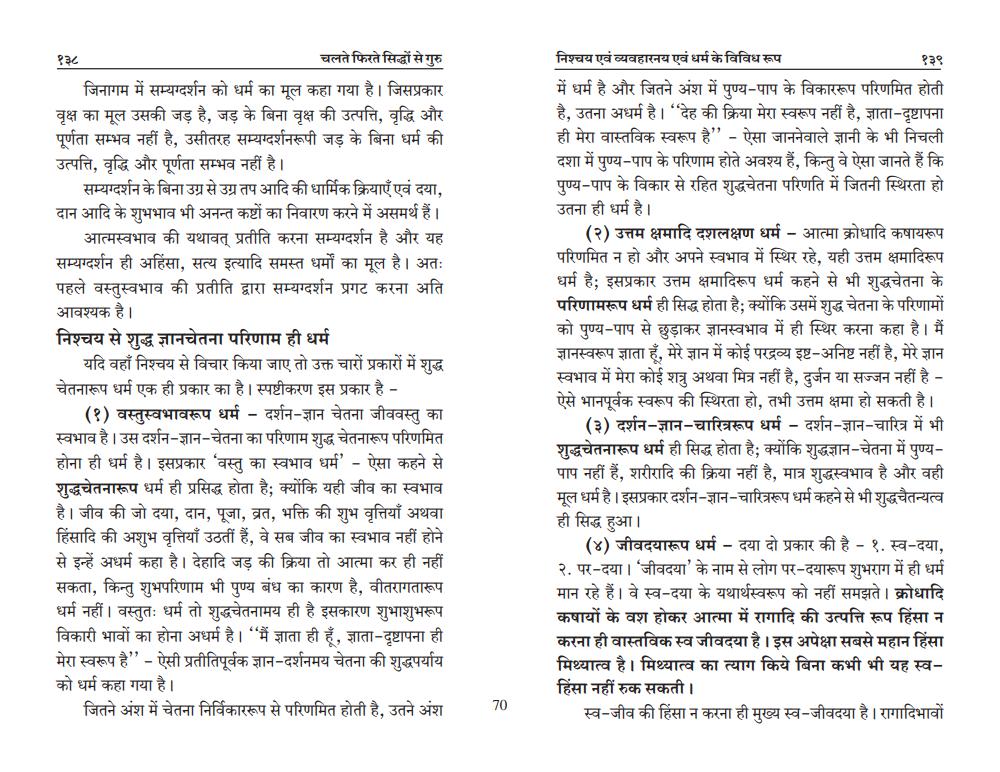________________
१३८
चलते फिरते सिद्धों से गुरु जिनागम में सम्यग्दर्शन को धर्म का मूल कहा गया है। जिसप्रकार वृक्ष का मूल उसकी जड़ है, जड़ के बिना वृक्ष की उत्पत्ति, वृद्धि और पूर्णता सम्भव नहीं है, उसीतरह सम्यग्दर्शनरूपी जड़ के बिना धर्म की उत्पत्ति, वृद्धि और पूर्णता सम्भव नहीं है।
सम्यग्दर्शन के बिना उग्र से उग्र तप आदि की धार्मिक क्रियाएँ एवं दया, दान आदि के शुभभाव भी अनन्त कष्टों का निवारण करने में असमर्थ हैं।
आत्मस्वभाव की यथावत् प्रतीति करना सम्यग्दर्शन है और यह सम्यग्दर्शन ही अहिंसा, सत्य इत्यादि समस्त धर्मों का मूल है। अत: पहले वस्तुस्वभाव की प्रतीति द्वारा सम्यग्दर्शन प्रगट करना अति
आवश्यक है। निश्चय से शुद्ध ज्ञानचेतना परिणाम ही धर्म
यदि वहाँ निश्चय से विचार किया जाए तो उक्त चारों प्रकारों में शुद्ध चेतनारूप धर्म एक ही प्रकार का है। स्पष्टीकरण इस प्रकार है -
(१) वस्तुस्वभावरूप धर्म - दर्शन-ज्ञान चेतना जीववस्तु का स्वभाव है। उस दर्शन-ज्ञान-चेतना का परिणाम शुद्ध चेतनारूप परिणमित होना ही धर्म है। इसप्रकार 'वस्तु का स्वभाव धर्म' - ऐसा कहने से शुद्धचेतनारूप धर्म ही प्रसिद्ध होता है; क्योंकि यही जीव का स्वभाव है। जीव की जो दया, दान, पूजा, व्रत, भक्ति की शुभ वृत्तियाँ अथवा हिंसादि की अशुभ वृत्तियाँ उठतीं हैं, वे सब जीव का स्वभाव नहीं होने से इन्हें अधर्म कहा है। देहादि जड़ की क्रिया तो आत्मा कर ही नहीं सकता, किन्तु शुभपरिणाम भी पुण्य बंध का कारण है, वीतरागतारूप धर्म नहीं। वस्तुतः धर्म तो शुद्धचेतनामय ही है इसकारण शुभाशुभरूप विकारी भावों का होना अधर्म है। “मैं ज्ञाता ही हूँ, ज्ञाता-दृष्टापना ही मेरा स्वरूप है" - ऐसी प्रतीतिपूर्वक ज्ञान-दर्शनमय चेतना की शुद्धपर्याय को धर्म कहा गया है।
जितने अंश में चेतना निर्विकाररूप से परिणमित होती है, उतने अंश
निश्चय एवं व्यवहारनय एवं धर्म के विविध रूप
१३९ में धर्म है और जितने अंश में पुण्य-पाप के विकाररूप परिणमित होती है, उतना अधर्म है। “देह की क्रिया मेरा स्वरूप नहीं है, ज्ञाता-दृष्टापना ही मेरा वास्तविक स्वरूप है" - ऐसा जाननेवाले ज्ञानी के भी निचली दशा में पुण्य-पाप के परिणाम होते अवश्य हैं, किन्तु वे ऐसा जानते हैं कि पुण्य-पाप के विकार से रहित शुद्धचेतना परिणति में जितनी स्थिरता हो उतना ही धर्म है।
(२) उत्तम क्षमादि दशलक्षण धर्म - आत्मा क्रोधादि कषायरूप परिणमित न हो और अपने स्वभाव में स्थिर रहे, यही उत्तम क्षमादिरूप धर्म है; इसप्रकार उत्तम क्षमादिरूप धर्म कहने से भी शुद्धचेतना के परिणामरूप धर्म ही सिद्ध होता है; क्योंकि उसमें शुद्ध चेतना के परिणामों को पुण्य-पाप से छुड़ाकर ज्ञानस्वभाव में ही स्थिर करना कहा है। मैं ज्ञानस्वरूप ज्ञाता हूँ, मेरे ज्ञान में कोई परद्रव्य इष्ट-अनिष्ट नहीं है, मेरे ज्ञान स्वभाव में मेरा कोई शत्रु अथवा मित्र नहीं है, दुर्जन या सज्जन नहीं है - ऐसे भानपूर्वक स्वरूप की स्थिरता हो, तभी उत्तम क्षमा हो सकती है।
(३) दर्शन-ज्ञान-चारित्ररूप धर्म - दर्शन-ज्ञान-चारित्र में भी शुद्धचेतनारूप धर्म ही सिद्ध होता है; क्योंकि शुद्धज्ञान-चेतना में पुण्यपाप नहीं हैं, शरीरादि की क्रिया नहीं है, मात्र शुद्धस्वभाव है और वही मूल धर्म है। इसप्रकार दर्शन-ज्ञान-चारित्ररूप धर्म कहने से भी शुद्धचैतन्यत्व ही सिद्ध हुआ।
(४) जीवदयारूप धर्म - दया दो प्रकार की है - १. स्व-दया, २. पर-दया। 'जीवदया' के नाम से लोग पर-दयारूप शुभराग में ही धर्म मान रहे हैं। वे स्व-दया के यथार्थस्वरूप को नहीं समझते। क्रोधादि कषायों के वश होकर आत्मा में रागादि की उत्पत्ति रूप हिंसा न करना ही वास्तविक स्व जीवदया है । इस अपेक्षा सबसे महान हिंसा मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व का त्याग किये बिना कभी भी यह स्वहिंसा नहीं रुक सकती। __स्व-जीव की हिंसा न करना ही मुख्य स्व-जीवदया है। रागादिभावों
70