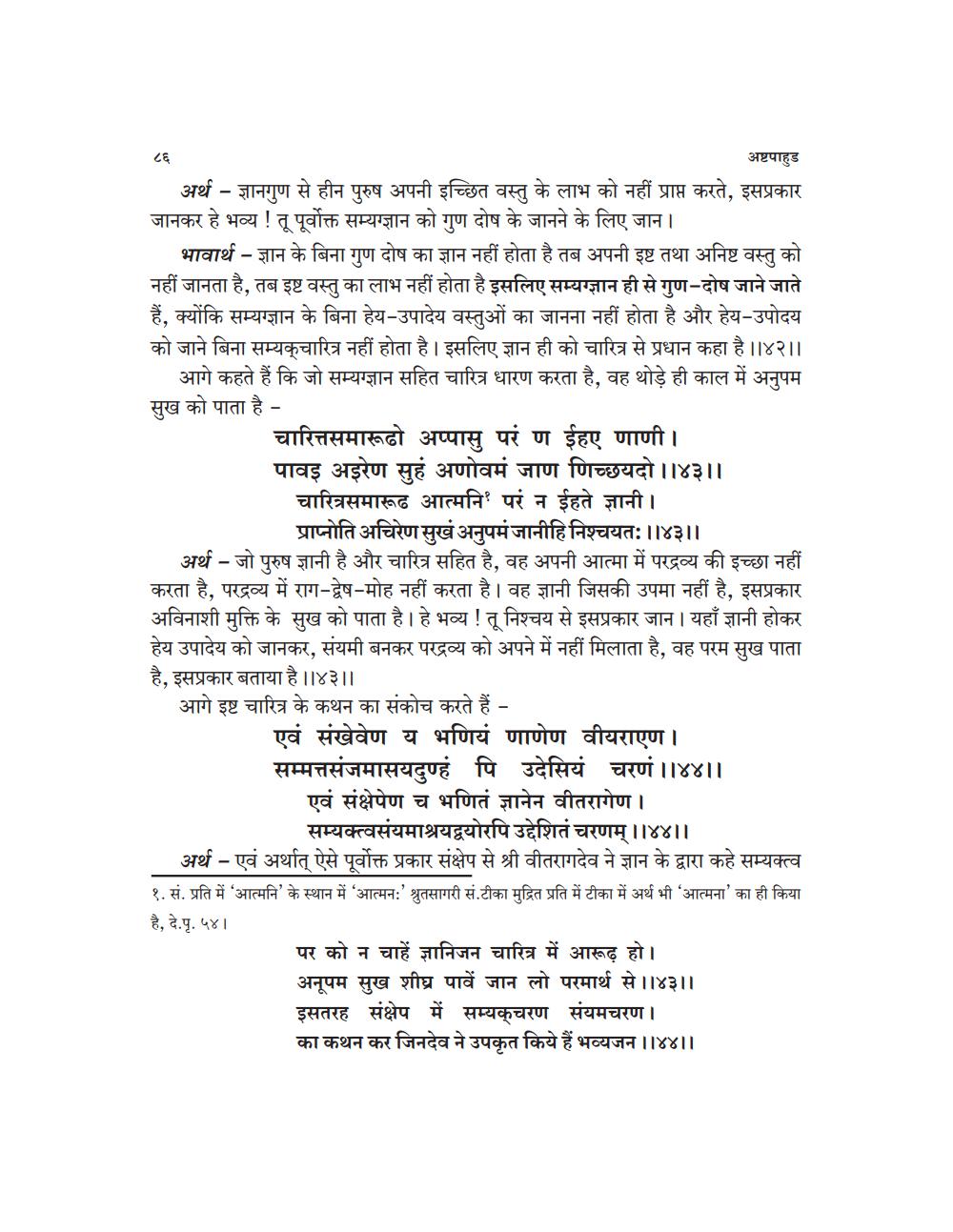________________
अष्टपाहुड अर्थ – ज्ञानगुण से हीन पुरुष अपनी इच्छित वस्तु के लाभ को नहीं प्राप्त करते, इसप्रकार जानकर हे भव्य ! तु पूर्वोक्त सम्यग्ज्ञान को गुण दोष के जानने के लिए जान।
भावार्थ - ज्ञान के बिना गुण दोष का ज्ञान नहीं होता है तब अपनी इष्ट तथा अनिष्ट वस्तु को नहीं जानता है, तब इष्ट वस्तु का लाभ नहीं होता है इसलिए सम्यग्ज्ञान ही से गुण-दोष जाने जाते हैं, क्योंकि सम्यग्ज्ञान के बिना हेय-उपादेय वस्तुओं का जानना नहीं होता है और हेय-उपोदय को जाने बिना सम्यक्चारित्र नहीं होता है। इसलिए ज्ञान ही को चारित्र से प्रधान कहा है ।।४२।।
आगे कहते हैं कि जो सम्यग्ज्ञान सहित चारित्र धारण करता है, वह थोड़े ही काल में अनुपम सुख को पाता है -
चारित्तसमारूढो अप्पासु परं ण ईहए णाणी। पावइ अइरेण सुहं अणोवमं जाण णिच्छयदो।।४३।।
चारित्रसमारूढ आत्मनि' परं न ईहते ज्ञानी।
प्राप्नोति अचिरेण सुखं अनुपमंजानीहि निश्चयतः।।४३।। अर्थ - जो पुरुष ज्ञानी है और चारित्र सहित है, वह अपनी आत्मा में परद्रव्य की इच्छा नहीं करता है, परद्रव्य में राग-द्वेष-मोह नहीं करता है। वह ज्ञानी जिसकी उपमा नहीं है, इसप्रकार अविनाशी मुक्ति के सुख को पाता है। हे भव्य ! तू निश्चय से इसप्रकार जान । यहाँ ज्ञानी होकर हेय उपादेय को जानकर, संयमी बनकर परद्रव्य को अपने में नहीं मिलाता है, वह परम सुख पाता है, इसप्रकार बताया है ।।४३।। आगे इष्ट चारित्र के कथन का संकोच करते हैं -
एवं संखेवेण य भणियं णाणेण वीयराएण। सम्मत्तसंजमासयदुण्हं पि उदेसियं चरणं ।।४४।।
एवं संक्षेपेण च भणितं जानेन वीतरागेण।
सम्यक्त्वसंयमाश्रयद्वयोरपि उद्देशितं चरणम् ।।४४।। अर्थ – एवं अर्थात् ऐसे पूर्वोक्त प्रकार संक्षेप से श्री वीतरागदेव ने ज्ञान के द्वारा कहे सम्यक्त्व १. सं. प्रति में 'आत्मनि' के स्थान में आत्मनः' श्रुतसागरी सं.टीका मुद्रित प्रति में टीका में अर्थ भी ‘आत्मना' का ही किया है, दे.पृ. ५४।
पर को न चाहें ज्ञानिजन चारित्र में आरूढ हो। अनूपम सुख शीघ्र पावें जान लो परमार्थ से ।।४३।। इसतरह संक्षेप में सम्यक्चरण संयमचरण । का कथन कर जिनदेव ने उपकत किये हैं भव्यजन ।।४४।।