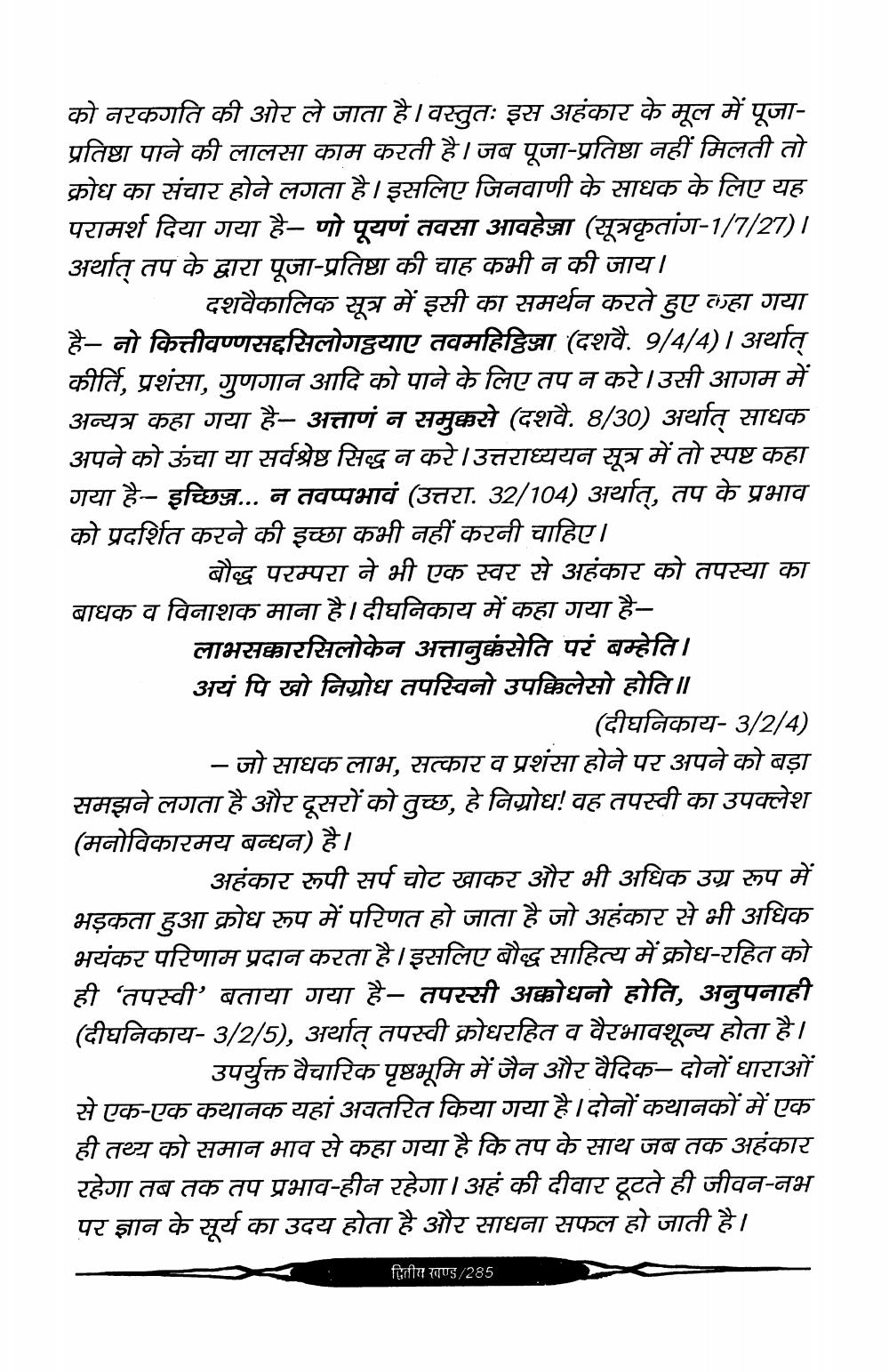________________
को नरकगति की ओर ले जाता है। वस्तुतः इस अहंकार के मूल में पूजाप्रतिष्ठा पाने की लालसा काम करती है। जब पूजा-प्रतिष्ठा नहीं मिलती तो क्रोध का संचार होने लगता है। इसलिए जिनवाणी के साधक के लिए यह परामर्श दिया गया है- णो पूयणं तवसा आवहेज्जा (सूत्रकृतांग-1/7/27)। अर्थात् तप के द्वारा पूजा-प्रतिष्ठा की चाह कभी न की जाय।
दशवैकालिक सूत्र में इसी का समर्थन करते हुए कहा गया है- नो कित्तीवण्णसहसिलोगट्टयाए तवमहिट्ठिजा (दशवै. 9/4/4)। अर्थात् कीर्ति, प्रशंसा, गुणगान आदि को पाने के लिए तप न करे। उसी आगम में अन्यत्र कहा गया है- अत्ताणं न समुक्कसे (दशवै. 8/30) अर्थात् साधक अपने को ऊंचा या सर्वश्रेष्ठ सिद्ध न करे । उत्तराध्ययन सूत्र में तो स्पष्ट कहा गया है- इच्छिज्ज... न तवप्पभावं (उत्तरा. 32/104) अर्थात्, तप के प्रभाव को प्रदर्शित करने की इच्छा कभी नहीं करनी चाहिए।
बौद्ध परम्परा ने भी एक स्वर से अहंकार को तपस्या का बाधक व विनाशक माना है। दीघनिकाय में कहा गया है
लाभसक्कारसिलोकेन अत्तानक्कंसेति परं बम्हेति। अयं पि खो निग्रोध तपस्विनो उपक्किलेसो होति॥
(दीघनिकाय-3/2/4) - जो साधक लाभ, सत्कार व प्रशंसा होने पर अपने को बड़ा समझने लगता है और दूसरों को तुच्छ, हे निग्रोध! वह तपस्वी का उपक्लेश (मनोविकारमय बन्धन) है।
अहंकार रूपी सर्प चोट खाकर और भी अधिक उग्र रूप में भड़कता हुआ क्रोध रूप में परिणत हो जाता है जो अहंकार से भी अधिक भयंकर परिणाम प्रदान करता है। इसलिए बौद्ध साहित्य में क्रोध-रहित को ही 'तपस्वी' बताया गया है- तपस्सी अक्कोधनो होति, अनुपनाही (दीघनिकाय-3/2/5), अर्थात् तपस्वी क्रोधरहित व वैरभावशून्य होता है।
उपर्युक्त वैचारिक पृष्ठभूमि में जैन और वैदिक-दोनों धाराओं से एक-एक कथानक यहां अवतरित किया गया है। दोनों कथानकों में एक ही तथ्य को समान भाव से कहा गया है कि तप के साथ जब तक अहंकार रहेगा तब तक तप प्रभाव-हीन रहेगा। अहं की दीवार टूटते ही जीवन-नभ पर ज्ञान के सूर्य का उदय होता है और साधना सफल हो जाती है।
द्वितीय तण्ड/285