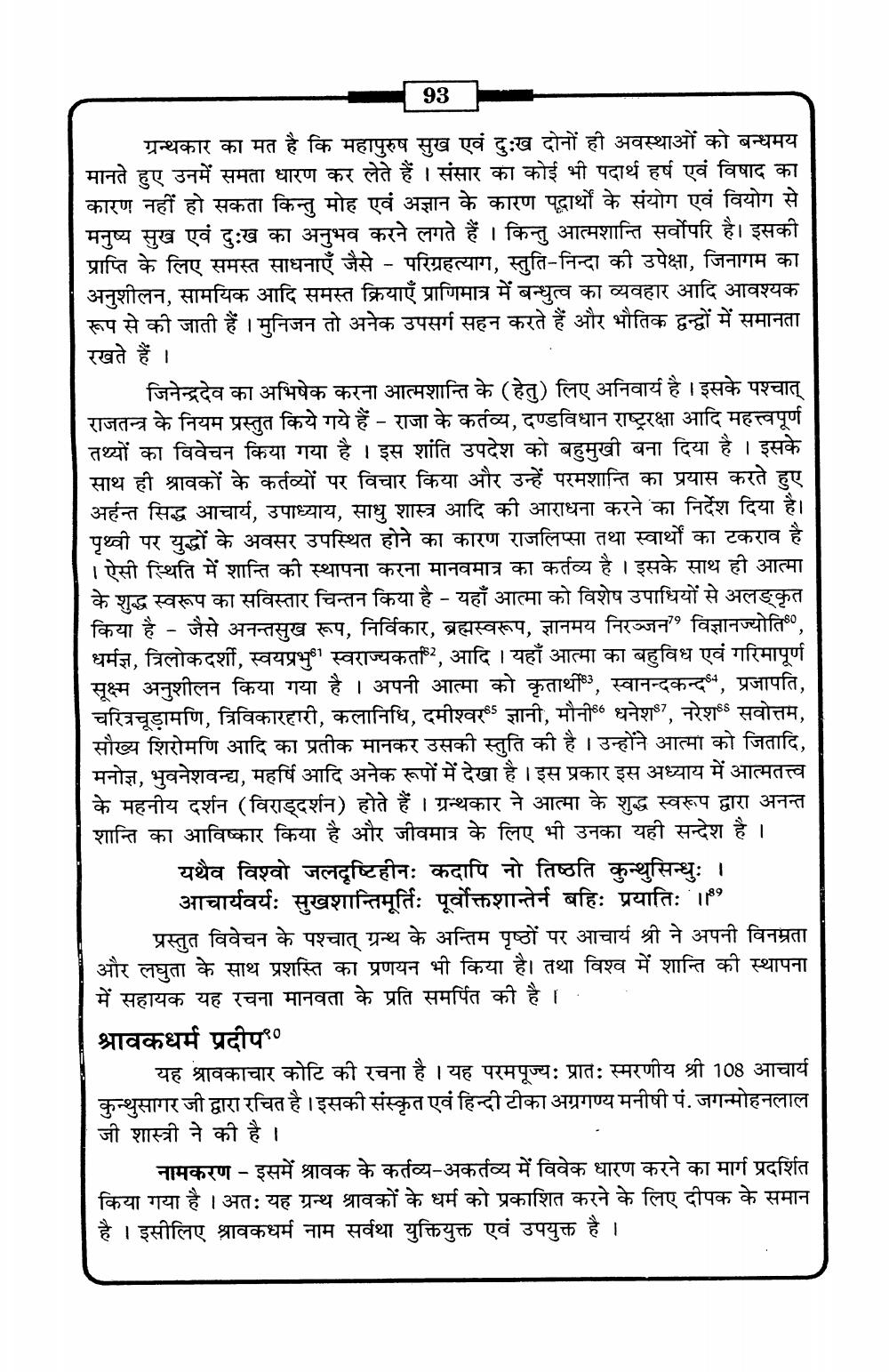________________
93
ग्रन्थकार का मत है कि महापुरुष सुख एवं दुःख दोनों ही अवस्थाओं को बन्धमय मानते हुए उनमें समता धारण कर लेते हैं। संसार का कोई भी पदार्थ हर्ष एवं विषाद का कारण नहीं हो सकता किन्तु मोह एवं अज्ञान के कारण पदार्थों के संयोग एवं वियोग से मनुष्य सुख एवं दुःख का अनुभव करने लगते हैं । किन्तु आत्मशान्ति सर्वोपरि है। इसकी प्राप्ति के लिए समस्त साधनाएँ जैसे- परिग्रहत्याग, स्तुति-निन्दा की उपेक्षा, जिनागम का अनुशीलन, सामयिक आदि समस्त क्रियाएँ प्राणिमात्र में बन्धुत्व का व्यवहार आदि आवश्यक रूप से की जाती हैं । मुनिजन तो अनेक उपसर्ग सहन करते हैं और भौतिक द्वन्द्वों में समानता रखते हैं ।
I
जिनेन्द्रदेव का अभिषेक करना आत्मशान्ति के (हेतु) लिए अनिवार्य है । इसके पश्चात् राजतन्त्र के नियम प्रस्तुत किये गये हैं - राजा के कर्तव्य, दण्डविधान राष्ट्ररक्षा आदि महत्त्वपूर्ण तथ्यों का विवेचन किया गया है। इस शांति उपदेश को बहुमुखी बना दिया है । इसके साथ ही श्रावकों के कर्तव्यों पर विचार किया और उन्हें परमशान्ति का प्रयास करते हुए अर्हन्त सिद्ध आचार्य, उपाध्याय, साधु शास्त्र आदि की आराधना करने का निर्देश दिया है। पृथ्वी पर युद्धों के अवसर उपस्थित होने का कारण राजलिप्सा तथा स्वार्थों का टकराव है । ऐसी स्थिति में शान्ति की स्थापना करना मानवमात्र का कर्तव्य है । इसके साथ ही आत्मा
शुद्ध स्वरूप का सविस्तार चिन्तन किया है - यहाँ आत्मा को विशेष उपाधियों से अलङ्कृत किया है - जैसे अनन्तसुख रूप, निर्विकार, ब्रह्मस्वरूप, ज्ञानमय निरञ्जन” विज्ञानज्योतिं, धर्मज्ञ, त्रिलोकदर्शी, स्वयप्रभु" स्वराज्यकर्ता 2, आदि । यहाँ आत्मा का बहुविध एवं गरिमापूर्ण सूक्ष्म अनुशीलन किया गया है । अपनी आत्मा को कृतार्थी, स्वानन्दकन्द, प्रजापति, चरित्रचूड़ामणि, त्रिविकारहारी, कलानिधि, दमीश्वर" ज्ञानी, मौनी" धनेश 7, नरेश" सवोत्तम, सौख्य शिरोमणि आदि का प्रतीक मानकर उसकी स्तुति की है । उन्होंने आत्मा को जितादि, मनोज्ञ, भुवनेशवन्द्य, महर्षि आदि अनेक रूपों में देखा है। इस प्रकार इस अध्याय में आत्मतत्त्व के महनीय दर्शन (विराड्दर्शन) होते हैं । ग्रन्थकार ने आत्मा के शुद्ध स्वरूप द्वारा अनन्त शान्ति का आविष्कार किया है और जीवमात्र के लिए भी उनका यही सन्देश है ।
यथैव विश्वो जलदृष्टिहीनः कदापि नो तिष्ठति कुन्थुसिन्धुः । आचार्यवर्यः सुखशान्तिमूर्तिः पूर्वोक्तशान्तेर्न बहिः प्रयातिः ॥ १
प्रस्तुत विवेचन के पश्चात् ग्रन्थ के अन्तिम पृष्ठों पर आचार्य श्री ने अपनी विनम्रता और लघुता के साथ प्रशस्ति का प्रणयन भी किया है। तथा विश्व में शान्ति की स्थापना में सहायक यह रचना मानवता के प्रति समर्पित की है ।
श्रावकधर्म प्रदीप ̈
यह श्रावकाचार कोटि की रचना है । यह परमपूज्यः प्रातः स्मरणीय श्री 108 आचार्य कुन्थुसागर जी द्वारा रचित है। इसकी संस्कृत एवं हिन्दी टीका अग्रगण्य मनीषी पं. जगन्मोहनलाल जी शास्त्री ने की है ।
नामकरण - इसमें श्रावक के कर्तव्य-अकर्तव्य में विवेक धारण करने का मार्ग प्रदर्शित किया गया है । अतः यह ग्रन्थ श्रावकों के धर्म को प्रकाशित करने के लिए दीपक के समान है । इसीलिए श्रावकधर्म नाम सर्वथा युक्तियुक्त एवं उपयुक्त है ।