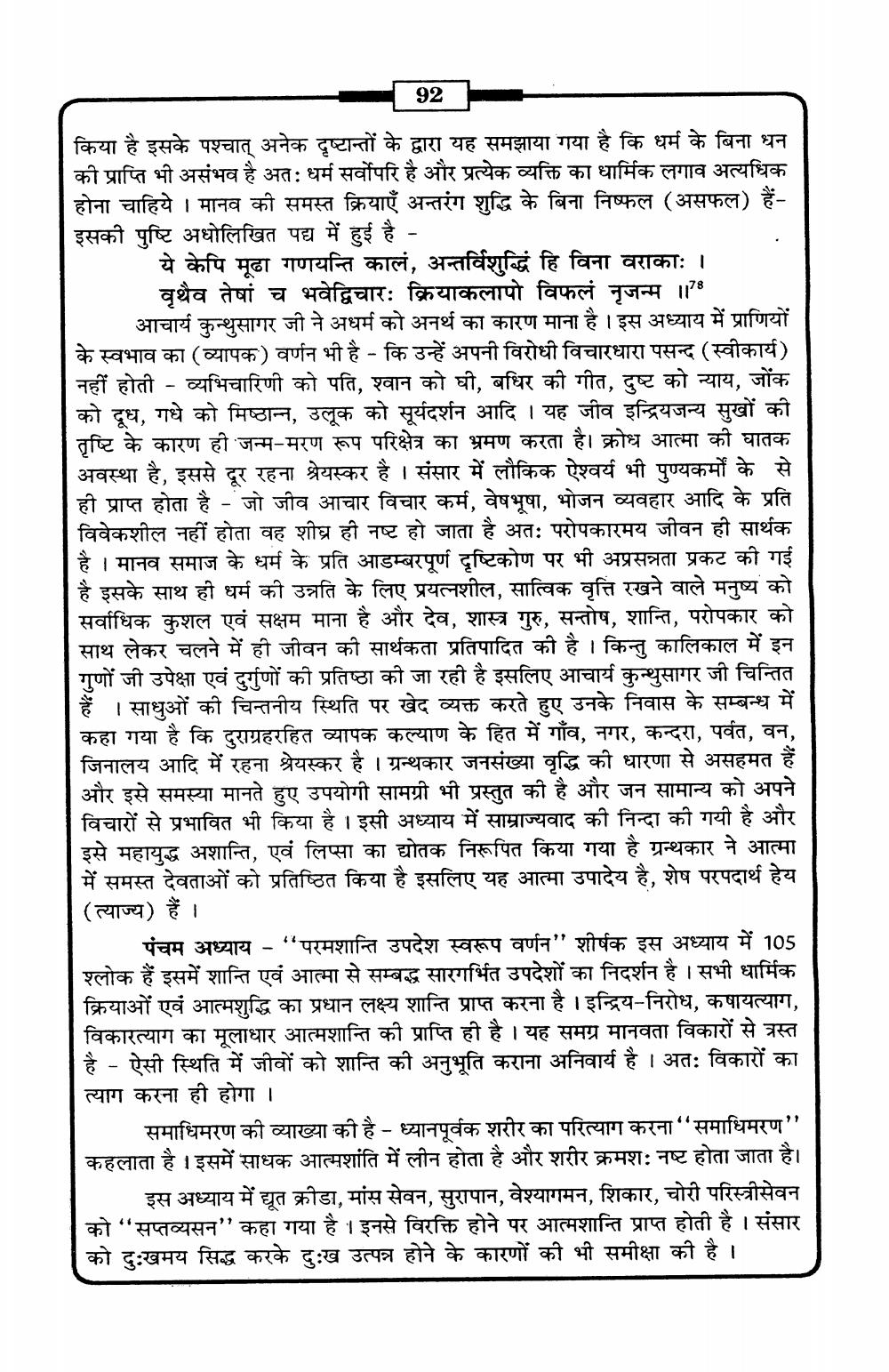________________
92
किया है इसके पश्चात् अनेक दृष्टान्तों के द्वारा यह समझाया गया है कि धर्म के बिना धन की प्राप्ति भी असंभव है अत: धर्म सर्वोपरि है और प्रत्येक व्यक्ति का धार्मिक लगाव अत्यधिक होना चाहिये । मानव की समस्त क्रियाएँ अन्तरंग शुद्धि के बिना निष्फल (असफल) हैंइसकी पुष्टि अधोलिखित पद्य में हुई है -
ये केपि मूढा गणयन्ति कालं, अन्तर्विशुद्धिं हि विना वराकाः । वृथैव तेषां च भवेद्विचारः क्रियाकलापो विफलं नृजन्म ॥
आचार्य कुन्थुसागर जी ने अधर्म को अनर्थ का कारण माना है । इस अध्याय में प्राणियों के स्वभाव का (व्यापक) वर्णन भी है - कि उन्हें अपनी विरोधी विचारधारा पसन्द (स्वीकार्य) नहीं होती - व्यभिचारिणी को पति, श्वान को घी, बधिर की गीत, दुष्ट को न्याय, जोंक को दूध, गधे को मिष्ठान्न, उलूक को सूर्यदर्शन आदि । यह जीव इन्द्रियजन्य सुखों की तृष्टि के कारण ही जन्म-मरण रूप परिक्षेत्र का भ्रमण करता है। क्रोध आत्मा की घातक अवस्था है, इससे दूर रहना श्रेयस्कर है । संसार में लौकिक ऐश्वर्य भी पुण्यकर्मों के से ही प्राप्त होता है - जो जीव आचार विचार कर्म, वेषभूषा, भोजन व्यवहार आदि के प्रति विवेकशील नहीं होता वह शीघ्र ही नष्ट हो जाता है अतः परोपकारमय जीवन ही सार्थक है । मानव समाज के धर्म के प्रति आडम्बरपूर्ण दृष्टिकोण पर भी अप्रसन्नता प्रकट की गई है इसके साथ ही धर्म की उन्नति के लिए प्रयत्नशील, सात्विक वृत्ति रखने वाले मनुष्य को सर्वाधिक कुशल एवं सक्षम माना है और देव, शास्त्र गरु. सन्तोष, शान्ति, परोपकार को साथ लेकर चलने में ही जीवन की सार्थकता प्रतिपादित की है । किन्तु कालिकाल में इन गुणों जी उपेक्षा एवं दुर्गुणों की प्रतिष्ठा की जा रही है इसलिए आचार्य कुन्थुसागर जी चिन्तित हैं । साधुओं की चिन्तनीय स्थिति पर खेद व्यक्त करते हुए उनके निवास के सम्बन्ध में कहा गया है कि दुराग्रहरहित व्यापक कल्याण के हित में गाँव, नगर, कन्दरा, पर्वत, वन, जिनालय आदि में रहना श्रेयस्कर है । ग्रन्थकार जनसंख्या वृद्धि की धारणा से असहमत हैं
और इसे समस्या मानते हुए उपयोगी सामग्री भी प्रस्तुत की है और जन सामान्य को अपने विचारों से प्रभावित भी किया है । इसी अध्याय में साम्राज्यवाद की निन्दा की गयी है और इसे महायुद्ध अशान्ति, एवं लिप्सा का द्योतक निरूपित किया गया है ग्रन्थकार ने आत्मा में समस्त देवताओं को प्रतिष्ठित किया है इसलिए यह आत्मा उपादेय है, शेष परपदार्थ हेय (त्याज्य) हैं।
पंचम अध्याय - "परमशान्ति उपदेश स्वरूप वर्णन" शीर्षक इस अध्याय में 105 श्लोक हैं इसमें शान्ति एवं आत्मा से सम्बद्ध सारगर्भित उपदेशों का निदर्शन है । सभी धार्मिक क्रियाओं एवं आत्मशुद्धि का प्रधान लक्ष्य शान्ति प्राप्त करना है । इन्द्रिय-निरोध, कषायत्याग, विकारत्याग का मूलाधार आत्मशान्ति की प्राप्ति ही है । यह समग्र मानवता विकारों से त्रस्त है - ऐसी स्थिति में जीवों को शान्ति की अनुभूति कराना अनिवार्य है । अत: विकारों का त्याग करना ही होगा ।
समाधिमरण की व्याख्या की है - ध्यानपूर्वक शरीर का परित्याग करना "समाधिमरण" कहलाता है । इसमें साधक आत्मशांति में लीन होता है और शरीर क्रमश: नष्ट होता जाता है।
इस अध्याय में द्यूत क्रीडा, मांस सेवन, सुरापान, वेश्यागमन, शिकार, चोरी परिस्त्रीसेवन को "सप्तव्यसन" कहा गया है । इनसे विरक्ति होने पर आत्मशान्ति प्राप्त होती है । संसार को दुःखमय सिद्ध करके दुःख उत्पन्न होने के कारणों की भी समीक्षा की है ।