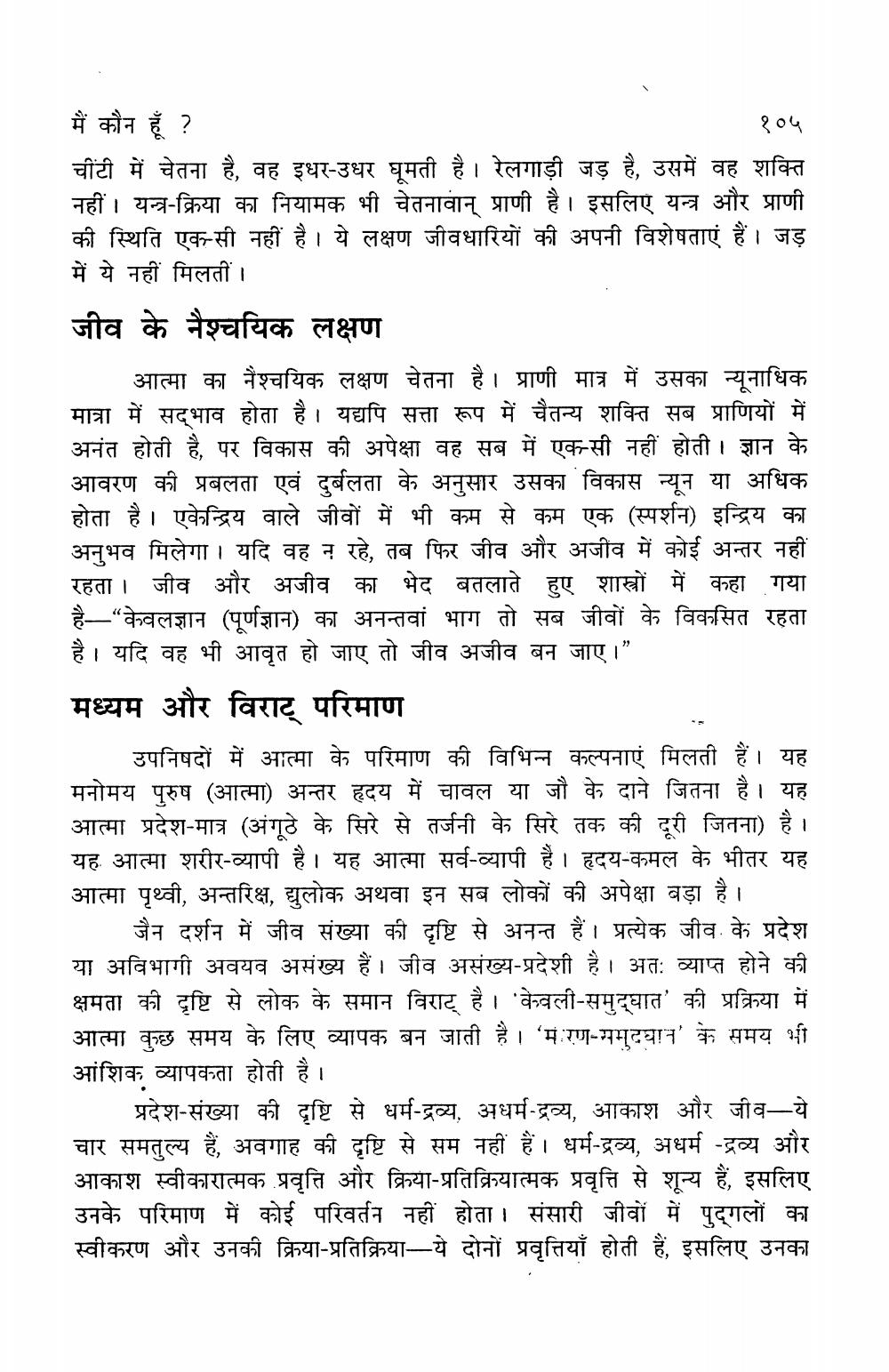________________
मैं कौन हूँ ?
१०५
चींटी में चेतना है, वह इधर-उधर घूमती है। रेलगाड़ी जड़ है, उसमें वह शक्ति नहीं । यन्त्र-क्रिया का नियामक भी चेतनावान् प्राणी है । इसलिए यन्त्र और प्राणी की स्थिति एक सी नहीं है। लक्षण जीवधारियों की अपनी विशेषताएं हैं। जड़ में ये नहीं मिलतीं ।
1
जीव के नैश्चयिक लक्षण
आत्मा का नैश्चयिक लक्षण चेतना है । प्राणी मात्र में उसका न्यूनाधिक मात्रा में सद्भाव होता है । यद्यपि सत्ता रूप में चैतन्य शक्ति सब प्राणियों में अनंत होती है, पर विकास की अपेक्षा वह सब में एक-सी नहीं होती । ज्ञान के आवरण की प्रबलता एवं दुर्बलता के अनुसार उसका विकास न्यून या अधिक होता है । एकेन्द्रिय वाले जीवों में भी कम से कम एक (स्पर्शन) इन्द्रिय का अनुभव मिलेगा । यदि वह न रहे, तब फिर जीव और अजीव में कोई अन्तर नहीं रहता। जीव और अजीव का भेद बतलाते हुए शास्त्रों में कहा गया है — “केवलज्ञान (पूर्णज्ञान) का अनन्तवां भाग तो सब जीवों के विकसित रहता है । यदि वह भी आवृत हो जाए तो जीव अजीव बन जाए। "
मध्यम और विराट् परिमाण
उपनिषदों में आत्मा के परिमाण की विभिन्न कल्पनाएं मिलती हैं । यह मनोमय पुरुष (आत्मा) अन्तर हृदय में चावल या जौ के दाने जितना है । यह आत्मा प्रदेश- मात्र (अंगूठे के सिरे से तर्जनी के सिरे तक की दूरी जितना ) है यह आत्मा शरीर-व्यापी है । यह आत्मा सर्व व्यापी है । हृदय-कमल के भीतर यह आत्मा पृथ्वी, अन्तरिक्ष, द्युलोक अथवा इन सब लोकों की अपेक्षा बड़ा है
1
|
जैन दर्शन में जीव संख्या की दृष्टि से अनन्त हैं । प्रत्येक जीव के प्रदेश या अविभागी अवयव असंख्य हैं। जीव असंख्य- प्रदेशी है । अतः व्याप्त होने की क्षमता की दृष्टि से लोक के समान विराट् है । 'केवली - समुद्घात' की प्रक्रिया में आत्मा कुछ समय के लिए व्यापक बन जाती है। 'मरण-समुदघान' के समय भी आंशिक व्यापकता होती है 1
प्रदेश- संख्या की दृष्टि से धर्म-द्रव्य, अधर्म- द्रव्य, आकाश और जीव-ये चार समतुल्य हैं, अवगाह की दृष्टि से सम नहीं हैं । धर्म-द्रव्य, अधर्म - द्रव्य और आकाश स्वीकारात्मक प्रवृत्ति और क्रिया-प्रतिक्रियात्मक प्रवृत्ति से शून्य हैं, इसलिए उनके परिमाण में कोई परिवर्तन नहीं होता । संसारी जीवों में पुद्गलों का स्वीकरण और उनकी क्रिया-प्रतिक्रिया - ये दोनों प्रवृत्तियाँ होती हैं, इसलिए उनका