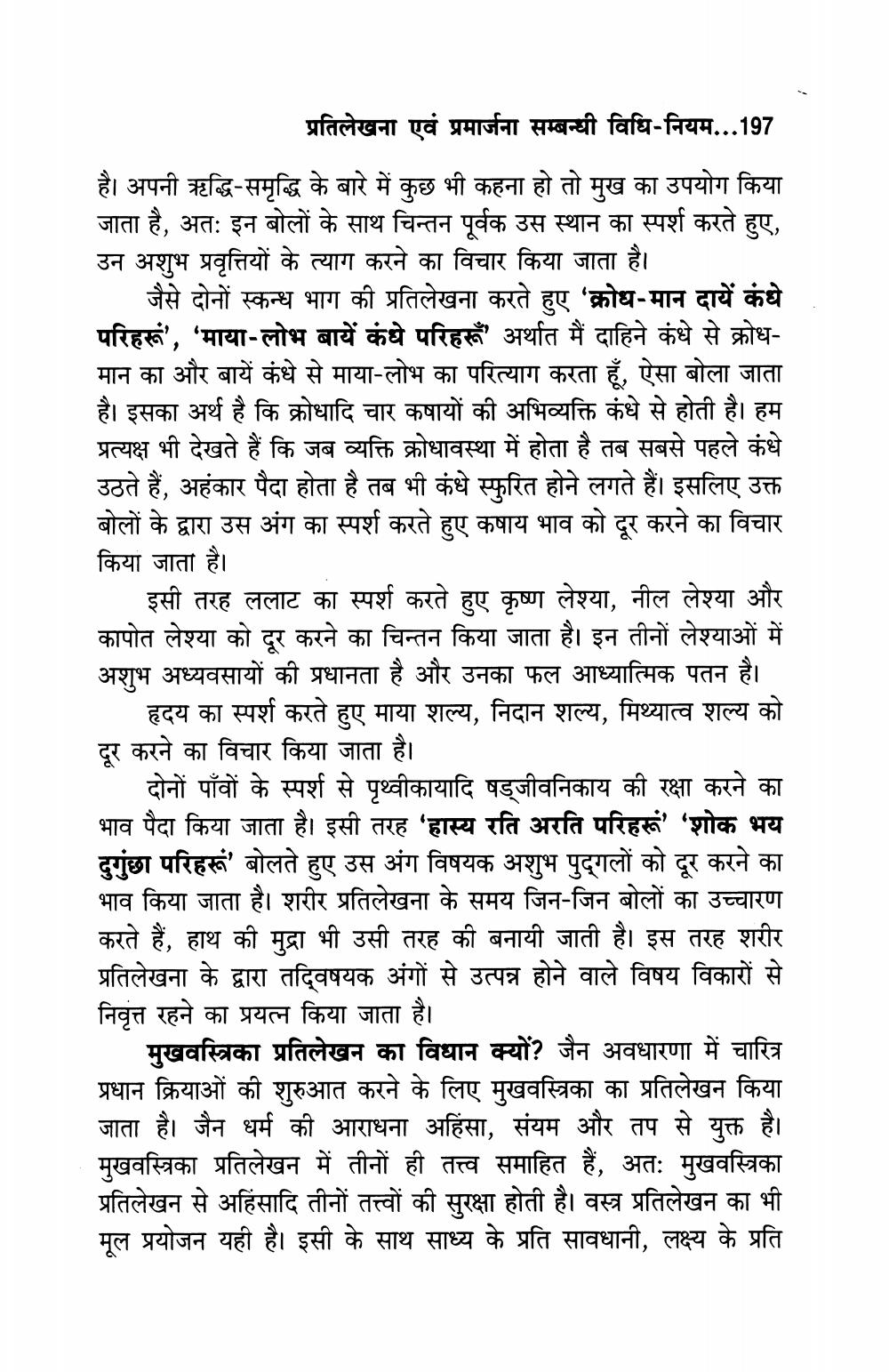________________
प्रतिलेखना एवं प्रमार्जना सम्बन्धी विधि-नियम...197 है। अपनी ऋद्धि-समृद्धि के बारे में कुछ भी कहना हो तो मुख का उपयोग किया जाता है, अत: इन बोलों के साथ चिन्तन पूर्वक उस स्थान का स्पर्श करते हुए, उन अशुभ प्रवृत्तियों के त्याग करने का विचार किया जाता है। ___ जैसे दोनों स्कन्ध भाग की प्रतिलेखना करते हुए 'क्रोध-मान दायें कंधे परिहरूं', 'माया-लोभ बायें कंधे परिहरूँ' अर्थात मैं दाहिने कंधे से क्रोधमान का और बायें कंधे से माया-लोभ का परित्याग करता हूँ, ऐसा बोला जाता है। इसका अर्थ है कि क्रोधादि चार कषायों की अभिव्यक्ति कंधे से होती है। हम प्रत्यक्ष भी देखते हैं कि जब व्यक्ति क्रोधावस्था में होता है तब सबसे पहले कंधे उठते हैं, अहंकार पैदा होता है तब भी कंधे स्फुरित होने लगते हैं। इसलिए उक्त बोलों के द्वारा उस अंग का स्पर्श करते हुए कषाय भाव को दूर करने का विचार किया जाता है। __इसी तरह ललाट का स्पर्श करते हुए कृष्ण लेश्या, नील लेश्या और कापोत लेश्या को दूर करने का चिन्तन किया जाता है। इन तीनों लेश्याओं में अशुभ अध्यवसायों की प्रधानता है और उनका फल आध्यात्मिक पतन है। ____ हृदय का स्पर्श करते हुए माया शल्य, निदान शल्य, मिथ्यात्व शल्य को दूर करने का विचार किया जाता है।
दोनों पाँवों के स्पर्श से पृथ्वीकायादि षड्जीवनिकाय की रक्षा करने का भाव पैदा किया जाता है। इसी तरह 'हास्य रति अरति परिहरूं' 'शोक भय दुगुंछा परिहरूं' बोलते हुए उस अंग विषयक अशुभ पुद्गलों को दूर करने का भाव किया जाता है। शरीर प्रतिलेखना के समय जिन-जिन बोलों का उच्चारण करते हैं, हाथ की मुद्रा भी उसी तरह की बनायी जाती है। इस तरह शरीर प्रतिलेखना के द्वारा तद्विषयक अंगों से उत्पन्न होने वाले विषय विकारों से निवृत्त रहने का प्रयत्न किया जाता है।
मुखवस्त्रिका प्रतिलेखन का विधान क्यों? जैन अवधारणा में चारित्र प्रधान क्रियाओं की शुरुआत करने के लिए मुखवस्त्रिका का प्रतिलेखन किया जाता है। जैन धर्म की आराधना अहिंसा, संयम और तप से युक्त है। मुखवस्त्रिका प्रतिलेखन में तीनों ही तत्त्व समाहित हैं, अत: मुखवस्त्रिका प्रतिलेखन से अहिंसादि तीनों तत्त्वों की सुरक्षा होती है। वस्त्र प्रतिलेखन का भी मूल प्रयोजन यही है। इसी के साथ साध्य के प्रति सावधानी, लक्ष्य के प्रति