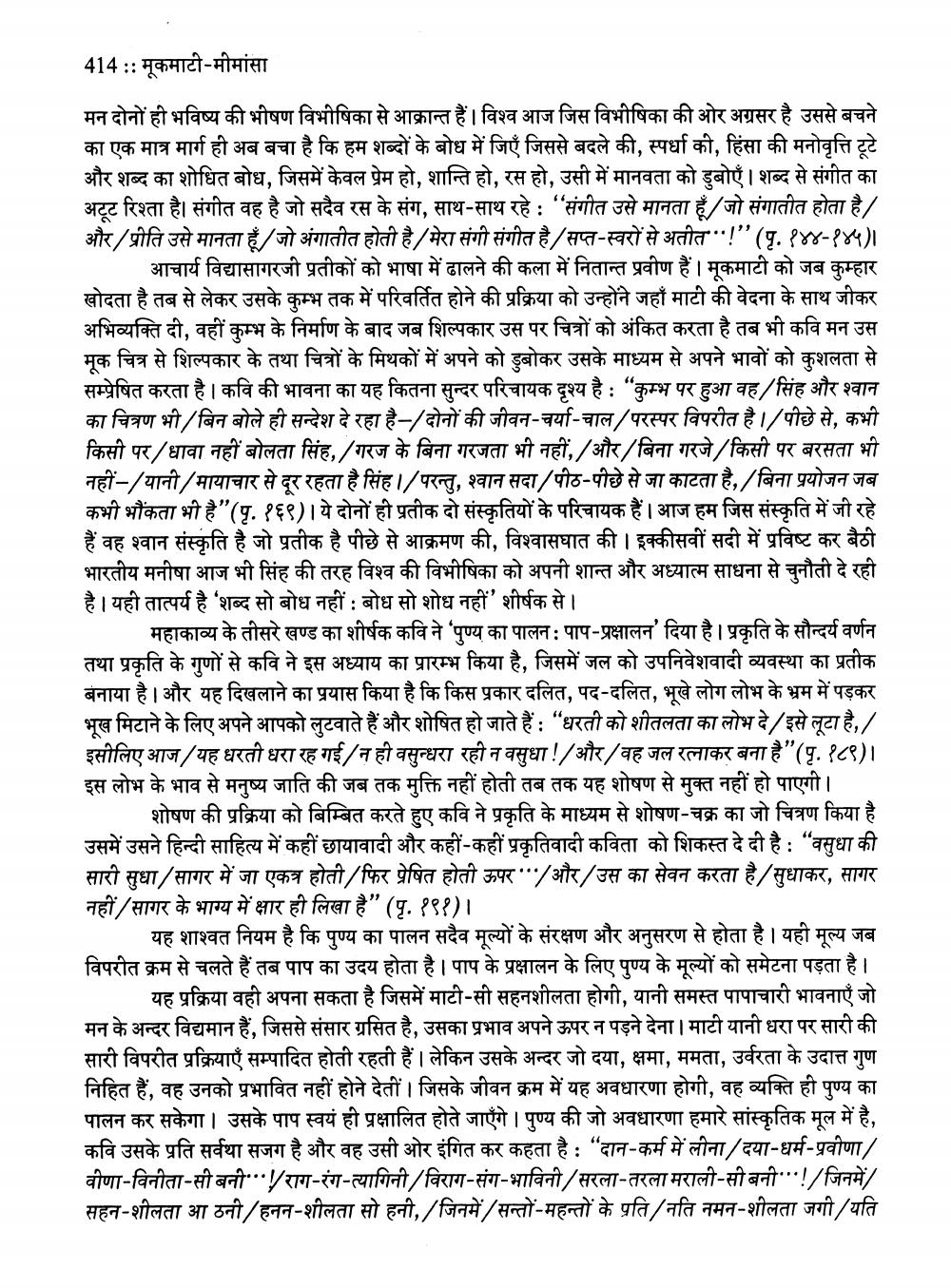________________
414 :: मूकमाटी-मीमांसा मन दोनों ही भविष्य की भीषण विभीषिका से आक्रान्त हैं। विश्व आज जिस विभीषिका की ओर अग्रसर है उससे बचने का एक मात्र मार्ग ही अब बचा है कि हम शब्दों के बोध में जिएँ जिससे बदले की, स्पर्धा की, हिंसा की मनोवृत्ति टूटे और शब्द का शोधित बोध, जिसमें केवल प्रेम हो, शान्ति हो, रस हो, उसी में मानवता को डुबोएँ। शब्द से संगीत का अटूट रिश्ता है। संगीत वह है जो सदैव रस के संग, साथ-साथ रहे : "संगीत उसे मानता हूँ/जो संगातीत होता है/ और/प्रीति उसे मानता हूँ/जो अंगातीत होती है/मेरा संगी संगीत है/सप्त-स्वरों से अतीत !" (पृ. १४४-१४५)।
आचार्य विद्यासागरजी प्रतीकों को भाषा में ढालने की कला में नितान्त प्रवीण हैं । मूकमाटी को जब कुम्हार खोदता है तब से लेकर उसके कुम्भ तक में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को उन्होंने जहाँ माटी की वेदना के साथ जीकर अभिव्यक्ति दी, वहीं कुम्भ के निर्माण के बाद जब शिल्पकार उस पर चित्रों को अंकित करता है तब भी कवि मन उस मूक चित्र से शिल्पकार के तथा चित्रों के मिथकों में अपने को डुबोकर उसके माध्यम से अपने भावों को कुशलता से सम्प्रेषित करता है । कवि की भावना का यह कितना सुन्दर परिचायक दृश्य है : “कुम्भ पर हुआ वह/सिंह और श्वान का चित्रण भी/बिन बोले ही सन्देश दे रहा है-/दोनों की जीवन-चर्या-चाल/परस्पर विपरीत है।/पीछे से, कभी किसी पर/धावा नहीं बोलता सिंह,/गरज के बिना गरजता भी नहीं,/और/बिना गरजे/किसी पर बरसता भी नहीं-/यानी/मायाचार से दूर रहता है सिंह ।/परन्तु, श्वान सदा/पीठ-पीछे से जा काटता है,/बिना प्रयोजन जब कभी भौंकता भी है" (पृ. १६९)। ये दोनों ही प्रतीक दो संस्कृतियों के परिचायक हैं। आज हम जिस संस्कृति में जी रहे हैं वह श्वान संस्कृति है जो प्रतीक है पीछे से आक्रमण की, विश्वासघात की। इक्कीसवीं सदी में प्रविष्ट कर बैठी भारतीय मनीषा आज भी सिंह की तरह विश्व की विभीषिका को अपनी शान्त और अध्यात्म साधना से चुनौती दे रही है। यही तात्पर्य है 'शब्द सो बोध नहीं : बोध सो शोध नहीं' शीर्षक से।
महाकाव्य के तीसरे खण्ड का शीर्षक कवि ने 'पुण्य का पालन : पाप-प्रक्षालन' दिया है। प्रकृति के सौन्दर्य वर्णन तथा प्रकृति के गुणों से कवि ने इस अध्याय का प्रारम्भ किया है, जिसमें जल को उपनिवेशवादी व्यवस्था का प्रतीक बनाया है। और यह दिखलाने का प्रयास किया है कि किस प्रकार दलित, पद-दलित, भूखे लोग लोभ के भ्रम में पड़कर भूख मिटाने के लिए अपने आपको लुटवाते हैं और शोषित हो जाते हैं : "धरती को शीतलता का लोभ दे/इसे लूटा है,/ इसीलिए आज/यह धरती धरा रह गई/न ही वसुन्धरा रही न वसुधा!/और/वह जल रत्नाकर बना है"(पृ. १८९)। इस लोभ के भाव से मनुष्य जाति की जब तक मुक्ति नहीं होती तब तक यह शोषण से मुक्त नहीं हो
हो पाएगी। शोषण की प्रक्रिया को बिम्बित करते हए कवि ने प्रकति के माध्यम से शोषण-चक्र का जो चित्रण किया है उसमें उसने हिन्दी साहित्य में कहीं छायावादी और कहीं-कहीं प्रकृतिवादी कविता को शिकस्त दे दी है : “वसुधा की सारी सुधा/सागर में जा एकत्र होती/फिर प्रेषित होती ऊपर ""/और/उस का सेवन करता है/सुधाकर, सागर नहीं/सागर के भाग्य में क्षार ही लिखा है" (पृ. १९१)।
यह शाश्वत नियम है कि पुण्य का पालन सदैव मूल्यों के संरक्षण और अनुसरण से होता है। यही मल्य जब विपरीत क्रम से चलते हैं तब पाप का उदय होता है । पाप के प्रक्षालन के लिए पुण्य के मूल्यों को समेटना पड़ता है।
यह प्रक्रिया वही अपना सकता है जिसमें माटी-सी सहनशीलता होगी, यानी समस्त पापाचारी भावनाएँ जो न के अन्दर विद्यमान हैं. जिससे संसार गसित है. उसका प्रभाव अपने ऊपर न पड़ने देना। माटी यानी धरा पर सारी की सारी विपरीत प्रक्रियाएँ सम्पादित होती रहती हैं। लेकिन उसके अन्दर जो दया, क्षमा, ममता, उर्वरता के उदात्त गुण निहित हैं, वह उनको प्रभावित नहीं होने देती। जिसके जीवन क्रम में यह अवधारणा होगी. वह व्यक्ति ही पण्य का पालन कर सकेगा। उसके पाप स्वयं ही प्रक्षालित होते जाएँगे । पुण्य की जो अवधारणा हमारे सांस्कृतिक मूल में कवि उसके प्रति सर्वथा सजग है और वह उसी ओर इंगित कर कहता है : “दान-कर्म में लीना/दया-धर्म-प्रवीणा/
पीता-सी बनी.../राग-रंग-त्यागिनी/विराग-संग-भाविनी/सरला-तरला मराली-सी बनी.../जिनमें/ सहन-शीलता आ ठनी/हनन-शीलता सो हनी,/जिनमें/सन्तों-महन्तों के प्रति/नति नमन-शीलता जगी/यति