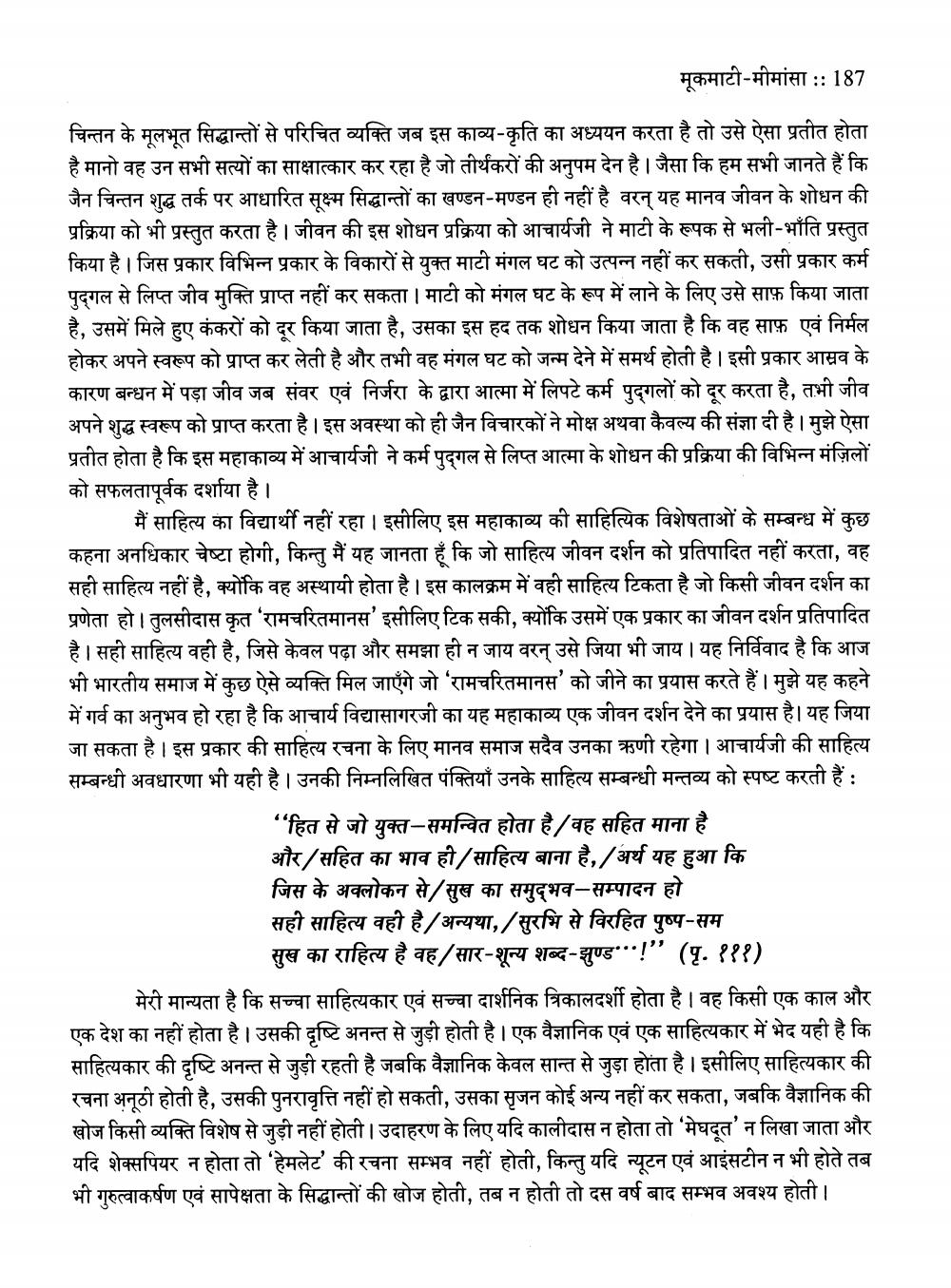________________
मूकमाटी-मीमांसा :: 187
चिन्तन के मूलभूत सिद्धान्तों से परिचित व्यक्ति जब इस काव्य-कृति का अध्ययन करता है तो उसे ऐसा प्रतीत होता है मानो वह उन सभी सत्यों का साक्षात्कार कर रहा है जो तीर्थंकरों की अनुपम देन है । जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जैन चिन्तन शुद्ध तर्क पर आधारित सूक्ष्म सिद्धान्तों का खण्डन-मण्डन ही नहीं है वरन् यह मानव जीवन के शोधन की प्रक्रिया को भी प्रस्तुत करता है। जीवन की इस शोधन प्रक्रिया को आचार्यजी ने माटी के रूपक से भली-भाँति प्रस्तुत किया है। जिस प्रकार विभिन्न प्रकार के विकारों से युक्त माटी मंगल घट को उत्पन्न नहीं कर सकती, उसी प्रकार कर्म पुद्गल से लिप्त जीव मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता । माटी को मंगल घट के रूप में लाने के लिए उसे साफ़ किया जाता है, उसमें मिले हुए कंकरों को दूर किया जाता है, उसका इस हद तक शोधन किया जाता है कि वह साफ़ एवं निर्मल होकर अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेती है और तभी वह मंगल घट को जन्म देने में समर्थ होती है । इसी प्रकार आस्रव के कारण बन्धन में पड़ा जीव जब संवर एवं निर्जरा के द्वारा आत्मा में लिपटे कर्म पुद्गलों को दूर करता है, तभी जीव अपने शुद्ध स्वरूप को प्राप्त करता है । इस अवस्था को ही जैन विचारकों ने मोक्ष अथवा कैवल्य की संज्ञा दी है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि इस महाकाव्य में आचार्यजी ने कर्म पुद्गल से लिप्त आत्मा के शोधन की प्रक्रिया की विभिन्न मंज़िलों को सफलतापूर्वक दर्शाया है।
मैं साहित्य का विद्यार्थी नहीं रहा । इसीलिए इस महाकाव्य की साहित्यिक विशेषताओं के सम्बन्ध में कुछ कहना अनधिकार चेष्टा होगी, किन्तु मैं यह जानता हूँ कि जो साहित्य जीवन दर्शन को प्रतिपादित नहीं करता, वह सही साहित्य नहीं है, क्योंकि वह अस्थायी होता है । इस कालक्रम में वही साहित्य टिकता है जो किसी जीवन दर्शन का प्रणेता हो । तुलसीदास कृत 'रामचरितमानस' इसीलिए टिक सकी, क्योंकि उसमें एक प्रकार का जीवन दर्शन प्रतिपादित है। सही साहित्य वही है, जिसे केवल पढ़ा और समझा ही न जाय वरन् उसे जिया भी जाय । यह निर्विवाद है कि आज भी भारतीय समाज में कुछ ऐसे व्यक्ति मिल जाएंगे जो 'रामचरितमानस' को जीने का प्रयास करते हैं। मुझे यह कहने में गर्व का अनुभव हो रहा है कि आचार्य विद्यासागरजी का यह महाकाव्य एक जीवन दर्शन देने का प्रयास है। यह जिया जा सकता है । इस प्रकार की साहित्य रचना के लिए मानव समाज सदैव उनका ऋणी रहेगा। आचार्यजी की साहित्य सम्बन्धी अवधारणा भी यही है । उनकी निम्नलिखित पंक्तियाँ उनके साहित्य सम्बन्धी मन्तव्य को स्पष्ट करती हैं :
"हित से जो युक्त-समन्वित होता है/वह सहित माना है और/सहित का भाव ही/साहित्य बाना है,/अर्थ यह हुआ कि जिस के अवलोकन से/सुख का समुद्भव-सम्पादन हो सही साहित्य वही है/अन्यथा,/सुरभि से विरहित पुष्प-सम
सुख का राहित्य है वह/सार-शून्य शब्द-झुण्ड'!" (पृ. १११) मेरी मान्यता है कि सच्चा साहित्यकार एवं सच्चा दार्शनिक त्रिकालदर्शी होता है । वह किसी एक काल और एक देश का नहीं होता है। उसकी दृष्टि अनन्त से जुड़ी होती है । एक वैज्ञानिक एवं एक साहित्यकार में भेद यही है कि साहित्यकार की दृष्टि अनन्त से जुड़ी रहती है जबकि वैज्ञानिक केवल सान्त से जुड़ा होता है । इसीलिए साहित्यकार की रचना अनूठी होती है, उसकी पुनरावृत्ति नहीं हो सकती, उसका सृजन कोई अन्य नहीं कर सकता, जबकि वैज्ञानिक की खोज किसी व्यक्ति विशेष से जुड़ी नहीं होती। उदाहरण के लिए यदि कालीदास न होता तो 'मेघदूत' न लिखा जाता और यदि शेक्सपियर न होता तो 'हेमलेट' की रचना सम्भव नहीं होती, किन्तु यदि न्यूटन एवं आइंसटीन न भी होते तब भी गुरुत्वाकर्षण एवं सापेक्षता के सिद्धान्तों की खोज होती, तब न होती तो दस वर्ष बाद सम्भव अवश्य होती।