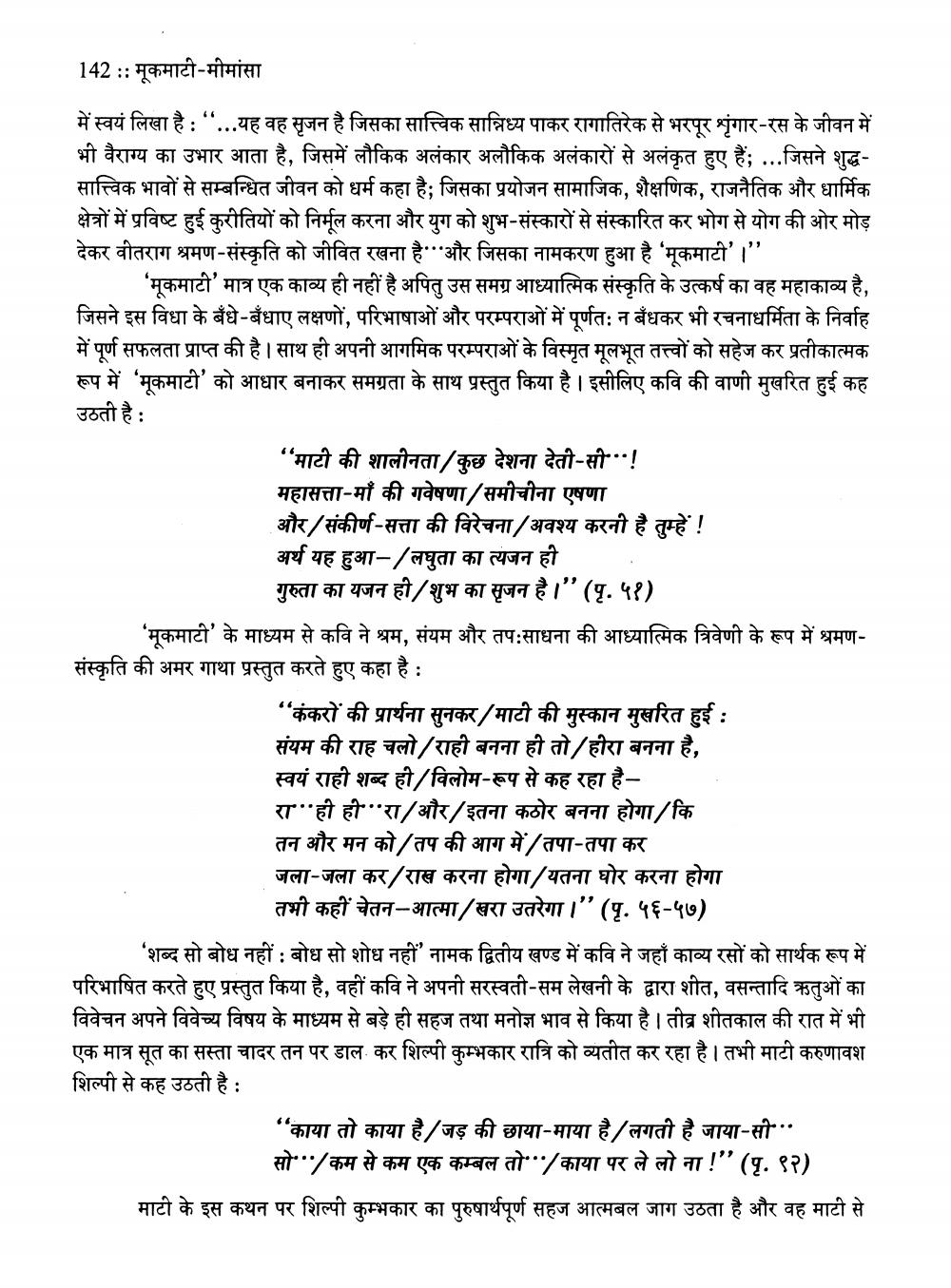________________
142 :: मूकमाटी-मीमांसा
में स्वयं लिखा है : "...यह वह सृजन है जिसका सात्त्विक सान्निध्य पाकर रागातिरेक से भरपूर शृंगार-रस के जीवन में भी वैराग्य का उभार आता है, जिसमें लौकिक अलंकार अलौकिक अलंकारों से अलंकृत हुए हैं; ...जिसने शुद्धसात्त्विक भावों से सम्बन्धित जीवन को धर्म कहा है; जिसका प्रयोजन सामाजिक, शैक्षणिक, राजनैतिक और धार्मिक क्षेत्रों में प्रविष्ट हुई कुरीतियों को निर्मूल करना और युग को शुभ-संस्कारों से संस्कारित कर भोग से योग की ओर मोड़ देकर वीतराग श्रमण-संस्कृति को जीवित रखना है और जिसका नामकरण हुआ है 'मूकमाटी'।" ।
'मूकमाटी' मात्र एक काव्य ही नहीं है अपितु उस समग्र आध्यात्मिक संस्कृति के उत्कर्ष का वह महाकाव्य है, जिसने इस विधा के बँधे-बँधाए लक्षणों, परिभाषाओं और परम्पराओं में पूर्णत: न बँधकर भी रचनाधर्मिता के निर्वाह में पूर्ण सफलता प्राप्त की है। साथ ही अपनी आगमिक परम्पराओं के विस्मृत मूलभूत तत्त्वों को सहेज कर प्रतीकात्मक रूप में 'मूकमाटी' को आधार बनाकर समग्रता के साथ प्रस्तुत किया है । इसीलिए कवि की वाणी मुखरित हुई कह उठती है :
"माटी की शालीनता/कुछ देशना देती-सी ! महासत्ता-माँ की गवेषणा/समीचीना एषणा और/संकीर्ण-सत्ता की विरेचना/अवश्य करनी है तुम्हें ! अर्थ यह हुआ-/लघुता का त्यजन ही
गुरुता का यजन ही/शुभ का सृजन है।" (पृ. ५१) 'मूकमाटी' के माध्यम से कवि ने श्रम, संयम और तप:साधना की आध्यात्मिक त्रिवेणी के रूप में श्रमणसंस्कृति की अमर गाथा प्रस्तुत करते हुए कहा है :
"कंकरों की प्रार्थना सुनकर/माटी की मुस्कान मुखरित हुई : संयम की राह चलो/राही बनना ही तो/हीरा बनना है, स्वयं राही शब्द ही/विलोम-रूप से कह रहा हैराही ही "रा/और/इतना कठोर बनना होगा/कि तन और मन को/तप की आग में/तपा-तपा कर जला-जला कर/राख करना होगा/यतना घोर करना होगा
तभी कहीं चेतन-आत्मा/खरा उतरेगा।" (पृ. ५६-५७) 'शब्द सो बोध नहीं : बोध सो शोध नहीं नामक द्वितीय खण्ड में कवि ने जहाँ काव्य रसों को सार्थक रूप में परिभाषित करते हुए प्रस्तुत किया है, वहीं कवि ने अपनी सरस्वती-सम लेखनी के द्वारा शीत, वसन्तादि ऋतुओं का विवेचन अपने विवेच्य विषय के माध्यम से बड़े ही सहज तथा मनोज्ञ भाव से किया है । तीव्र शीतकाल की रात में भी एक मात्र सूत का सस्ता चादर तन पर डाल कर शिल्पी कुम्भकार रात्रि को व्यतीत कर रहा है । तभी माटी करुणावश शिल्पी से कह उठती है :
"काया तो काया है/जड़ की छाया-माया है/लगती है जाया-सी..
सो"/कम से कम एक कम्बल तो"/काया पर ले लो ना !" (पृ. ९२) माटी के इस कथन पर शिल्पी कुम्भकार का पुरुषार्थपूर्ण सहज आत्मबल जाग उठता है और वह माटी से