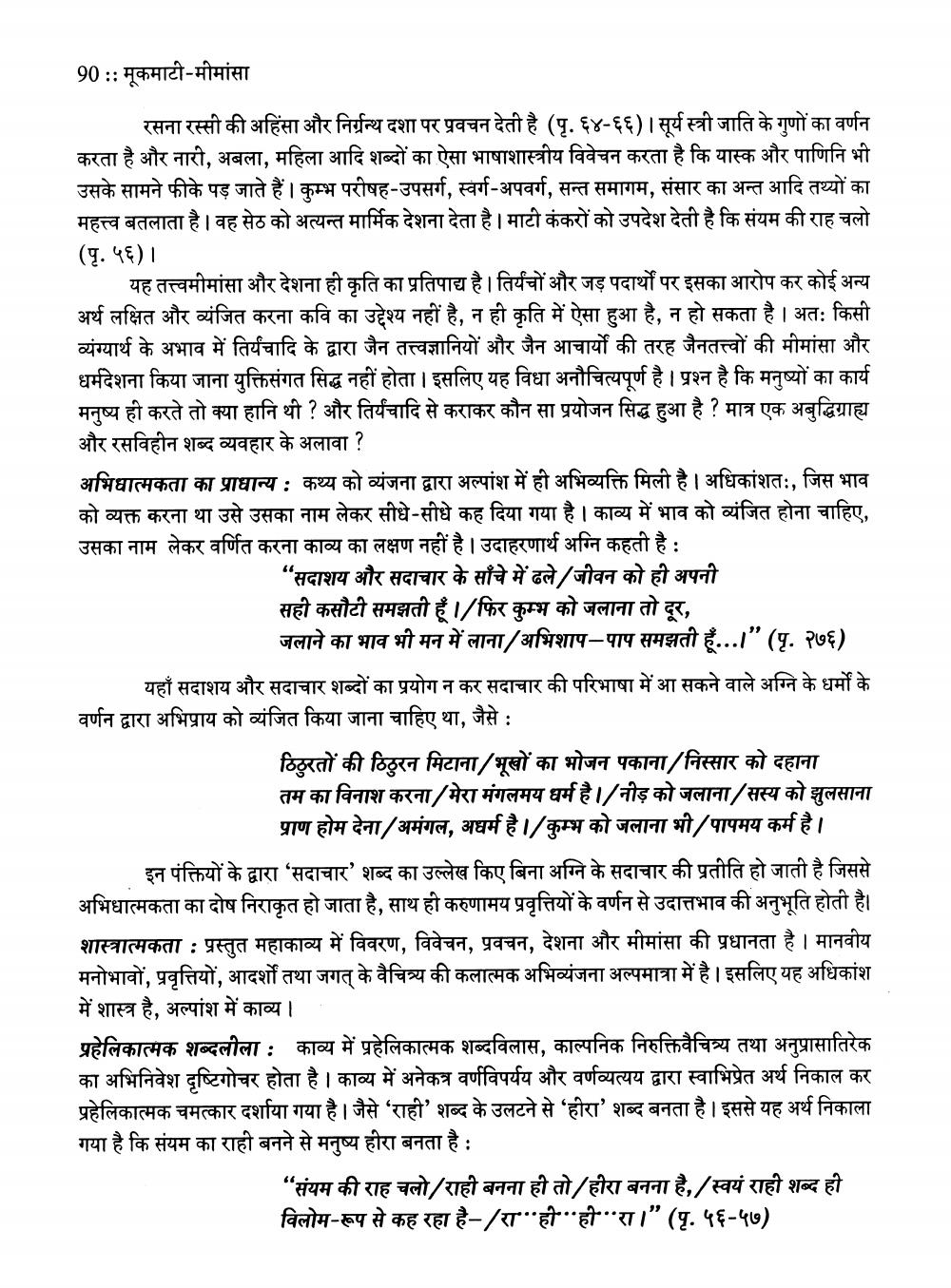________________
90 :: मूकमाटी-मीमांसा
रसना रस्सी की अहिंसा और निर्ग्रन्थ दशा पर प्रवचन देती है (पृ. ६४-६६ ) । सूर्य स्त्री जाति के गुणों का वर्णन करता है और नारी अबला, महिला आदि शब्दों का ऐसा भाषाशास्त्रीय विवेचन करता है कि यास्क और पाणिनि भी उसके सामने फीके पड़ जाते हैं। कुम्भ परीषह-उपसर्ग, स्वर्ग-अपवर्ग, सन्त समागम, संसार का अन्त आदि तथ्यों का महत्त्व बतलाता है । वह सेठ को अत्यन्त मार्मिक देशना देता है। माटी कंकरों को उपदेश देती है कि संयम की राह चलो (पृ. ५६) ।
यह तत्त्वमीमांसा और देशना ही कृति का प्रतिपाद्य है। तिर्यंचों और जड़ पदार्थों पर इसका आरोप कर कोई अन्य अर्थ लक्षित और व्यंजित करना कवि का उद्देश्य नहीं है, न ही कृति में ऐसा हुआ है, न हो सकता है । अतः किसी व्यंग्यार्थ के अभाव में तिर्यंचादि के द्वारा जैन तत्त्वज्ञानियों और जैन आचार्यों की तरह जैनतत्त्वों की मीमांसा और धर्मदेशना किया जाना युक्तिसंगत सिद्ध नहीं होता। इसलिए यह विधा अनौचित्यपूर्ण है । प्रश्न है कि मनुष्यों का कार्य मनुष्य ही करते तो क्या हानि थी ? और तिर्यंचादि से कराकर कौन सा प्रयोजन सिद्ध हुआ है ? मात्र एक अबुद्धिग्राह्य और रसविहीन शब्द व्यवहार के अलावा ?
अभिधात्मकता का प्राधान्य : कथ्य को व्यंजना द्वारा अल्पांश में ही अभिव्यक्ति मिली है । अधिकांशतः, जिस भाव को व्यक्त करना था उसे उसका नाम लेकर सीधे-सीधे कह दिया गया है। काव्य में भाव को व्यंजित होना चाहिए, उसका नाम लेकर वर्णित करना काव्य का लक्षण नहीं है । उदाहरणार्थ अग्नि कहती है :
66
"सदाशय और सदाचार के साँचे में ढले / जीवन को ही अपनी
सही कसौटी समझती हूँ // फिर कुम्भ को जलाना तो दूर,
जलाने का भाव भी मन में लाना / अभिशाप - - पाप समझती हूँ... ।” (पृ. २७६)
यहाँ सदाशय और सदाचार शब्दों का प्रयोग न कर सदाचार की परिभाषा में आ सकने वाले अग्नि के धर्मों के वर्णन द्वारा अभिप्राय को व्यंजित किया जाना चाहिए था, जैसे :
ठिठुरतों की ठिठुरन मिटाना / भूखों का भोजन पकाना / निस्सार को दहाना
तम का विनाश करना/ मेरा मंगलमय धर्म है । / नीड़ को जलाना / सस्य को झुलसाना प्राण होम देना / अमंगल, अधर्म है । / कुम्भ को जलाना भी / पापमय कर्म है ।
इन पंक्तियों के द्वारा 'सदाचार' शब्द का उल्लेख किए बिना अग्नि के सदाचार की प्रतीति हो जाती है जिससे अभिधात्मकता का दोष निराकृत हो जाता है, साथ ही करुणामय प्रवृत्तियों के वर्णन से उदात्तभाव की अनुभूति होती है। शास्त्रात्मकता : प्रस्तुत महाकाव्य में विवरण, विवेचन, प्रवचन, देशना और मीमांसा की प्रधानता है । मानवीय मनोभावों, प्रवृत्तियों, आदर्शों तथा जगत् के वैचित्र्य की कलात्मक अभिव्यंजना अल्पमात्रा में है। इसलिए यह अधिकांश शास्त्र है, अल्पांश में काव्य ।
प्रहेलिकात्मक शब्दलीला : काव्य में प्रहेलिकात्मक शब्दविलास, काल्पनिक निरुक्तिवैचित्र्य तथा अनुप्रासातिरेक का अभिनिवेश दृष्टिगोचर होता है । काव्य में अनेकत्र वर्णविपर्यय और वर्णव्यत्यय द्वारा स्वाभिप्रेत अर्थ निकाल कर प्रहेलिकात्मक चमत्कार दर्शाया गया है। जैसे 'राही' शब्द के उलटने से 'हीरा' शब्द बनता है। इससे यह अर्थ निकाला गया है कि संयम का राही बनने से मनुष्य हीरा बनता है।
:
"संयम की राह चलो / राही बनना ही तो / हीरा बनना है, / स्वयं राही शब्द ही विलोम-रूप से कह रहा है - / रा" ही हीरा ।” (पृ. ५६-५७)