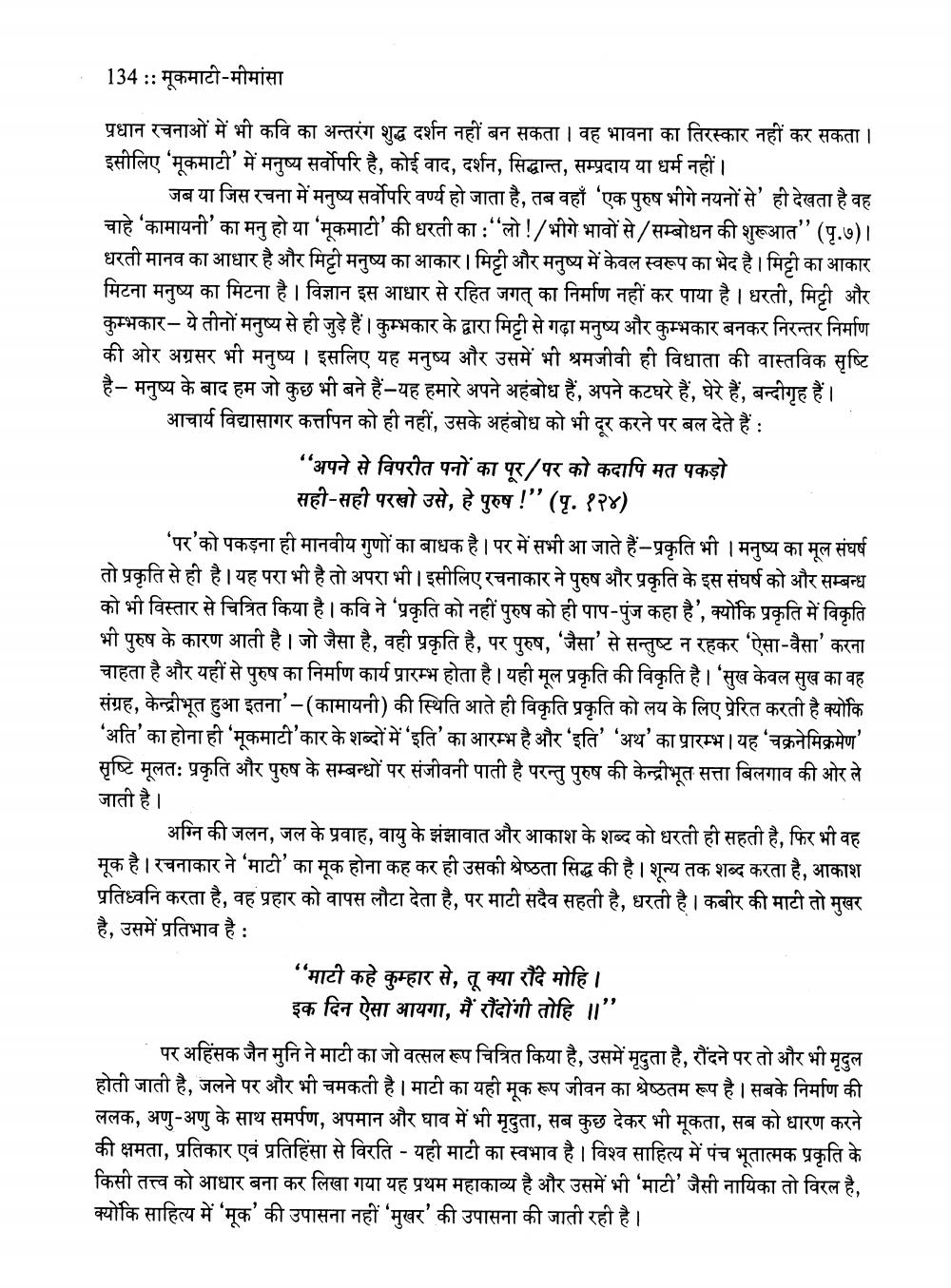________________
134 :: मूकमाटी-मीमांसा
प्रधान रचनाओं में भी कवि का अन्तरंग शुद्ध दर्शन नहीं बन सकता । वह भावना का तिरस्कार नहीं कर सकता । इसीलिए 'मूकमाटी' में मनुष्य सर्वोपरि है, कोई वाद, दर्शन, सिद्धान्त, सम्प्रदाय या धर्म नहीं ।
जब या जिस रचना में मनुष्य सर्वोपरि वर्ण्य हो जाता है, तब वहाँ 'एक पुरुष भीगे नयनों से' ही देखता है वह चाहे 'कामायनी' का मनु हो या 'मूकमाटी' की धरती का : "लो ! / भीगे भावों से / सम्बोधन की शुरूआत " (पृ.७)। धरती मानव का आधार है और मिट्टी मनुष्य का आकार । मिट्टी और मनुष्य में केवल स्वरूप का भेद है। मिट्टी का आकार मिटना मनुष्य का मिटना है। विज्ञान इस आधार से रहित जगत् का निर्माण नहीं कर पाया है। धरती, मिट्टी और कुम्भकार- - ये तीनों मनुष्य से ही जुड़े हैं । कुम्भकार के द्वारा मिट्टी से गढ़ा मनुष्य और कुम्भकार बनकर निरन्तर निर्माण की ओर अग्रसर भी मनुष्य । इसलिए यह मनुष्य और उसमें भी श्रमजीवी ही विधाता की वास्तविक सृष्टि है - मनुष्य के बाद हम जो कुछ भी बने हैं - यह हमारे अपने अहंबोध हैं, अपने कटघरे हैं, घेरे हैं, बन्दीगृह हैं।
आचार्य विद्यासागर कर्त्तापन को ही नहीं, उसके अहंबोध को भी दूर करने पर बल देते हैं :
"अपने से विपरीत पनों का पूर/ पर को कदापि मत पकड़ो सही-सही परखो उसे, हे पुरुष !" (पृ. १२४)
'पर'को पकड़ना ही मानवीय गुणों का बाधक है। पर में सभी आ जाते हैं - प्रकृति भी । मनुष्य का मूल संघर्ष
तो प्रकृति से ही है । यह परा भी है तो अपरा भी । इसीलिए रचनाकार ने पुरुष और प्रकृति के इस संघर्ष को और सम्बन्ध को भी विस्तार से चित्रित किया है । कवि ने 'प्रकृति को नहीं पुरुष को ही पाप-पुंज कहा है', क्योंकि प्रकृति में विकृति भी पुरुष के कारण आती है। जो जैसा है, वही प्रकृति है, पर पुरुष, 'जैसा' से सन्तुष्ट न रहकर 'ऐसा-वैसा' करना चाहता है और यहीं से पुरुष का निर्माण कार्य प्रारम्भ होता है। यही मूल प्रकृति की विकृति है । 'सुख केवल सुख का वह संग्रह, केन्द्रीभूत हुआ इतना' - ( कामायनी) की स्थिति आते ही विकृति प्रकृति को लय के लिए प्रेरित करती है क्योंकि 'अति' का होना ही 'मूकमाटी' कार के शब्दों में 'इति' का आरम्भ है और 'इति' 'अथ' का प्रारम्भ । यह 'चक्रनेमिक्रमेण' सृष्टि मूलत: प्रकृति और पुरुष के सम्बन्धों पर संजीवनी पाती है परन्तु पुरुष की केन्द्रीभूत सत्ता बिलगाव की ओर ले जाती है ।
अग्नि की जलन, जल के प्रवाह, वायु के झंझावात और आकाश के शब्द को धरती ही सहती है, फिर भी वह मूक है। रचनाकार ने 'माटी' का मूक होना कह कर ही उसकी श्रेष्ठता सिद्ध की है। शून्य तक शब्द करता है, आ प्रतिध्वनि करता है, वह प्रहार को वापस लौटा देता है, पर माटी सदैव सहती है, धरती है। कबीर की माटी तो मुखर है, उसमें प्रतिभाव है :
"माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रौदै मोहि । इक दिन ऐसा आयगा, मैं रौंदोंगी तोहि ॥ "
पर अहिंसक जैन मुनि ने माटी का जो वत्सल रूप चित्रित किया है, उसमें मृदुता है, रौंदने पर तो और भी मृदुल होती जाती है, जलने पर और भी चमकती है। माटी का यही मूक रूप जीवन का श्रेष्ठतम रूप है। सबके निर्माण की ललक, अणु-अणु के साथ समर्पण, अपमान और घाव में भी मृदुता, सब कुछ देकर भी मूकता, सब को धारण करने की क्षमता, प्रतिकार एवं प्रतिहिंसा से विरति - यही माटी का स्वभाव है । विश्व साहित्य में पंच भूतात्मक प्रकृति के किसी तत्त्व को आधार बना कर लिखा गया यह प्रथम महाकाव्य है और उसमें भी 'माटी' जैसी नायिका तो विरल है, क्योंकि साहित्य में 'मूक' की उपासना नहीं 'मुखर' की उपासना की जाती रही है ।