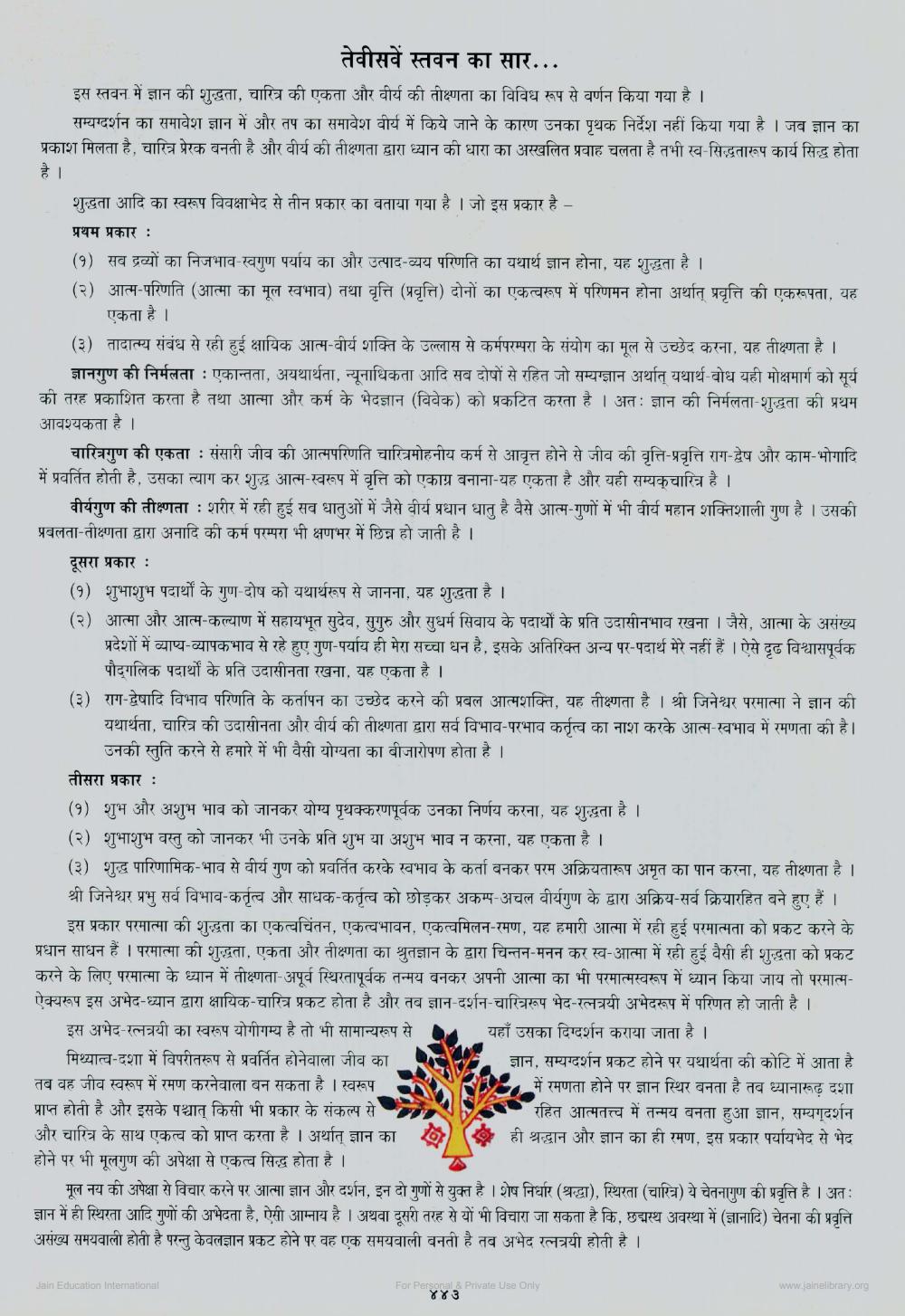________________
तेवीसवें स्तवन का सार... इस स्तवन में ज्ञान की शुद्धता, चारित्र की एकता और वीर्य की तीक्ष्णता का विविध रूप से वर्णन किया गया है ।
सम्यग्दर्शन का समावेश ज्ञान में और तप का समावेश वीर्य में किये जाने के कारण उनका पृथक निर्देश नहीं किया गया है । जब ज्ञान का प्रकाश मिलता है, चारित्र प्रेरक बनती है और वीर्य की तीक्ष्णता द्वारा ध्यान की धारा का अस्खलित प्रवाह चलता है तभी स्व-सिद्धतारूप कार्य सिद्ध होता
शुद्धता आदि का स्वरूप विवक्षाभेद से तीन प्रकार का बताया गया है | जो इस प्रकार है - प्रथम प्रकार : (१) सब द्रव्यों का निजभाव-स्वगुण पर्याय का और उत्पाद-व्यय परिणति का यथार्थ ज्ञान होना, यह शुद्धता है । (२) आत्म-परिणति (आत्मा का मूल स्वभाव) तथा वृत्ति (प्रवृत्ति) दोनों का एकत्वरूप में परिणमन होना अर्थात् प्रवृत्ति की एकरूपता, यह
एकता है। (३) तादात्य संबंध से रही हुई क्षायिक आत्म-वीर्य शक्ति के उल्लास से कर्मपरम्परा के संयोग का मूल से उच्छेद करना, यह तीक्ष्णता है ।
ज्ञानगुण की निर्मलता : एकान्तता, अयथार्थता, न्यूनाधिकता आदि सब दोषों से रहित जो सम्यग्ज्ञान अर्थात् यथार्थ बोध यही मोक्षमार्ग को सूर्य की तरह प्रकाशित करता है तथा आत्मा और कर्म के भेदज्ञान (विवेक) को प्रकटित करता है । अतः ज्ञान की निर्मलता-शुद्धता की प्रथम आवश्यकता है ।
चारित्रगुण की एकता : संसारी जीव की आत्मपरिणति चारित्रमोहनीय कर्म से आवृत्त होने से जीव की वृत्ति-प्रवृत्ति राग-द्वेष और काम-भोगादि में प्रवर्तित होती है, उसका त्याग कर शुद्ध आत्म-स्वरूप में वृत्ति को एकाग्र बनाना-यह एकता है और यही सम्यक्चारित्र है ।
वीर्यगुण की तीक्ष्णता : शरीर में रही हुई सब धातुओं में जैसे वीर्य प्रधान धातु है वैसे आत्म-गुणों में भी वीर्य महान शक्तिशाली गुण है । उसकी प्रबलता-तीक्ष्णता द्वारा अनादि की कर्म परम्परा भी क्षणभर में छिन्न हो जाती है ।
दूसरा प्रकार : (१) शुभाशुभ पदार्थों के गुण-दोष को यथार्थरूप से जानना, यह शुद्धता है । (२) आत्मा और आत्म-कल्याण में सहायभूत सुदेव, सुगुरु और सुधर्म सिवाय के पदार्थों के प्रति उदासीनभाव रखना । जैसे, आत्मा के असंख्य
प्रदेशों में व्याप्य-व्यापकभाव से रहे हुए गुण-पर्याय ही मेरा सच्चा धन है, इसके अतिरिक्त अन्य पर-पदार्थ मेरे नहीं हैं । ऐसे दृढ विश्वासपूर्वक
पौद्गलिक पदार्थों के प्रति उदासीनता रखना, यह एकता है । (३) राग-द्वेषादि विभाव परिणति के कर्तापन का उच्छेद करने की प्रबल आत्मशक्ति, यह तीक्ष्णता है । श्री जिनेश्वर परमात्मा ने ज्ञान की
यथार्थता, चारित्र की उदासीनता और वीर्य की तीक्ष्णता द्वारा सर्व विभाव-परभाव कर्तृत्व का नाश करके आत्म-स्वभाव में रमणता की है।
उनकी स्तुति करने से हमारे में भी वैसी योग्यता का बीजारोपण होता है । तीसरा प्रकार : (१) शुभ और अशुभ भाव को जानकर योग्य पृथक्करणपूर्वक उनका निर्णय करना, यह शुद्धता है । (२) शुभाशुभ वस्तु को जानकर भी उनके प्रति शुभ या अशुभ भाव न करना, यह एकता है । (३) शुद्ध पारिणामिक-भाव से वीर्य गुण को प्रवर्तित करके स्वभाव के कर्ता बनकर परम अक्रियतारूप अमृत का पान करना, यह तीक्ष्णता है | श्री जिनेश्वर प्रभु सर्व विभाव-कर्तृत्व और साधक-कर्तृत्व को छोड़कर अकम्प-अचल वीर्यगुण के द्वारा अक्रिय-सर्व क्रियारहित बने हुए हैं ।
इस प्रकार परमात्मा की शुद्धता का एकत्वचिंतन, एकत्वभावन, एकत्वमिलन-रमण, यह हमारी आत्मा में रही हुई परमात्मता को प्रकट करने के प्रधान साधन हैं । परमात्मा की शुद्धता, एकता और तीक्ष्णता का श्रुतज्ञान के द्वारा चिन्तन-मनन कर स्व-आत्मा में रही हुई वैसी ही शुद्धता को प्रकट करने के लिए परमात्मा के ध्यान में तीक्ष्णता-अपूर्व स्थिरतापूर्वक तन्मय बनकर अपनी आत्मा का भी परमात्मस्वरूप में ध्यान किया जाय तो परमात्मऐक्यरूप इस अभेद-ध्यान द्वारा क्षायिक-चारित्र प्रकट होता है और तब ज्ञान-दर्शन-चारित्ररूप भेद-रत्नत्रयी अभेदरूप में परिणत हो जाती है ।
इस अभेद-रत्नत्रयी का स्वरूप योगीगम्य है तो भी सामान्यरूप से यहाँ उसका दिग्दर्शन कराया जाता है। मिथ्यात्व-दशा में विपरीतरूप से प्रवर्तित होनेवाला जीव का
ज्ञान, सम्यग्दर्शन प्रकट होने पर यथार्थता की कोटि में आता है तब वह जीव स्वरूप में रमण करनेवाला बन सकता है । स्वरूप
में रमणता होने पर ज्ञान स्थिर बनता है तब ध्यानारूढ़ दशा प्राप्त होती है और इसके पश्चात् किसी भी प्रकार के संकल्प से
रहित आत्मतत्त्व में तन्मय बनता हुआ ज्ञान, सम्यग्दर्शन और चारित्र के साथ एकत्व को प्राप्त करता है । अर्थात् ज्ञान का
ही श्रद्धान और ज्ञान का ही रमण, इस प्रकार पर्यायभेद से भेद होने पर भी मूलगुण की अपेक्षा से एकत्व सिद्ध होता है ।
मूल नय की अपेक्षा से विचार करने पर आत्मा ज्ञान और दर्शन, इन दो गुणों से युक्त है । शेष निर्धार (श्रद्धा), स्थिरता (चारित्र) ये चेतनागुण की प्रवृत्ति है । अतः ज्ञान में ही स्थिरता आदि गुणों की अभेदता है, ऐसी आम्नाय है । अथवा दूसरी तरह से यों भी विचारा जा सकता है कि, छद्मस्थ अवस्था में (ज्ञानादि) चेतना की प्रवृत्ति असंख्य समयवाली होती है परन्तु केवलज्ञान प्रकट होने पर वह एक समयवाली बनती है तब अभेद रत्नत्रयी होती है ।
वाला बन सकता है । स्वरूप
Jain Education International
For Peru
Private Use Only
www.jainelibrary.org