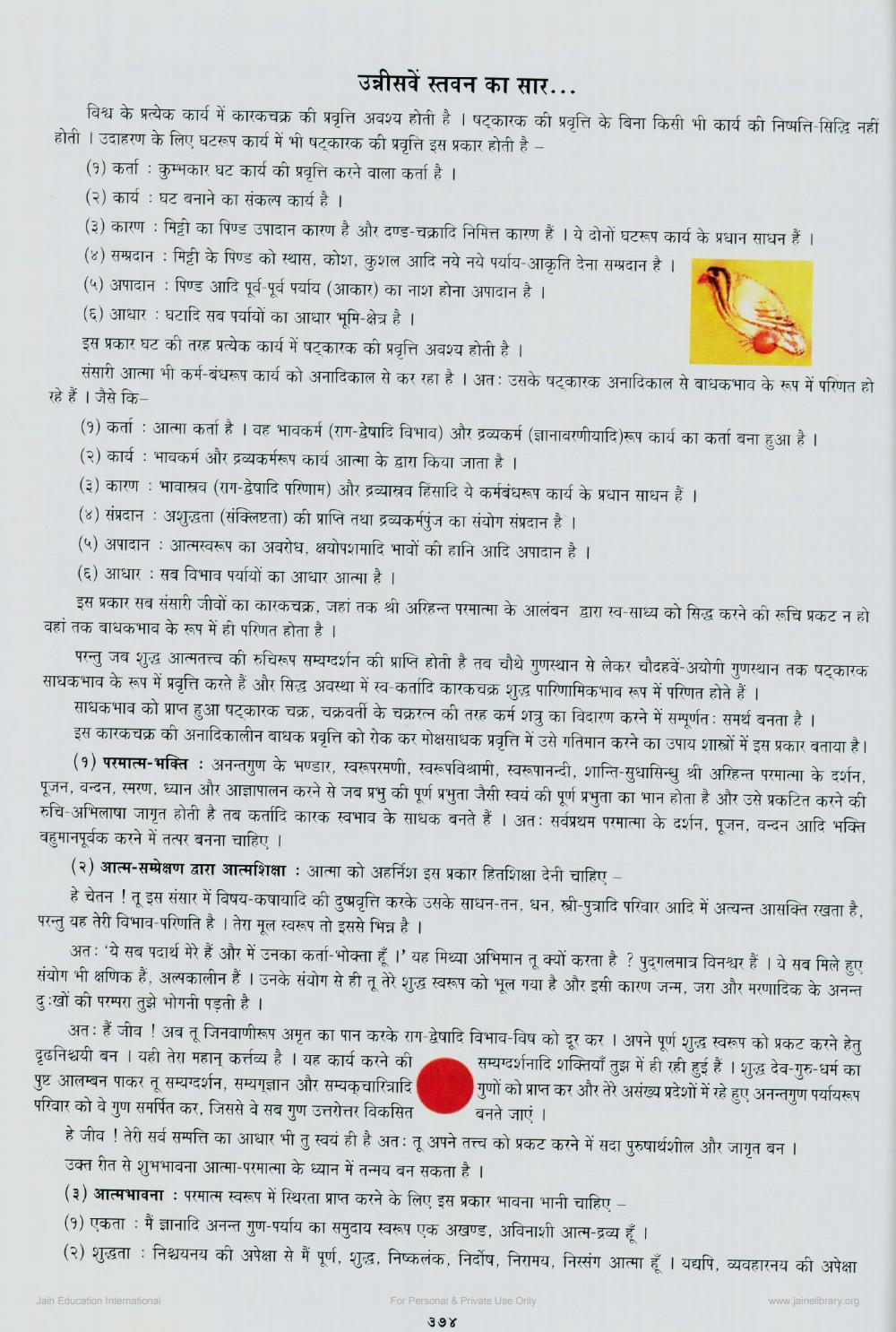________________
उन्नीसवें स्तवन का सार...
विश्व के प्रत्येक कार्य में कारकचक्र की प्रवृत्ति अवश्य होती है । षट्कारक की प्रवृत्ति के बिना किसी भी कार्य की निष्पत्ति सिद्धि नहीं होती । उदाहरण के लिए घटरूप कार्य में भी षट्कारक की प्रवृत्ति इस प्रकार होती है -
(१) कर्ता : कुम्भकार घट कार्य की प्रवृत्ति करने वाला कर्ता है ।
(२) कार्य घट बनाने का संकल्प कार्य है ।
(३) कारण : मिट्टी का पिण्ड उपादान कारण है और दण्ड-चक्रादि निमित्त कारण हैं । ये दोनों घटरूप कार्य के प्रधान साधन हैं ।
(४) सम्प्रदान : मिट्टी के पिण्ड को स्थास, कोश, कुशल आदि नये नये पर्याय- आकृति देना सम्प्रदान है ।
(५) अपादान : पिण्ड आदि पूर्व-पूर्व पर्याय (आकार) का नाश होना अपादान है ।
(६) आधार: घटादि सब पर्यायों का आधार भूमि क्षेत्र है ।
इस प्रकार घट की तरह प्रत्येक कार्य में षट्कारक की प्रवृत्ति अवश्य होती है ।
संसारी आत्मा भी कर्म-बंधरूप कार्य को अनादिकाल से कर रहा है । अतः उसके षट्कारक अनादिकाल से बाधकभाव के रूप में परिणत हो रहे हैं । जैसे कि
I
(१) कर्ता : आत्मा कर्ता है । वह भावकर्म (राग-द्वेषादि विभाव) और द्रव्यकर्म (ज्ञानावरणीयादि) रूप कार्य का कर्ता बना हुआ है ।
(२) कार्य : भावकर्म और द्रव्यकर्मरूप कार्य आत्मा के द्वारा किया जाता है ।
(३) कारण : भावास्रव (राग-द्वेषादि परिणाम) और द्रव्यास्रव हिंसादि ये कर्मबंधरूप कार्य के प्रधान साधन हैं ।
(४) संप्रदान: अशुद्धता (संक्लिष्टता) की प्राप्ति तथा द्रव्यकर्मपुंज का संयोग संप्रदान है ।
(५) अपादान : आत्मस्वरूप का अवरोध, क्षयोपशमादि भावों की हानि आदि अपादान है ।
(६) आधार: सब विभाव पर्यायों का आधार आत्मा है ।
इस प्रकार सब संसारी जीवों का कारकचक्र, जहां तक श्री अरिहन्त परमात्मा के आलंबन द्वारा स्व-साध्य को सिद्ध करने की रूचि प्रकट न हो वहां तक बाधकभाव के रूप में ही परिणत होता है ।
परन्तु जब शुद्ध आत्मतत्त्व की रुचिरूप सम्यग्दर्शन की प्राप्ति होती है तब चौथे गुणस्थान से लेकर चौदहवें अयोगी गुणस्थान तक षट्कारक साधकभाव के रूप में प्रवृत्ति करते हैं और सिद्ध अवस्था में स्व-कर्तादि कारकचक्र शुद्ध पारिणामिकभाव रूप में परिणत होते हैं ।
साधकभाव को प्राप्त हुआ षट्कारक चक्र, चक्रवर्ती के चक्ररत्न की तरह कर्म शत्रु का विदारण करने में सम्पूर्णत: समर्थ बनता है ।
इस कारकचक्र की अनादिकालीन बाधक प्रवृत्ति को रोक कर मोक्षसाधक प्रवृत्ति में उसे गतिमान करने का उपाय शास्त्रों में इस प्रकार बताया है।
(१) परमात्म-भक्ति : अनन्तगुण के भण्डार, स्वरूपरमणी, स्वरूपविश्रामी, स्वरूपानन्दी, शान्ति-सुधासिन्धु श्री अरिहन्त परमात्मा के दर्शन, पूजन, वन्दन, स्मरण, ध्यान और आज्ञापालन करने से जब प्रभु की पूर्ण प्रभुता जैसी स्वयं की पूर्ण प्रभुता का भान होता है और उसे प्रकटित करने की रुचि- अभिलाषा जागृत होती है तब कर्तादि कारक स्वभाव के साधक बनते हैं । अतः सर्वप्रथम परमात्मा के दर्शन, पूजन, वन्दन आदि भक्ति बहुमानपूर्वक करने में तत्पर बनना चाहिए ।
(२) आत्म-सम्प्रेक्षण द्वारा आत्मशिक्षा: आत्मा को अहर्निश इस प्रकार हितशिक्षा देनी चाहिए
हे चेतन ! तू इस संसार में विषय-कषायादि की दुष्प्रवृत्ति करके उसके साधन-तन, धन, स्त्री-पुत्रादि परिवार आदि में अत्यन्त आसक्ति रखता है, परन्तु यह तेरी विभाव-परिणति है । तेरा मूल स्वरूप तो इससे भिन्न है ।
अतः ‘ये सब पदार्थ मेरे हैं और में उनका कर्ता-भोक्ता हूँ ।' यह मिथ्या अभिमान तू क्यों करता है ? पुद्गलमात्र विनश्वर हैं । ये सब मिले हुए संयोग भी क्षणिक हैं, अल्पकालीन हैं। उनके संयोग से ही तू तेरे शुद्ध स्वरूप को भूल गया है और इसी कारण जन्म, जरा और मरणादिक के अनन्त दुःखों की परम्परा तुझे भोगनी पड़ती है ।
अत: हैं जीव ! अब तू जिनवाणीरूप अमृत का पान करके राग-द्वेषादि विभाव-विष को दूर कर । अपने पूर्ण शुद्ध स्वरूप को प्रकट करने हेतु दृढनिश्चयी बन । यही तेरा महान् कर्त्तव्य है । यह कार्य करने की सम्यग्दर्शनादि शक्तियाँ तुझ में ही रही हुई हैं । शुद्ध देव-गुरु-धर्म का गुणों को प्राप्त कर और तेरे असंख्य प्रदेशों में रहे हुए अनन्तगुण पर्यायरूप बनते जाएं ।
पुष्ट आलम्बन पाकर तू सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्रादि परिवार को वे गुण समर्पित कर, जिससे वे सब गुण उत्तरोत्तर विकसित
हे जीव ! तेरी सर्व सम्पत्ति का आधार भी तु स्वयं ही है अतः तू अपने तत्त्व को प्रकट करने में सदा पुरुषार्थशील और जागृत बन ।
उक्त रीत से शुभभावना आत्मा-परमात्मा के ध्यान में तन्मय बन सकता है ।
(३) आत्मभावना : परमात्म स्वरूप में स्थिरता प्राप्त करने के लिए इस प्रकार भावना भानी चाहिए
(१) एकता : मैं ज्ञानादि अनन्त गुण- पर्याय का समुदाय स्वरूप एक अखण्ड, अविनाशी आत्म-द्रव्य हूँ ।
(२) शुद्धता : निश्चयनय की अपेक्षा से मैं पूर्ण, शुद्ध, निष्कलंक, निर्दोष, निरामय, निस्संग आत्मा हूँ । यद्यपि, व्यवहारनय की अपेक्षा
Jain Education International
For Personal & Private Use Only
७७४
-
www.jainelibrary.org