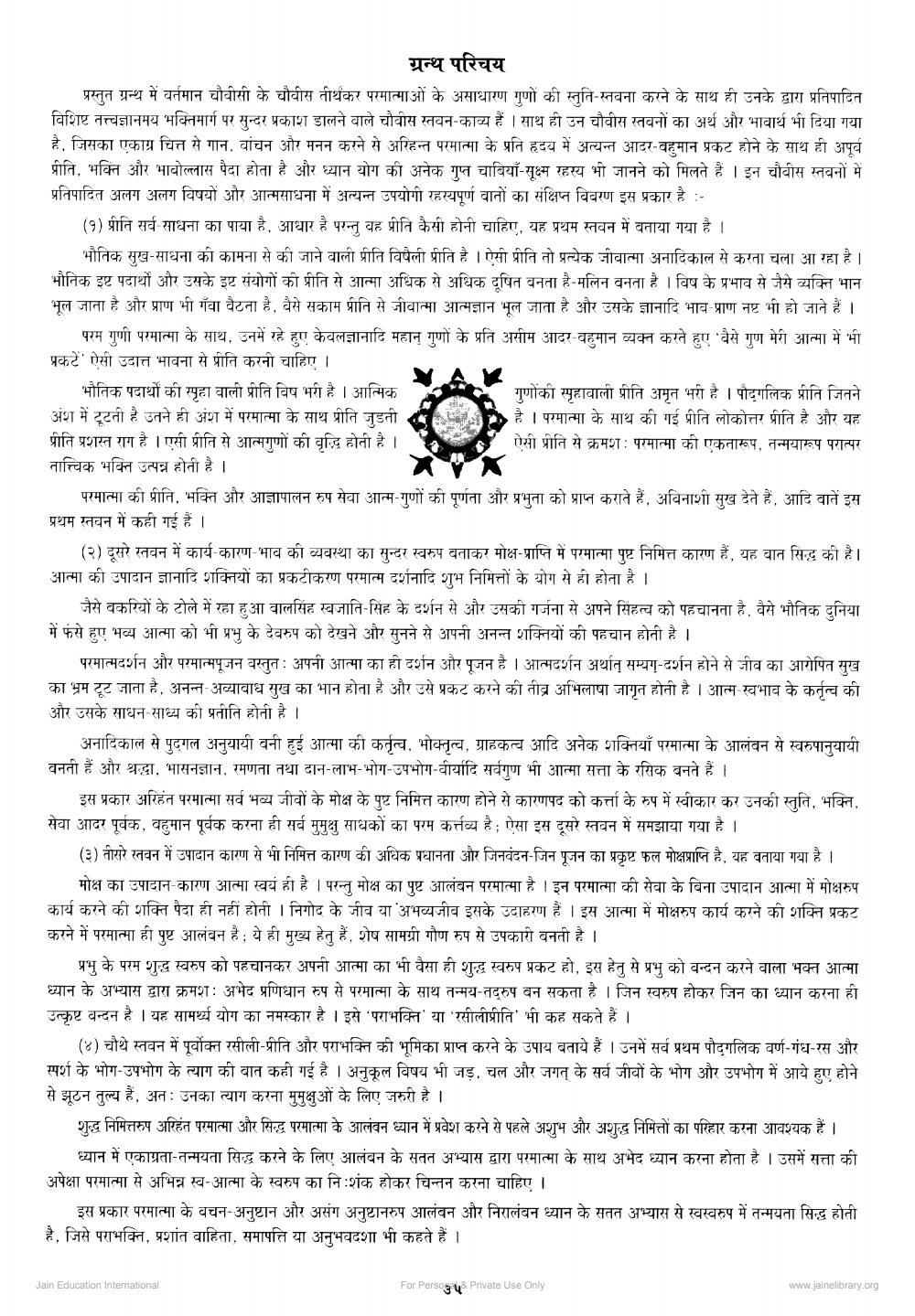________________
ग्रन्थ परिचय
प्रस्तुत ग्रन्थ में वर्तमान चौवीसी के चौवीस तीर्थंकर परमात्माओं के असाधारण गुणों की स्तुति - स्तवना करने के साथ ही उनके द्वारा प्रतिपादित विशिष्ट तत्त्वज्ञानमय भक्तिमार्ग पर सुन्दर प्रकाश डालने वाले चौवीस स्तवन-काव्य हैं। साथ ही उन चौवीस स्तवनों का अर्थ और भावार्थ भी दिया गया है, जिसका एकाग्र चित्त से गान, वांचन और मनन करने से अरिहन्त परमात्मा के प्रति हृदय में अत्यन्त आदर- बहुमान प्रकट होने के साथ ही अपूर्व प्रीति, भक्ति और भावोल्लास पैदा होता है और ध्यान योग की अनेक गुप्त चाबियाँ सूक्ष्म रहस्य भी जानने को मिलते हैं । इन चौवीस स्तवनों में प्रतिपादित अलग अलग विषयों और आत्मसाधना में अत्यन्त उपयोगी रहस्यपूर्ण बातों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है :
(१) प्रीति सर्व साधना का पाया है, आधार है परन्तु वह प्रीति कैसी होनी चाहिए, यह प्रथम स्तवन में बताया गया है ।
भौतिक सुख-साधना की कामना से की जाने वाली प्रीति विषैली प्रीति है । ऐसी प्रीति तो प्रत्येक जीवात्मा अनादिकाल से करता चला आ रहा है भौतिक इष्ट पदार्थों और उसके इष्ट संयोगों की प्रीति से आत्मा अधिक से अधिक दूषित बनता है मलिन बनता है । विष के प्रभाव से जैसे व्यक्ति भान भूल जाता है और प्राण भी गँवा बैठता है, वैसे सकाम प्रीति से जीवात्मा आत्मज्ञान भूल जाता है और उसके ज्ञानादि भाव-प्राण नष्ट भी हो जाते हैं । परम गुणी परमात्मा के साथ, उनमें रहे हुए केवलज्ञानादि महान गुणों के प्रति असीम आदर-बहुमान व्यक्त करते हु "वैसे गुण मेरी आत्मा में भी प्रकटें ऐसी उदात्त भावना से प्रीति करनी चाहिए ।
भौतिक पदार्थों की स्पृहा वाली प्रीति विष भरी है । आत्मिक अंश में टूटती है उतने ही अंश में परमात्मा के साथ प्रीति जुडती प्रीति प्रशस्त राग है । एसी प्रीति से आत्मगुणों की वृद्धि होती है । तात्त्विक भक्ति उत्पन्न होती है ।
गुणोंकी स्पृहावाली प्रीति अमृत भरी है । पौद्गलिक प्रीति जितने है । परमात्मा के साथ की गई प्रीति लोकोत्तर प्रीति है और यह ऐसी प्रीति से क्रमश: परमात्मा की एकतारूप, तन्मयारूप परात्पर
परमात्मा की प्रीति, भक्ति और आज्ञापालन रूप सेवा आत्म- गुणों की पूर्णता और प्रभुता को प्राप्त कराते हैं, अविनाशी सुख देते हैं, आदि वातें इस प्रथम स्तवन में कही गई हैं ।
(२) दूसरे स्तवन में कार्य-कारण-भाव की व्यवस्था का सुन्दर स्वरुप बताकर मोक्ष प्राप्ति में परमात्मा पुष्ट निमित्त कारण हैं, यह बात सिद्ध की है। आत्मा की उपादान ज्ञानादि शक्तियों का प्रकटीकरण परमात्म दर्शनादि शुभ निमित्तों के योग से ही होता है।
1
जैसे बकरियों के टोले में रहा हुआ वालसिंह स्वजाति सिंह के दर्शन से और उसकी गर्जना से अपने सिंहत्व को पहचानता है, वैसे भौतिक दुनिया हुए भव्य आत्मा को भी प्रभु के देवरूप को देखने और सुनने से अपनी अनन्त शक्तियों की पहचान होती है ।
में फंसे
परमात्मदर्शन और परमात्मपूजन वस्तुत: अपनी आत्मा का ही दर्शन और पूजन है । आत्मदर्शन अर्थात् सम्यग् दर्शन होने से जीव का आरोपित सुख का भ्रम टूट जाता है, अनन्त अव्यावाध सुख का भान होता है और उसे प्रकट करने की तीव्र अभिलाषा जागृत होती है । आत्म-स्वभाव के कर्तृत्व की और उसके साधन-साध्य की प्रतीति होती है ।
अनादिकाल से पुद्गल अनुयायी बनी हुई आत्मा की कर्तृत्व, भोक्तृत्व, ग्राहकत्व आदि अनेक शक्तियाँ परमात्मा के आलंबन से स्वरुपानुयायी वनती हैं और श्रद्धा, भासनज्ञान, रमणता तथा दान लाभ- भोग-उपभोग- वीर्यादि सर्वगुण भी आत्मा सत्ता के रसिक बनते हैं ।
इस प्रकार अरिहंत परमात्मा सर्व भव्य जीवों के मोक्ष के पुष्ट निमित्त कारण होने से कारणपद को कर्त्ता के रूप में स्वीकार कर उनकी स्तुति, भक्ति, सेवा आदरपूर्वक, बहुमान पूर्वक करना ही सर्व मुमुक्षु साधकों का परम कर्त्तव्य है; ऐसा इस दूसरे स्तवन में समझाया गया है ।
(३) तीसरे स्तवन में उपादान कारण से भी निमित्त कारण की अधिक प्रधानता और जिनवंदन - जिन पूजन का प्रकृष्ट फल मोक्षप्राप्ति है, यह बताया गया है ।
मोक्ष का उपादान-कारण आत्मा स्वयं ही है । परन्तु मोक्ष का पुष्ट आलंबन परमात्मा है । इन परमात्मा की सेवा के बिना उपादान आत्मा में मोक्षरुप कार्य करने की शक्ति पैदा ही नहीं होती । निगोद के जीव या अभव्यजीव इसके उदाहरण हैं । इस आत्मा में मोक्षरुप कार्य करने की शक्ति प्रकट करने में परमात्मा ही पुष्ट आलंबन है; ये ही मुख्य हेतु हैं, शेष सामग्री गौण रूप से उपकारी बनती है ।
प्रभु के परम शुद्ध स्वरुप को पहचानकर अपनी आत्मा का भी वैसा ही शुद्ध स्वरुप प्रकट हो, इस हेतु से प्रभु को वन्दन करने वाला भक्त आत्मा ध्यान के अभ्यास द्वारा क्रमश: अभेद प्रणिधान रूप से परमात्मा के साथ तन्मय-तद्रुप बन सकता है । जिन स्वरुप होकर जिन का ध्यान करना ही उत्कृष्ट वन्दन है । यह सामर्थ्य योग का नमस्कार है । इसे 'पराभक्ति' या 'रसीलीप्रीति' भी कह सकते हैं ।
(४) चौथे स्तवन में पूर्वोक्त रसीली - प्रीति और पराभक्ति की भूमिका प्राप्त करने के उपाय बताये हैं । उनमें सर्व प्रथम पौद्गलिक वर्ण-गंध-रस और स्पर्श के भोग-उपभोग के त्याग की बात कही गई है। अनुकूल विषय भी जड़, चल और जगत् के सर्व जीवों के भोग और उपभोग में आये हुए होने से झूटन तुल्य हैं, अत: उनका त्याग करना मुमुक्षुओं के लिए जरुरी है ।
शुद्ध निमित्तरूप अरिहंत परमात्मा और सिद्ध परमात्मा के आलंबन ध्यान में प्रवेश करने से पहले अशुभ और अशुद्ध निमित्तों का परिहार करना आवश्यक हैं । ध्यान में एकाग्रता - तन्मयता सिद्ध करने के लिए आलंबन के सतत अभ्यास द्वारा परमात्मा के साथ अभेद ध्यान करना होता है । उसमें सत्ता की अपेक्षा परमात्मा से अभिन्न स्व- आत्मा के स्वरुप का निःशंक होकर चिन्तन करना चाहिए ।
इस प्रकार परमात्मा के वचन- अनुष्टान और असंग अनुष्टानरूप आलंबन और निरालंबन ध्यान के सतत अभ्यास से स्वस्वरुप में तन्मयता सिद्ध होत है, जिसे पराभक्ति, प्रशांत वाहिता समापत्ति या अनुभवदशा भी कहते हैं ।
Jain Education International.
For Perso& Private Use Only
www.jainelibrary.org