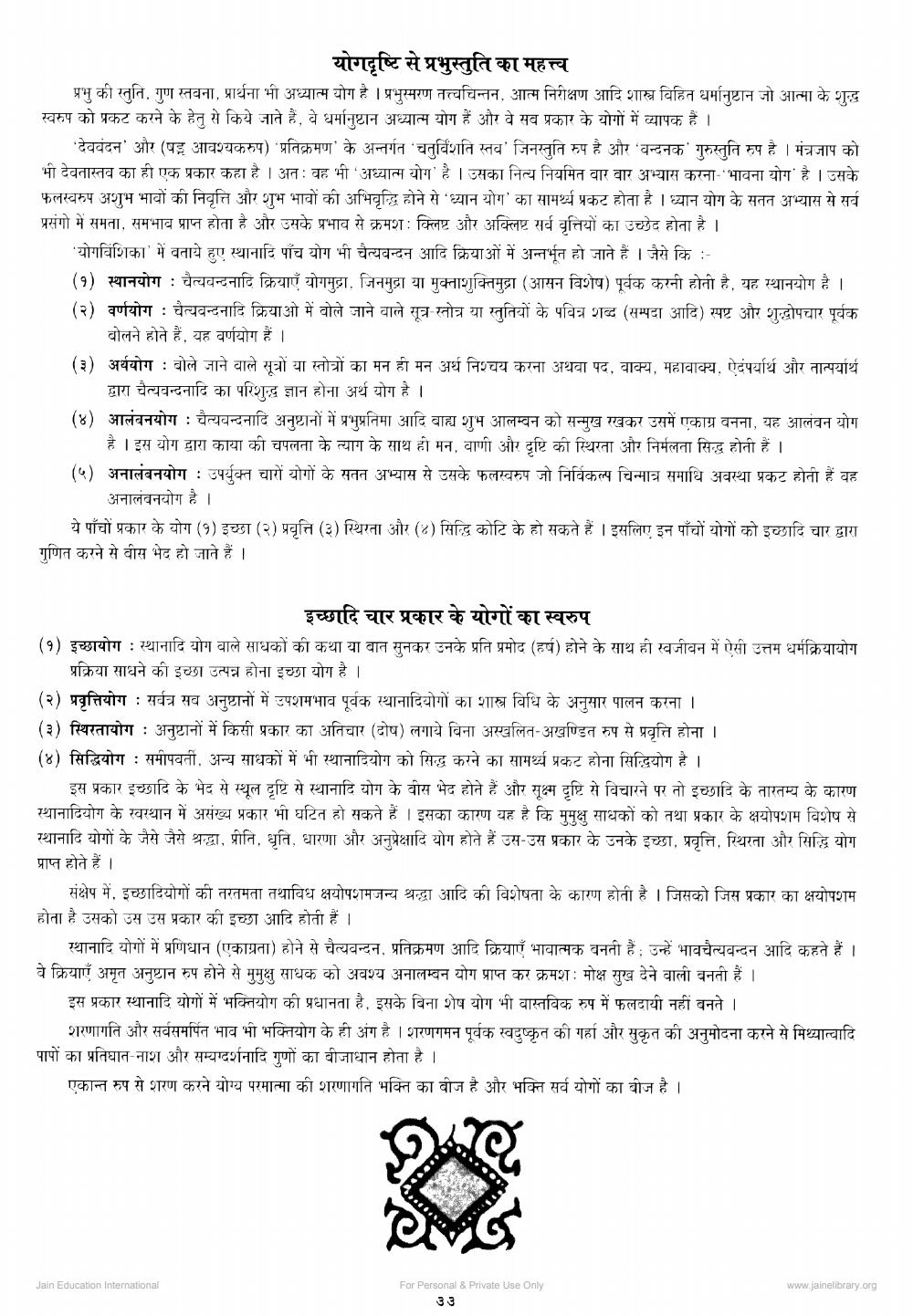________________
योगदृष्टि से प्रभुस्तुति का महत्त्व प्रभु की स्तुति. गुण स्तवना, प्रार्थना भी अध्यात्म योग है । प्रभुस्मरण तत्त्वचिन्तन, आत्म निरीक्षण आदि शास्त्र विहित धर्मानुष्टान जो आत्मा के शुद्ध स्वरुप को प्रकट करने के हेतु से किये जाते हैं, वे धर्मानुष्ठान अध्यात्म योग हैं और वे सब प्रकार के योगों में व्यापक हैं ।
'देववंदन' और (षड़ आवश्यकरुप) प्रतिक्रमण' के अन्तर्गत चतुर्विंशति स्तव' जिनस्तुति रूप है और 'वन्दनक' गुरुस्तुति रुप है । मंत्रजाप को भी देवतास्तव का ही एक प्रकार कहा है । अत : वह भी अध्यात्म योग' है । उसका नित्य नियमित वार वार अभ्यास करना ‘भावना योग' है । उसके फलस्वरुप अशुभ भावों की निवृत्ति और शुभ भावों की अभिवृद्धि होने से 'ध्यान योग' का सामर्थ्य प्रकट होता है । ध्यान योग के सतत अभ्यास से सर्व प्रसंगो में समता, समभाव प्राप्त होता है और उसके प्रभाव से क्रमश: क्लिष्ट और अक्लिष्ट सर्व वृत्तियों का उच्छेद होता है ।
'योगविंशिका' में बताये हुए स्थानादि पाँच योग भी चैत्यवन्दन आदि क्रियाओं में अन्न न हो जाते हैं । जैसे कि :(१) स्थानयोग : चैत्ववन्दनादि क्रियाएँ योगमुद्रा, जिनमुद्रा या मुक्ताशुक्तिमुद्रा (आसन विशेष) पूर्वक करनी होती है, यह स्थानयोग है । (२) वर्णयोग : चैत्यवन्दनादि क्रियाओ में वोले जाने वाले सूत्र स्तोत्र या स्तुतियों के पवित्र शब्द (सम्पदा आदि) स्पष्ट और शुद्धोपचार पूर्वक
बोलने होते हैं, यह वर्णयोग हैं। (३) अर्थयोग : बोले जाने वाले सूत्रों या स्तोत्रों का मन ही मन अर्थ निश्चय करना अथवा पद, वाक्य, महावाक्य, ऐदंपर्यार्थ और तात्पयार्थ
द्वारा चैत्यवन्दनादि का परिशुद्ध ज्ञान होना अर्थ योग है । (४) आलंबनयोग : चैत्यवन्दनादि अनुष्टानों में प्रभुप्रतिमा आदि बाह्य शुभ आलम्वन को सन्मुख रखकर उसमें एकाग्र बनना, यह आलंबन योग
है । इस योग द्वारा काया की चपलता के त्याग के साथ ही मन, वाणी और दृष्टि की स्थिरता और निर्मलता सिद्ध होती हैं। (५) अनालंबनयोग : उपर्युक्त चारों योगों के सतत अभ्यास से उसके फलस्वरुप जो निर्विकल्प चिन्मात्र समाधि अवस्था प्रकट होती हैं वह
अनालंबनयोग है । ये पाँचों प्रकार के योग (१) इच्छा (२) प्रवृत्ति (३) स्थिरता और (४) सिद्धि कोटि के हो सकते हैं । इसलिए इन पाँचों योगों को इच्छादि चार द्वारा गुणित करने से वीस भेद हो जाते हैं ।
इच्छादि चार प्रकार के योगों का स्वरुप (१) इच्छायोग : स्थानादि योग वाले साधकों की कथा या बात सुनकर उनके प्रति प्रमोद (हर्ष) होने के साथ ही स्वजीवन में ऐसी उत्तम धर्मक्रियायोग
प्रक्रिया साधने की इच्छा उत्पन्न होना इच्छा योग है ।। (२) प्रवृत्तियोग : सर्वत्र सब अनुष्ठानों में उपशमभाव पूर्वक स्थानादियोगों का शास्त्र विधि के अनुसार पालन करना । (३) स्थिरतायोग : अनुष्टानों में किसी प्रकार का अतिचार (दोष) लगाये बिना अस्खलित-अखण्डित रूप से प्रवृत्ति होना । (४) सिद्धियोग : समीपवती, अन्य साधकों में भी स्थानादियोग को सिद्ध करने का सामर्थ्य प्रकट होना सिद्धियोग है ।
इस प्रकार इच्छादि के भेद से स्थूल दृष्टि से स्थानादि योग के वीस भेद होते हैं और सूक्ष्म दृष्टि से विचारने पर तो इच्छादि के तारतम्य के कारण स्थानादियोग के स्वस्थान में असंख्य प्रकार भी घटित हो सकते हैं । इसका कारण यह है कि मुमुक्षु साधकों को तथा प्रकार के क्षयोपशम विशेष से स्थानादि योगों के जैसे जैसे श्रद्धा, प्रीति, धृति, धारणा और अनुप्रेक्षादि योग होते हैं उस-उस प्रकार के उनके इच्छा, प्रवृत्ति, स्थिरता और सिद्धि योग प्राप्त होते हैं।
संक्षेप में, इच्छादियोगों की तरतमता तथाविध क्षयोपशमजन्य श्रद्धा आदि की विशेषता के कारण होती है । जिसको जिस प्रकार का क्षयोपशम होता है उसको उस उस प्रकार की इच्छा आदि होती हैं ।
स्थानादि योगों में प्रणिधान (एकाग्रता) होने से चैत्यवन्दन, प्रतिक्रमण आदि क्रियाएँ भावात्मक बनती हैं : उन्हें भावचैत्यवन्दन आदि कहते हैं । वे क्रियाएँ अमृत अनुष्ठान रुप होने से मुमुक्षु साधक को अवश्य अनालम्बन योग प्राप्त कर क्रमशः मोक्ष सुख देने वाली बनती हैं ।
इस प्रकार स्थानादि योगों में भक्तियोग की प्रधानता है, इसके बिना शेष योग भी वास्तविक रुप में फलदायी नहीं बनते ।
शरणागति और सर्वसमर्पित भाव भी भक्तियोग के ही अंग है । शरणगमन पूर्वक स्वदुष्कृत की गर्दा और सुकृत की अनुमोदना करने से मिथ्यात्वादि पापों का प्रतिघात नाश और सम्यग्दर्शनादि गुणों का बीजाधान होता है ।
एकान्त रूप से शरण करने योग्य परमात्मा की शरणागति भक्ति का बीज है और भक्ति सर्व योगों का बीज है ।
Jain Education International
For Personal & Private Use Only
www.jainelibrary.org