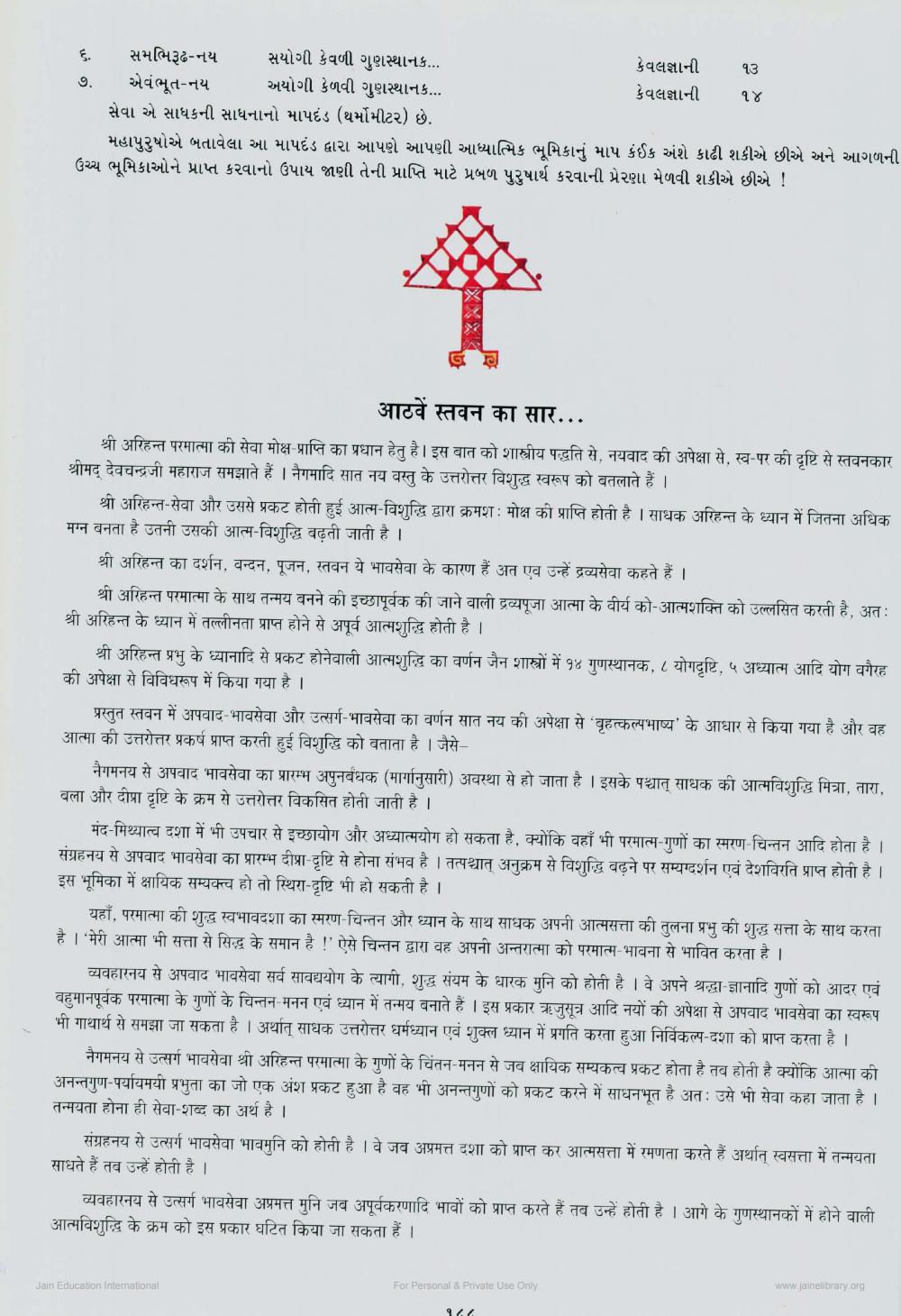________________
१३
६. समभि३८-नय सयोगी वणी गुरास्थान....
કેવલજ્ઞાની ७. मेवभूत-नय योगा वी गुरास्थान...
કેવલજ્ઞાની ૧૪ સેવા એ સાધકની સાધનાનો માપદંડ (થર્મોમીટર) છે.
મહાપુરુષોએ બતાવેલા આ માપદંડ દ્વારા આપણે આપણી આધ્યાત્મિક ભૂમિકાનું માપ કંઈક અંશે કાઢી શકીએ છીએ અને આગળની ઉચ્ચ ભૂમિકાઓને પ્રાપ્ત કરવાનો ઉપાય જાણી તેની પ્રાપ્તિ માટે પ્રબળ પુરુષાર્થ કરવાની પ્રેરણા મેળવી શકીએ છીએ !
आठवें स्तवन का सार... श्री अरिहन्त परमात्मा की सेवा मोक्ष प्राप्ति का प्रधान हेतु है। इस बात को शास्त्रीय पद्धति से, नयवाद की अपेक्षा से, स्व-पर की दृष्टि से स्तवनकार श्रीमद् देवचन्द्रजी महाराज समझाते हैं । नैगमादि सात नय वस्तु के उत्तरोत्तर विशुद्ध स्वरूप को बतलाते हैं ।
श्री अरिहन्त-सेवा और उससे प्रकट होती हुई आत्म-विशुद्धि द्वारा क्रमशः मोक्ष की प्राप्ति होती है । साधक अरिहन्त के ध्यान में जितना अधिक मग्न बनता है उतनी उसकी आत्म-विशुद्धि बढ़ती जाती है ।
श्री अरिहन्त का दर्शन, वन्दन, पूजन, स्तवन ये भावसेवा के कारण हैं अत एव उन्हें द्रव्यसेवा कहते हैं ।
श्री अरिहन्त परमात्मा के साथ तन्मय बनने की इच्छापूर्वक की जाने वाली द्रव्यपूजा आत्मा के वीर्य को-आत्मशक्ति को उल्लसित करती है, अत: श्री अरिहन्त के ध्यान में तल्लीनता प्राप्त होने से अपूर्व आत्मशुद्धि होती है।
श्री अरिहन्त प्रभु के ध्यानादि से प्रकट होनेवाली आत्मशुद्धि का वर्णन जैन शास्त्रों में १४ गुणस्थानक, ८ योगदृष्टि, ५ अध्यात्म आदि योग वगैरह की अपेक्षा से विविधरूप में किया गया है।
प्रस्तुत स्तवन में अपवाद-भावसेवा और उत्सर्ग-भावसेवा का वर्णन सात नय की अपेक्षा से ‘बृहत्कल्पभाष्य' के आधार से किया गया है और वह आत्मा की उत्तरोत्तर प्रकर्ष प्राप्त करती हुई विशुद्धि को बताता है । जैसे
नैगमनय से अपवाद भावसेवा का प्रारम्भ अपुनबंधक (मार्गानुसारी) अवस्था से हो जाता है । इसके पश्चात् साधक की आत्मविशुद्धि मित्रा, तारा, बला और दीपा दृष्टि के क्रम से उत्तरोत्तर विकसित होती जाती है ।
__ मंद-मिथ्यात्व दशा में भी उपचार से इच्छायोग और अध्यात्मयोग हो सकता है, क्योंकि वहाँ भी परमात्म-गुणों का स्मरण-चिन्तन आदि होता है । संग्रहनय से अपवाद भावसेवा का प्रारम्भ दीपा-दृष्टि से होना संभव है । तत्पश्चात् अनुक्रम से विशुद्धि बढ़ने पर सम्यग्दर्शन एवं देशविरति प्राप्त होती है । इस भूमिका में क्षायिक सम्यक्त्व हो तो स्थिरा-दृष्टि भी हो सकती है ।
यहाँ, परमात्मा की शुद्ध स्वभावदशा का स्मरण-चिन्तन और ध्यान के साथ साधक अपनी आत्मसत्ता की तुलना प्रभु की शुद्ध सत्ता के साथ करता है । 'मेरी आत्मा भी सत्ता से सिद्ध के समान है !' ऐसे चिन्तन द्वारा वह अपनी अन्तरात्मा को परमात्म-भावना से भावित करता है ।
व्यवहारनय से अपवाद भावसेवा सर्व सावद्ययोग के त्यागी, शुद्ध संयम के धारक मुनि को होती है । वे अपने श्रद्धा-ज्ञानादि गुणों को आदर एवं बहुमानपूर्वक परमात्मा के गुणों के चिन्तन मनन एवं ध्यान में तन्मय बनाते हैं । इस प्रकार ऋजुसूत्र आदि नयों की अपेक्षा से अपवाद भावसेवा का स्वरूप भी गाथार्थ से समझा जा सकता है । अर्थात् साधक उत्तरोत्तर धर्मध्यान एवं शुक्ल ध्यान में प्रगति करता हुआ निर्विकल्प-दशा को प्राप्त करता है।
नैगमनय से उत्सर्ग भावसेवा श्री अरिहन्त परमात्मा के गुणों के चिंतन-मनन से जब क्षायिक सम्यकत्व प्रकट होता है तब होती है क्योंकि आत्मा की अनन्तगुण-पर्यायमयी प्रभुता का जो एक अंश प्रकट हुआ है वह भी अनन्तगुणों को प्रकट करने में साधनभूत है अत: उसे भी सेवा कहा जाता है । तन्मयता होना ही सेवा-शब्द का अर्थ है ।
संग्रहनय से उत्सर्ग भावसेवा भावमुनि को होती है । वे जब अप्रमत्त दशा को प्राप्त कर आत्मसत्ता में रमणता करते हैं अर्थात् स्वसत्ता में तन्मयता साधते हैं तब उन्हें होती है ।
व्यवहारनय से उत्सर्ग भावसेवा अप्रमत्त मुनि जब अपूर्वकरणादि भावों को प्राप्त करते हैं तब उन्हें होती है । आगे के गणस्थानकों में होने वाली आत्मविशुद्धि के क्रम को इस प्रकार घटित किया जा सकता हैं ।
www.jainelibrary.org
For Personal & Private Use Only
Jain Education International