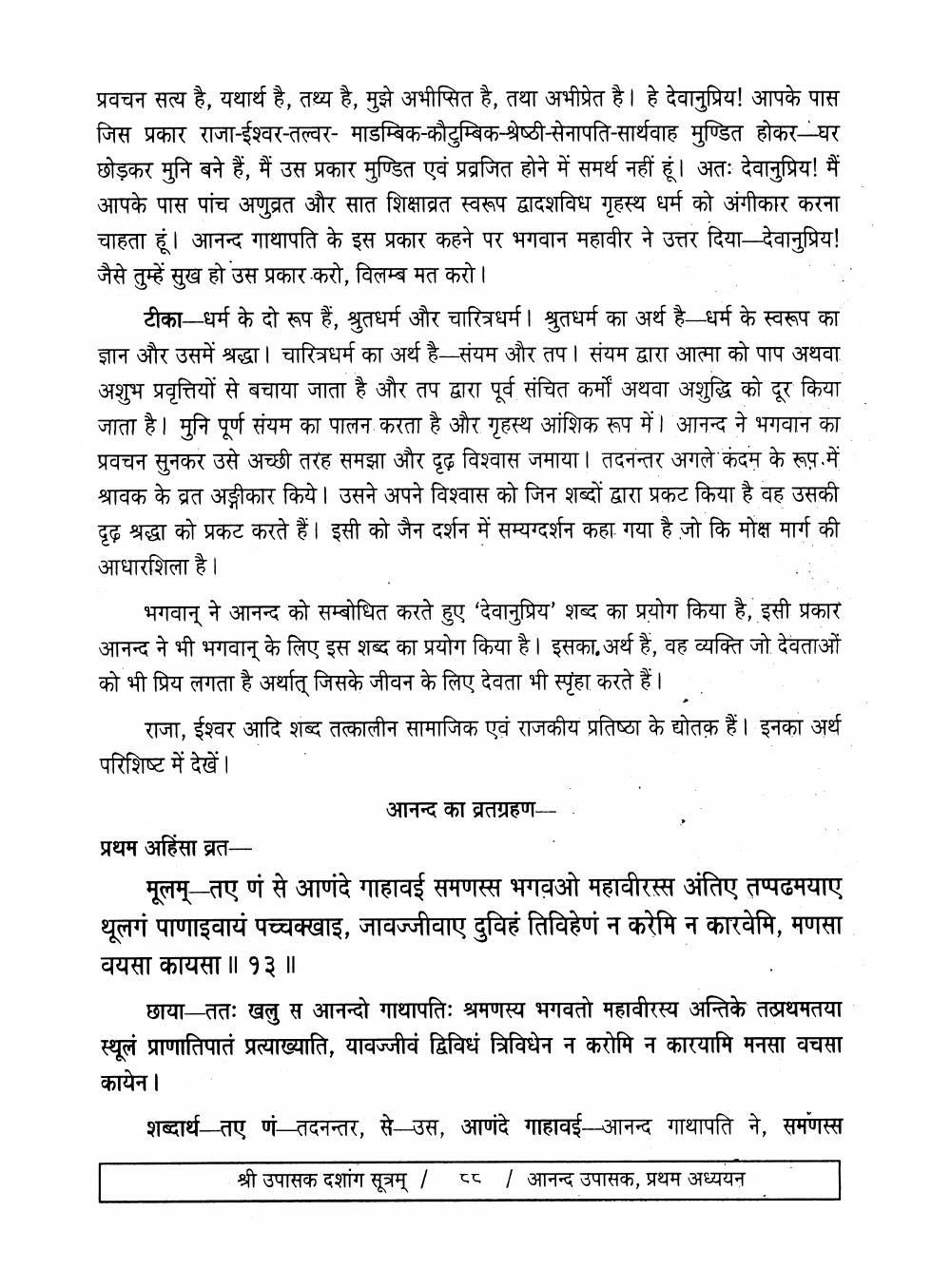________________ प्रवचन सत्य है, यथार्थ है, तथ्य है, मुझे अभीप्सित है, तथा अभीप्रेत है। हे देवानुप्रिय! आपके पास जिस प्रकार राजा-ईश्वर-तल्वर- माडम्बिक-कौटुम्बिक-श्रेष्ठी-सेनापति-सार्थवाह मुण्डित होकर घर छोड़कर मुनि बने हैं, मैं उस प्रकार मुण्डित एवं प्रव्रजित होने में समर्थ नहीं हूं। अतः देवानुप्रिय! मैं आपके पास पांच अणुव्रत और सात शिक्षाव्रत स्वरूप द्वादशविध गृहस्थ धर्म को अंगीकार करना चाहता हूं। आनन्द गाथापति के इस प्रकार कहने पर भगवान महावीर ने उत्तर दिया देवानुप्रिय! जैसे तुम्हें सुख हो उस प्रकार करो, विलम्ब मत करो। टीका—धर्म के दो रूप हैं, श्रुतधर्म और चारित्रधर्म। श्रुतधर्म का अर्थ है—धर्म के स्वरूप का ज्ञान और उसमें श्रद्धा। चारित्रधर्म का अर्थ है—संयम और तप / संयम द्वारा आत्मा को पाप अथवा अशुभ प्रवृत्तियों से बचाया जाता है और तप द्वारा पूर्व संचित कर्मों अथवा अशुद्धि को दूर किया जाता है। मुनि पूर्ण संयम का पालन करता है और गृहस्थ आंशिक रूप में। आनन्द ने भगवान का प्रवचन सुनकर उसे अच्छी तरह समझा और दृढ़ विश्वास जमाया। तदनन्तर अगले कंदम के रूप में श्रावक के व्रत अङ्गीकार किये। उसने अपने विश्वास को जिन शब्दों द्वारा प्रकट किया है वह उसकी दृढ़ श्रद्धा को प्रकट करते हैं। इसी को जैन दर्शन में सम्यग्दर्शन कहा गया है जो कि मोक्ष मार्ग की आधारशिला है। भगवान् ने आनन्द को सम्बोधित करते हुए 'देवानुप्रिय' शब्द का प्रयोग किया है, इसी प्रकार आनन्द ने भी भगवान् के लिए इस शब्द का प्रयोग किया है। इसका. अर्थ है, वह व्यक्ति जो देवताओं को भी प्रिय लगता है अर्थात् जिसके जीवन के लिए देवता भी स्पृहा करते हैं। राजा, ईश्वर आदि शब्द तत्कालीन सामाजिक एवं राजकीय प्रतिष्ठा के द्योतक हैं। इनका अर्थ परिशिष्ट में देखें। आनन्द का व्रतग्रहण- . प्रथम अहिंसा व्रत मूलम् तए णं से आणंदे गाहावई समणस्स भगवओ महावीरस्स अंतिए तप्पढमयाए थूलगं पाणाइवायं पच्चक्खाइ, जावज्जीवाए दुविहं तिविहेणं न करेमि न कारवेमि, मणसा वयसा कायसा // 13 // छाया ततः खलु स आनन्दो गाथापतिः श्रमणस्य भगवतो महावीरस्य अन्तिके तप्रथमतया स्थूलं प्राणातिपातं प्रत्याख्याति, यावज्जीवं द्विविधं त्रिविधेन न करोमि न कारयामि मनसा वचसा कायेन। शब्दार्थ तए णं तदनन्तर, से—उस, आणंदे गाहावई—आनन्द गाथापति ने, समणस्स | श्री उपासक दशांग सूत्रम् | 88 / आनन्द उपासक, प्रथम अध्ययन