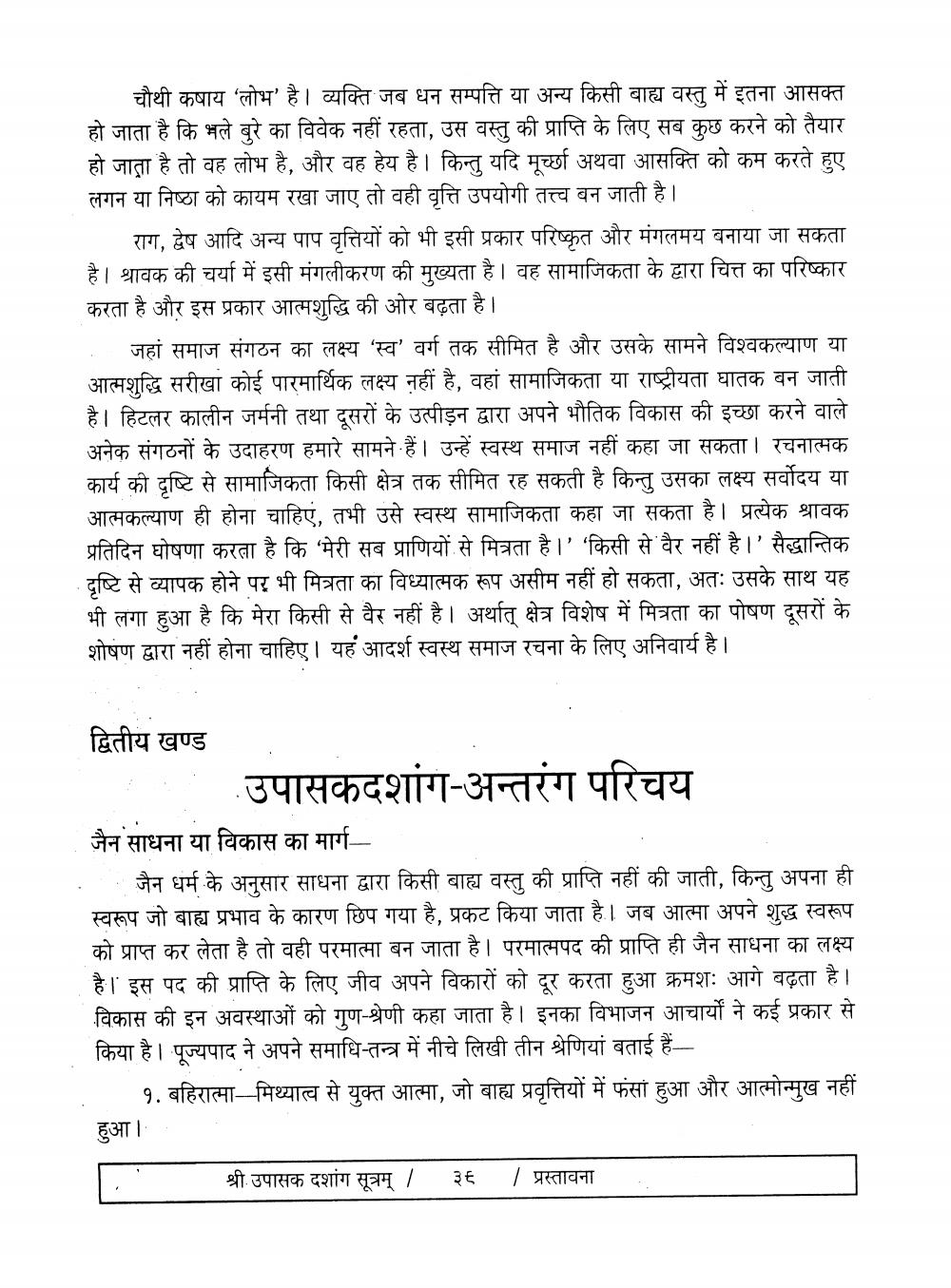________________ चौथी कषाय 'लोभ' है। व्यक्ति जब धन सम्पत्ति या अन्य किसी बाह्य वस्तु में इतना आसक्त हो जाता है कि भले बुरे का विवेक नहीं रहता, उस वस्तु की प्राप्ति के लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाता है तो वह लोभ है, और वह हेय है। किन्तु यदि मूर्छा अथवा आसक्ति को कम करते हुए लगन या निष्ठा को कायम रखा जाए तो वही वृत्ति उपयोगी तत्त्व बन जाती है। राग, द्वेष आदि अन्य पाप वृत्तियों को भी इसी प्रकार परिष्कृत और मंगलमय बनाया जा सकता है। श्रावक की चर्या में इसी मंगलीकरण की मुख्यता है। वह सामाजिकता के द्वारा चित्त का परिष्कार करता है और इस प्रकार आत्मशुद्धि की ओर बढ़ता है। ___ जहां समाज संगठन का लक्ष्य 'स्व' वर्ग तक सीमित है और उसके सामने विश्वकल्याण या आत्मशुद्धि सरीखा कोई पारमार्थिक लक्ष्य नहीं है, वहां सामाजिकता या राष्ट्रीयता घातक बन जाती है। हिटलर कालीन जर्मनी तथा दूसरों के उत्पीड़न द्वारा अपने भौतिक विकास की इच्छा करने वाले अनेक संगठनों के उदाहरण हमारे सामने हैं। उन्हें स्वस्थ समाज नहीं कहा जा सकता। रचनात्मक कार्य की दृष्टि से सामाजिकता किसी क्षेत्र तक सीमित रह सकती है किन्तु उसका लक्ष्य सर्वोदय या आत्मकल्याण ही होना चाहिए, तभी उसे स्वस्थ सामाजिकता कहा जा सकता है। प्रत्येक श्रावक प्रतिदिन घोषणा करता है कि 'मेरी सब प्राणियों से मित्रता है।' 'किसी से वैर नहीं है।' सैद्धान्तिक दृष्टि से व्यापक होने पर भी मित्रता का विध्यात्मक रूप असीम नहीं हो सकता, अतः उसके साथ यह भी लगा हुआ है कि मेरा किसी से वैर नहीं है। अर्थात् क्षेत्र विशेष में मित्रता का पोषण दूसरों के शोषण द्वारा नहीं होना चाहिए। यह आदर्श स्वस्थ समाज रचना के लिए अनिवार्य है। द्वितीय खण्ड उपासकदशांग-अन्तरंग परिचय जैन साधना या विकास का मार्ग - जैन धर्म के अनुसार साधना द्वारा किसी बाह्य वस्तु की प्राप्ति नहीं की जाती, किन्तु अपना ही स्वरूप जो बाह्य प्रभाव के कारण छिप गया है, प्रकट किया जाता है। जब आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप को प्राप्त कर लेता है तो वही परमात्मा बन जाता है। परमात्मपद की प्राप्ति ही जैन साधना का लक्ष्य है। इस पद की प्राप्ति के लिए जीव अपने विकारों को दूर करता हुआ क्रमशः आगे बढ़ता है। विकास की इन अवस्थाओं को गुण-श्रेणी कहा जाता है। इनका विभाजन आचार्यों ने कई प्रकार से किया है। पूज्यपाद ने अपने समाधि-तन्त्र में नीचे लिखी तीन श्रेणियां बताई हैं 1. बहिरात्मा–मिथ्यात्व से युक्त आत्मा, जो बाह्य प्रवृत्तियों में फंसा हुआ और आत्मोन्मुख नहीं हुआ। | श्री उपासक दशांग सूत्रम् / 36 / प्रस्तावना /