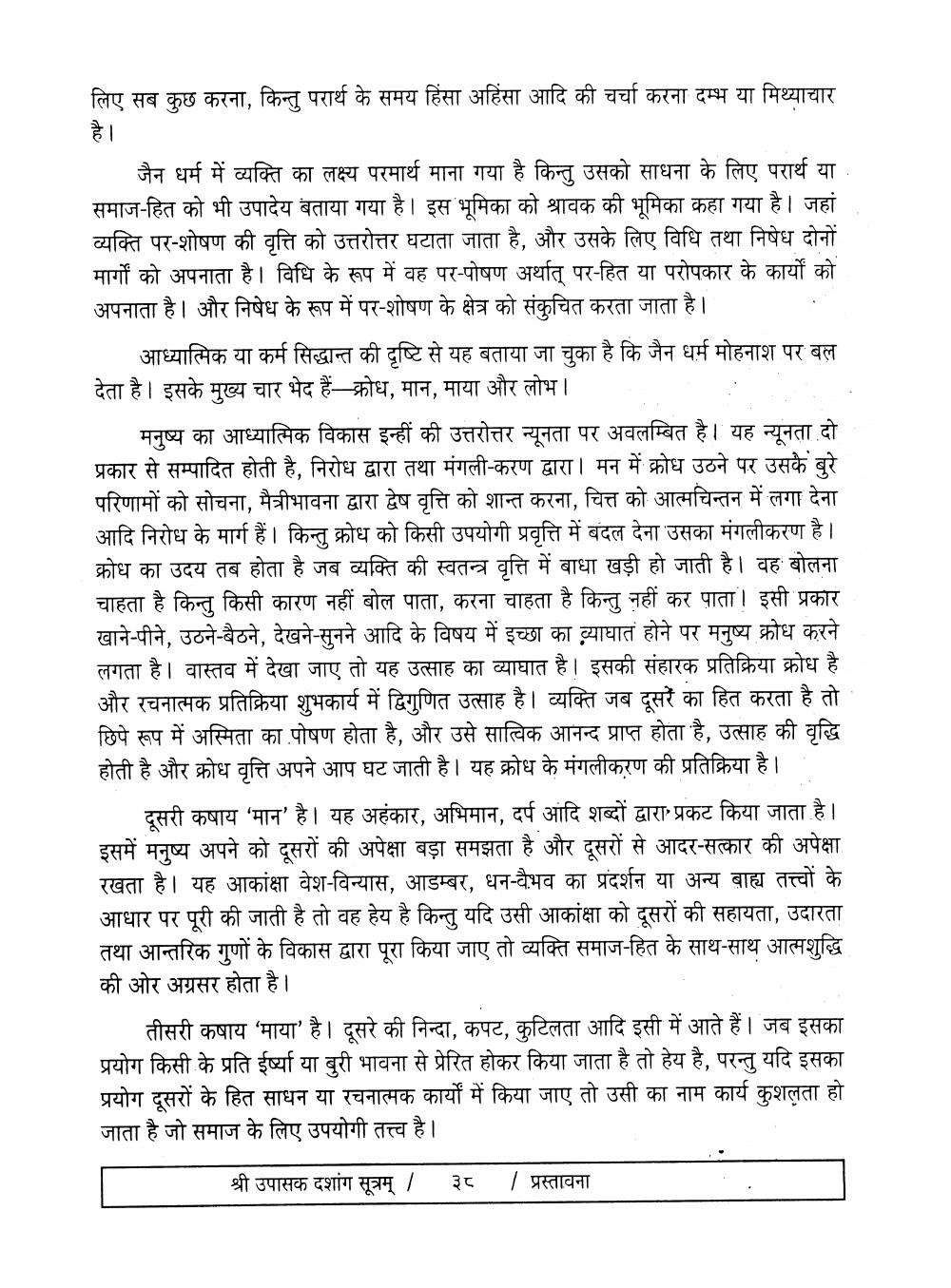________________ लिए सब कुछ करना, किन्तु परार्थ के समय हिंसा अहिंसा आदि की चर्चा करना दम्भ या मिथ्याचार है। जैन धर्म में व्यक्ति का लक्ष्य परमार्थ माना गया है किन्तु उसको साधना के लिए परार्थ या समाज-हित को भी उपादेय बताया गया है। इस भूमिका को श्रावक की भूमिका कहा गया है। जहां व्यक्ति पर-शोषण की वृत्ति को उत्तरोत्तर घटाता जाता है, और उसके लिए विधि तथा निषेध दोनों मार्गों को अपनाता है। विधि के रूप में वह पर-पोषण अर्थात् पर-हित या परोपकार के कार्यों को अपनाता है। और निषेध के रूप में पर-शोषण के क्षेत्र को संकुचित करता जाता है। आध्यात्मिक या कर्म सिद्धान्त की दृष्टि से यह बताया जा चुका है कि जैन धर्म मोहनाश पर बल देता है। इसके मुख्य चार भेद हैं—क्रोध, मान, माया और लोभ / मनुष्य का आध्यात्मिक विकास इन्हीं की उत्तरोत्तर न्यूनता पर अवलम्बित है। यह न्यूनता दो प्रकार से सम्पादित होती है, निरोध द्वारा तथा मंगली-करण द्वारा। मन में क्रोध उठने पर उसके बुरे परिणामों को सोचना, मैत्रीभावना द्वारा द्वेष वृत्ति को शान्त करना, चित्त को आत्मचिन्तन में लगा देना आदि निरोध के मार्ग हैं। किन्तु क्रोध को किसी उपयोगी प्रवृत्ति में बदल देना उसका मंगलीकरण है। क्रोध का उदय तब होता है जब व्यक्ति की स्वतन्त्र वृत्ति में बाधा खड़ी हो जाती है। वह बोलना चाहता है किन्तु किसी कारण नहीं बोल पाता, करना चाहता है किन्तु नहीं कर पाता। इसी प्रकार खाने-पीने, उठने-बैठने, देखने-सुनने आदि के विषय में इच्छा का व्याघात होने पर मनुष्य क्रोध करने लगता है। वास्तव में देखा जाए तो यह उत्साह का व्याघात है। इसकी संहारक प्रतिक्रिया क्रोध है और रचनात्मक प्रतिक्रिया शुभकार्य में द्विगुणित उत्साह है। व्यक्ति जब दूसरे का हित करता है तो छिपे रूप में अस्मिता का पोषण होता है, और उसे सात्विक आनन्द प्राप्त होता है, उत्साह की वृद्धि होती है और क्रोध वृत्ति अपने आप घट जाती है। यह क्रोध के मंगलीकरण की प्रतिक्रिया है। दूसरी कषाय 'मान' है। यह अहंकार, अभिमान, दर्प आदि शब्दों द्वारा प्रकट किया जाता है / इसमें मनुष्य अपने को दूसरों की अपेक्षा बड़ा समझता है और दूसरों से आदर-सत्कार की अपेक्षा रखता है। यह आकांक्षा वेश-विन्यास, आडम्बर, धन-वैभव का प्रदर्शन या अन्य बाह्य तत्त्वों के आधार पर पूरी की जाती है तो वह हेय है किन्तु यदि उसी आकांक्षा को दूसरों की सहायता, उदारता तथा आन्तरिक गुणों के विकास द्वारा पूरा किया जाए तो व्यक्ति समाज-हित के साथ-साथ आत्मशुद्धि की ओर अग्रसर होता है। तीसरी कषाय 'माया' है। दूसरे की निन्दा, कपट, कुटिलता आदि इसी में आते हैं। जब इसका प्रयोग किसी के प्रति ईर्ष्या या बुरी भावना से प्रेरित होकर किया जाता है तो हेय है, परन्तु यदि इसका प्रयोग दूसरों के हित साधन या रचनात्मक कार्यों में किया जाए तो उसी का नाम कार्य कुशलता हो जाता है जो समाज के लिए उपयोगी तत्त्व है। श्री उपासक दशांग सूत्रम् / 38 / प्रस्तावना