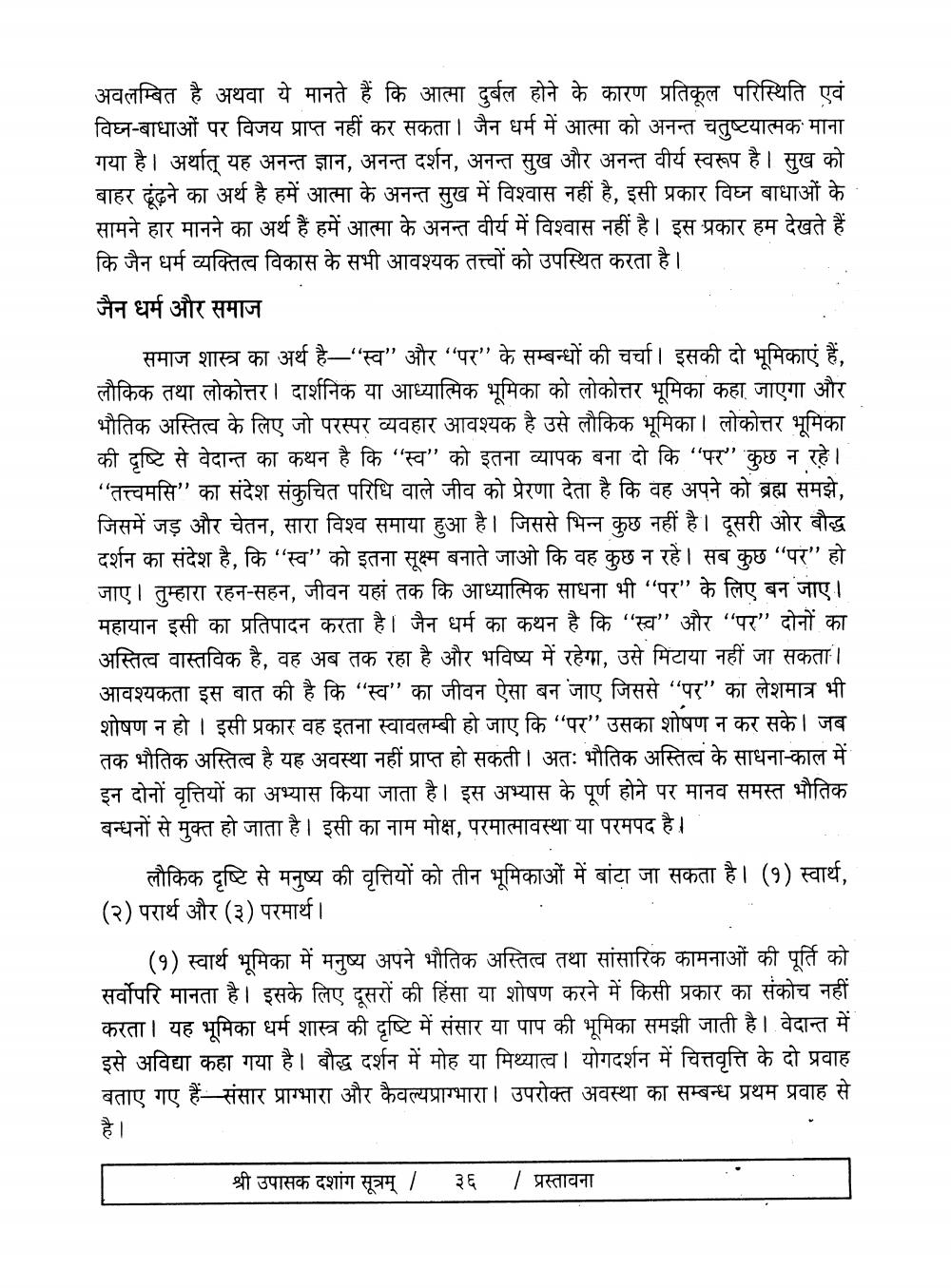________________ अवलम्बित है अथवा ये मानते हैं कि आत्मा दुर्बल होने के कारण प्रतिकूल परिस्थिति एवं विघ्न-बाधाओं पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। जैन धर्म में आत्मा को अनन्त चतुष्टयात्मक माना गया है। अर्थात् यह अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन, अनन्त सुख और अनन्त वीर्य स्वरूप है। सुख को बाहर ढूंढ़ने का अर्थ है हमें आत्मा के अनन्त सुख में विश्वास नहीं है, इसी प्रकार विघ्न बाधाओं के सामने हार मानने का अर्थ हैं हमें आत्मा के अनन्त वीर्य में विश्वास नहीं है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जैन धर्म व्यक्तित्व विकास के सभी आवश्यक तत्त्वों को उपस्थित करता है। जैन धर्म और समाज समाज शास्त्र का अर्थ है—“स्व” और “पर” के सम्बन्धों की चर्चा / इसकी दो भूमिकाएं हैं, लौकिक तथा लोकोत्तर / दार्शनिक या आध्यात्मिक भूमिका को लोकोत्तर भूमिका कहा जाएगा और भौतिक अस्तित्व के लिए जो परस्पर व्यवहार आवश्यक है उसे लौकिक भूमिका / लोकोत्तर भूमिका की दृष्टि से वेदान्त का कथन है कि “स्व” को इतना व्यापक बना दो कि “पर” कुछ न रहे। "तत्त्वमसि' का संदेश संकुचित परिधि वाले जीव को प्रेरणा देता है कि वह अपने को ब्रह्म समझे, जिसमें जड़ और चेतन, सारा विश्व समाया हुआ है। जिससे भिन्न कुछ नहीं है। दूसरी ओर बौद्ध दर्शन का संदेश है, कि “स्व” को इतना सूक्ष्म बनाते जाओ कि वह कुछ न रहे। सब कुछ “पर” हो जाए। तुम्हारा रहन-सहन, जीवन यहां तक कि आध्यात्मिक साधना भी “पर" के लिए बन जाए। महायान इसी का प्रतिपादन करता है। जैन धर्म का कथन है कि “स्व” और “पर” दोनों का अस्तित्व वास्तविक है, वह अब तक रहा है और भविष्य में रहेगा, उसे मिटाया नहीं जा सक आवश्यकता इस बात की है कि “स्व'' का जीवन ऐसा बन जाए जिससे “पर” का लेशमात्र भी शोषण न हो / इसी प्रकार वह इतना स्वावलम्बी हो जाए कि “पर” उसका शोषण न कर सके। जब तक भौतिक अस्तित्व है यह अवस्था नहीं प्राप्त हो सकती। अतः भौतिक अस्तित्व के साधना-काल में इन दोनों वृत्तियों का अभ्यास किया जाता है। इस अभ्यास के पूर्ण होने पर मानव समस्त भौतिक बन्धनों से मुक्त हो जाता है। इसी का नाम मोक्ष, परमात्मावस्था या परमपद है। लौकिक दृष्टि से मनुष्य की वृत्तियों को तीन भूमिकाओं में बांटा जा सकता है। (1) स्वार्थ, (2) परार्थ और (3) परमार्थ। (1) स्वार्थ भूमिका में मनुष्य अपने भौतिक अस्तित्व तथा सांसारिक कामनाओं की पूर्ति को सर्वोपरि मानता है। इसके लिए दूसरों की हिंसा या शोषण करने में किसी प्रकार का संकोच नहीं करता। यह भमिका धर्म शास्त्र की दष्टि में संसार या पाप की भमिका समझी जाती है। वेदान्त में इसे अविद्या कहा गया है। बौद्ध दर्शन में मोह या मिथ्यात्व। योगदर्शन में चित्तवृत्ति के दो प्रवाह बताए गए हैं—संसार प्राग्भारा और कैवल्यप्राग्भारा। उपरोक्त अवस्था का सम्बन्ध प्रथम प्रवाह से है। श्री उपासक दशा म् / 36 / प्रस्तावना