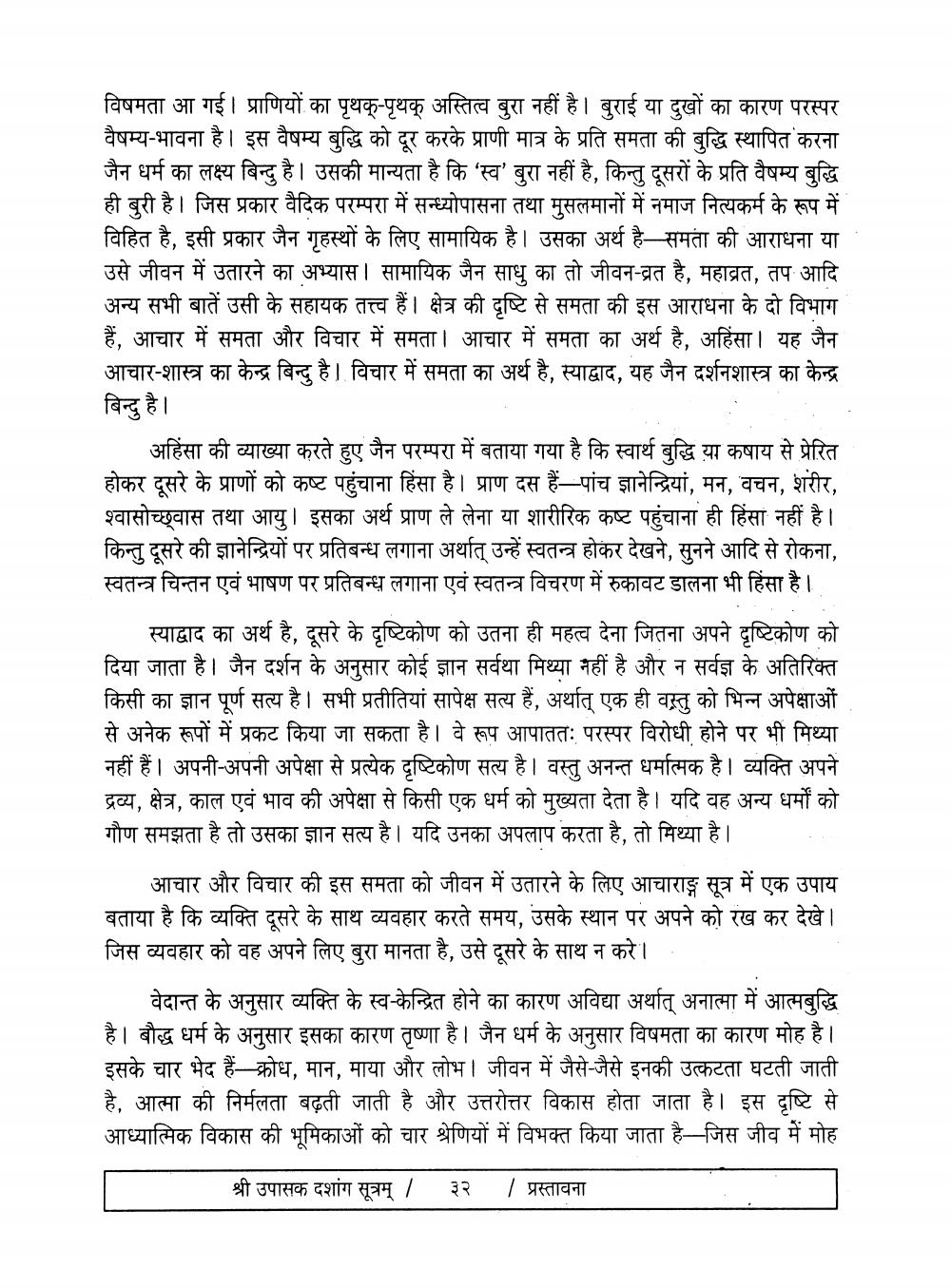________________ विषमता आ गई। प्राणियों का पृथक्-पृथक् अस्तित्व बुरा नहीं है। बुराई या दुखों का कारण परस्पर वैषम्य-भावना है। इस वैषम्य बुद्धि को दूर करके प्राणी मात्र के प्रति समता की बुद्धि स्थापित करना जैन धर्म का लक्ष्य बिन्दु है। उसकी मान्यता है कि 'स्व' बुरा नहीं है, किन्तु दूसरों के प्रति वैषम्य बुद्धि ही बुरी है। जिस प्रकार वैदिक परम्परा में सन्ध्योपासना तथा मुसलमानों में नमाज नित्यकर्म के रूप में विहित है, इसी प्रकार जैन गृहस्थों के लिए सामायिक है। उसका अर्थ है–समता की आराधना या उसे जीवन में उतारने का अभ्यास / सामायिक जैन साधु का तो जीवन-व्रत है, महाव्रत, तप आदि अन्य सभी बातें उसी के सहायक तत्त्व हैं। क्षेत्र की दृष्टि से समता की इस आराधना के दो विभाग हैं, आचार में समता और विचार में समता। आचार में समता का अर्थ है, अहिंसा / यह जैन आचार-शास्त्र का केन्द्र बिन्दु है। विचार में समता का अर्थ है, स्याद्वाद, यह जैन दर्शनशास्त्र का केन्द्र बिन्दु है। ___ अहिंसा की व्याख्या करते हुए जैन परम्परा में बताया गया है कि स्वार्थ बुद्धि या कषाय से प्रेरित होकर दूसरे के प्राणों को कष्ट पहुंचाना हिंसा है। प्राण दस हैं—पांच ज्ञानेन्द्रियां, मन, वचन, शरीर, श्वासोच्छ्वास तथा आयु। इसका अर्थ प्राण ले लेना या शारीरिक कष्ट पहुंचाना ही हिंसा नहीं है / किन्तु दूसरे की ज्ञानेन्द्रियों पर प्रतिबन्ध लगाना अर्थात् उन्हें स्वतन्त्र होकर देखने, सुनने आदि से रोकना, स्वतन्त्र चिन्तन एवं भाषण पर प्रतिबन्ध लगाना एवं स्वतन्त्र विचरण में रुकावट डालना भी हिंसा है। स्याद्वाद का अर्थ है, दूसरे के दृष्टिकोण को उतना ही महत्व देना जितना अपने दृष्टिकोण को दिया जाता है। जैन दर्शन के अनुसार कोई ज्ञान सर्वथा मिथ्या नहीं है और न सर्वज्ञ के अतिरिक्त किसी का ज्ञान पूर्ण सत्य है। सभी प्रतीतियां सापेक्ष सत्य हैं, अर्थात् एक ही वस्तु को भिन्न अपेक्षाओं से अनेक रूपों में प्रकट किया जा सकता है। वे रूप आपाततः परस्पर विरोधी होने पर भी मिथ्या नहीं हैं। अपनी-अपनी अपेक्षा से प्रत्येक दृष्टिकोण सत्य है। वस्तु अनन्त धर्मात्मक है। व्यक्ति अपने द्रव्य, क्षेत्र, काल एवं भाव की अपेक्षा से किसी एक धर्म को मुख्यता देता है। यदि वह अन्य धर्मों को गौण समझता है तो उसका ज्ञान सत्य है। यदि उनका अपलाप करता है, तो मिथ्या है | आचार और विचार की इस समता को जीवन में उतारने के लिए आचाराङ्ग सूत्र में एक उपाय बताया है कि व्यक्ति दूसरे के साथ व्यवहार करते समय, उसके स्थान पर अपने को रख कर देखे / जिस व्यवहार को वह अपने लिए बुरा मानता है, उसे दूसरे के साथ न करे। वेदान्त के अनुसार व्यक्ति के स्व-केन्द्रित होने का कारण अविद्या अर्थात् अनात्मा में आत्मबुद्धि है। बौद्ध धर्म के अनुसार इसका कारण तृष्णा है। जैन धर्म के अनुसार विषमता का कारण मोह है। इसके चार भेद हैं—क्रोध, मान, माया और लोभ / जीवन में जैसे-जैसे इनकी उत्कटता घटती जाती है, आत्मा की निर्मलता बढ़ती जाती है और उत्तरोत्तर विकास होता जाता है। इस दृष्टि से आध्यात्मिक विकास की भूमिकाओं को चार श्रेणियों में विभक्त किया जाता है—जिस जीव में मोह श्री उपासक दशांग सूत्रम् / 32 / प्रस्तावना