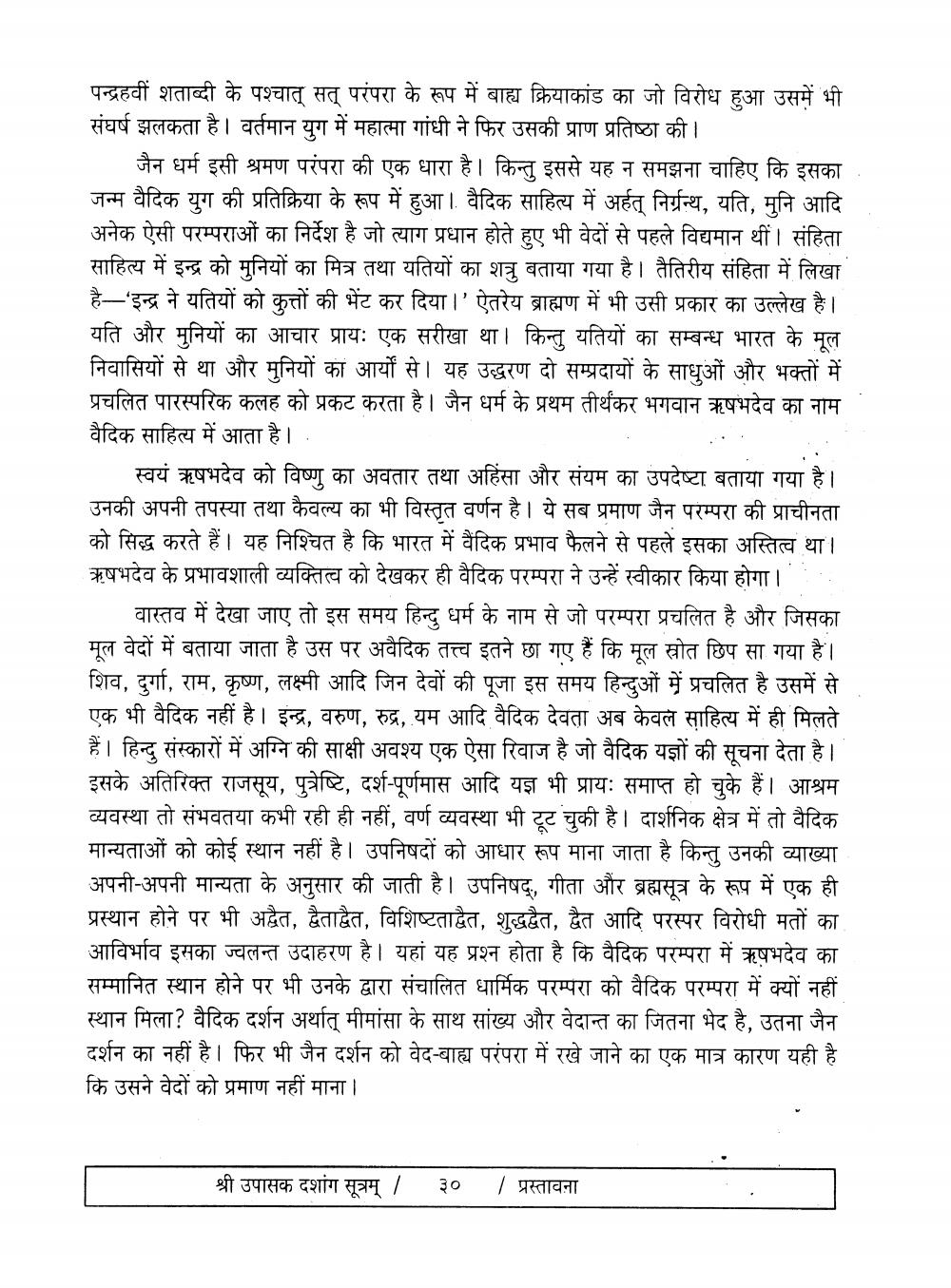________________ पन्द्रहवीं शताब्दी के पश्चात् सत् परंपरा के रूप में बाह्य क्रियाकांड का जो विरोध हुआ उसमें भी संघर्ष झलकता है। वर्तमान युग में महात्मा गांधी ने फिर उसकी प्राण प्रतिष्ठा की। जैन धर्म इसी श्रमण परंपरा की एक धारा है। किन्तु इससे यह न समझना चाहिए कि इसका जन्म वैदिक युग की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ। वैदिक साहित्य में अर्हत् निर्ग्रन्थ, यति, मुनि आदि अनेक ऐसी परम्पराओं का निर्देश है जो त्याग प्रधान होते हुए भी वेदों से पहले विद्यमान थीं। संहिता साहित्य में इन्द्र को मुनियों का मित्र तथा यतियों का शत्रु बताया गया है। तैतिरीय संहिता में लिखा है—'इन्द्र ने यतियों को कुत्तों की भेंट कर दिया।' ऐतरेय ब्राह्मण में भी उसी प्रकार का उल्लेख है। यति और मुनियों का आचार प्रायः एक सरीखा था। किन्तु यतियों का सम्बन्ध भारत के मूल निवासियों से था और मुनियों का आर्यों से। यह उद्धरण दो सम्प्रदायों के साधुओं और भक्तों में प्रचलित पारस्परिक कलह को प्रकट करता है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव का नाम वैदिक साहित्य में आता है। स्वयं ऋषभदेव को विष्णु का अवतार तथा अहिंसा और संयम का उपदेष्टा बताया गया है। उनकी अपनी तपस्या तथा कैवल्य का भी विस्तृत वर्णन है। ये सब प्रमाण जैन परम्परा की प्राचीनता को सिद्ध करते हैं। यह निश्चित है कि भारत में बैंदिक प्रभाव फैलने से पहले इसका अस्तित्व था। ऋषभदेव के प्रभावशाली व्यक्तित्व को देखकर ही वैदिक परम्परा ने उन्हें स्वीकार किया होगा। __वास्तव में देखा जाए तो इस समय हिन्दु धर्म के नाम से जो परम्परा प्रचलित है और जिसका मूल वेदों में बताया जाता है उस पर अवैदिक तत्त्व इतने छा गए हैं कि मूल स्रोत छिप सा गया है। शिव, दुर्गा, राम, कृष्ण, लक्ष्मी आदि जिन देवों की पूजा इस समय हिन्दुओं में प्रचलित है उसमें से एक भी वैदिक नहीं है। इन्द्र, वरुण, रुद्र, यम आदि वैदिक देवता अब केवल साहित्य में ही मिलते हैं। हिन्दु संस्कारों में अग्नि की साक्षी अवश्य एक ऐसा रिवाज है जो वैदिक यज्ञों की सूचना देता है। इसके अतिरिक्त राजसूय, पुत्रेष्टि, दर्श-पूर्णमास आदि यज्ञ भी प्रायः समाप्त हो चुके हैं। आश्रम व्यवस्था तो संभवतया कभी रही ही नहीं, वर्ण व्यवस्था भी टूट चुकी है। दार्शनिक क्षेत्र में तो वैदिक मान्यताओं को कोई स्थान नहीं है। उपनिषदों को आधार रूप माना जाता है किन्तु उनकी व्याख्या अपनी-अपनी मान्यता के अनुसार की जाती है। उपनिषद्, गीता और ब्रह्मसूत्र के रूप में एक ही प्रस्थान होने पर भी अद्वैत, द्वैताद्वैत, विशिष्टताद्वैत, शुद्धद्वैत, द्वैत आदि परस्पर विरोधी मतों का आविर्भाव इसका ज्वलन्त उदाहरण है। यहां यह प्रश्न होता है कि वैदिक परम्परा में ऋषभदेव का सम्मानित स्थान होने पर भी उनके द्वारा संचालित धार्मिक परम्परा को वैदिक परम्परा में क्यों नहीं स्थान मिला? वैदिक दर्शन अर्थात् मीमांसा के साथ सांख्य और वेदान्त का जितना भेद है, उतना जैन दर्शन का नहीं है। फिर भी जैन दर्शन को वेद-बाह्य परंपरा में रखे जाने का एक मात्र कारण यही है कि उसने वेदों को प्रमाण नहीं माना। __ श्री उपासक दशांग सूत्रम् / 30 / प्रस्तावना