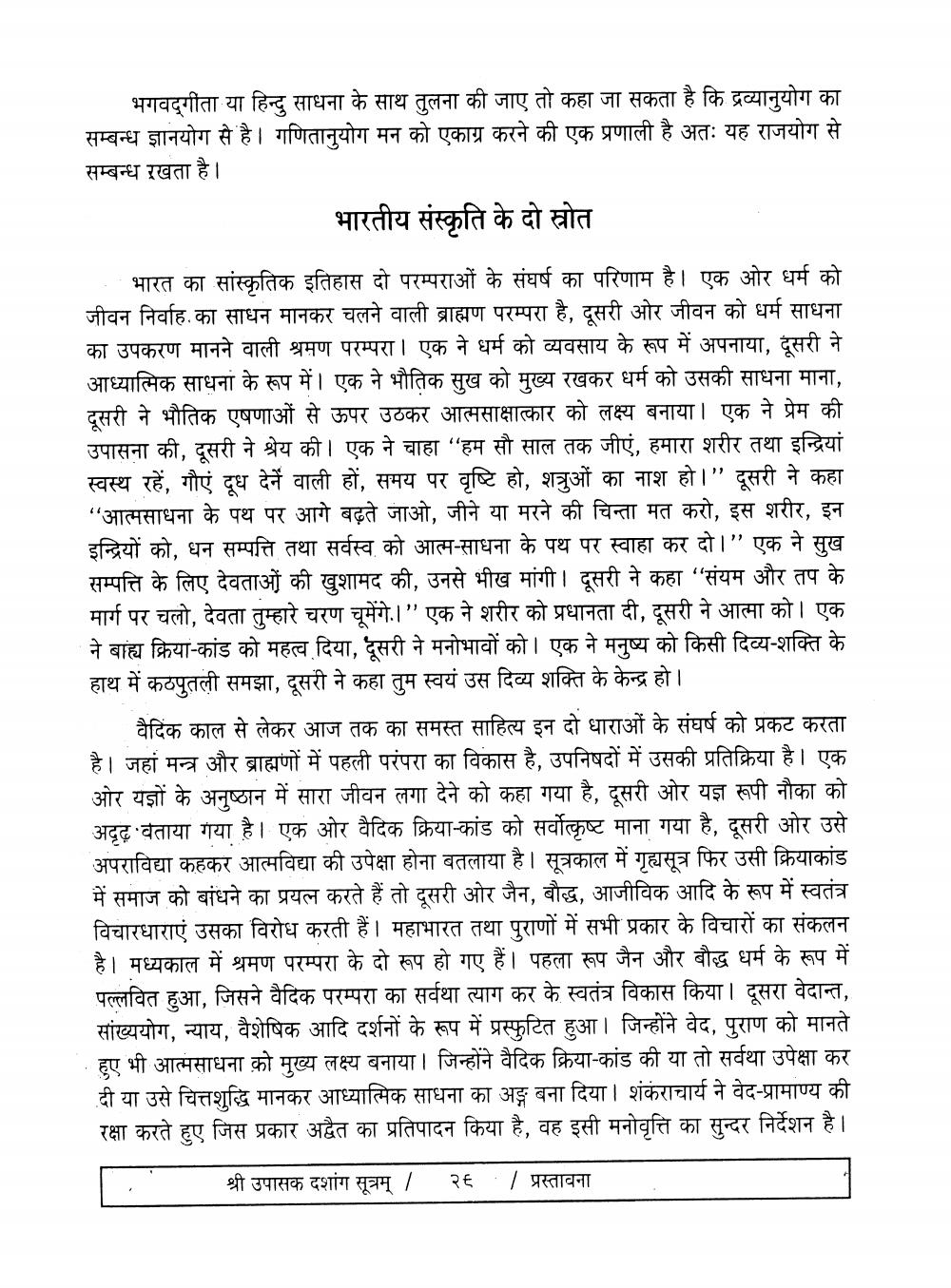________________ भगवद्गीता या हिन्दु साधना के साथ तुलना की जाए तो कहा जा सकता है कि द्रव्यानुयोग का सम्बन्ध ज्ञानयोग से है। गणितानुयोग मन को एकाग्र करने की एक प्रणाली है अतः यह राजयोग से सम्बन्ध रखता है। भारतीय संस्कृति के दो स्रोत स्वस भारत का सांस्कृतिक इतिहास दो परम्पराओं के संघर्ष का परिणाम है। एक ओर धर्म को जीवन निर्वाह का साधन मानकर चलने वाली ब्राह्मण परम्परा है, दूसरी ओर जीवन को धर्म साधना का उपकरण मानने वाली श्रमण परम्परा / एक ने धर्म को व्यवसाय के रूप में अपनाया, दूसरी ने आध्यात्मिक साधना के रूप में। एक ने भौतिक सुख को मुख्य रखकर धर्म को उसकी साधना माना, दूसरी ने भौतिक एषणाओं से ऊपर उठकर आत्मसाक्षात्कार को लक्ष्य बनाया। एक ने प्रेम की उपासना की, दूसरी ने श्रेय की। एक ने चाहा “हम सौ साल तक जीएं, हमारा शरीर तथा इन्द्रियां य रहें, गौएं दूध देने वाली हों, समय पर वृष्टि हो, शत्रुओं का नाश हो।" दूसरी ने कहा "आत्मसाधना के पथ पर आगे बढ़ते जाओ, जीने या मरने की चिन्ता मत करो, इस शरीर, इन इन्द्रियों को, धन सम्पत्ति तथा सर्वस्व को आत्म-साधना के पथ पर स्वाहा कर दो।" एक ने सुख सम्पत्ति के लिए देवताओं की खुशामद की, उनसे भीख मांगी। दूसरी ने कहा “संयम और तप के मार्ग पर चलो, देवता तुम्हारे चरण चूमेंगे.।" एक ने शरीर को प्रधानता दी, दूसरी ने आत्मा को। एक ने बाह्य क्रिया-कांड को महत्व दिया, 'दूसरी ने मनोभावों को। एक ने मनुष्य को किसी दिव्य-शक्ति के हाथ में कठपुतली समझा, दूसरी ने कहा तुम स्वयं उस दिव्य शक्ति के केन्द्र हो / __ वैदिक काल से लेकर आज तक का समस्त साहित्य इन दो धाराओं के संघर्ष को प्रकट करता है। जहां मन्त्र और ब्राह्मणों में पहली परंपरा का विकास है, उपनिषदों में उसकी प्रतिक्रिया है। एक ओर यज्ञों के अनुष्ठान में सारा जीवन लगा देने को कहा गया है, दूसरी ओर यज्ञ रूपी नौका को अदृढ़ बताया गया है। एक ओर वैदिक क्रिया-कांड को सर्वोत्कृष्ट माना गया है, दूसरी ओर उसे अपराविद्या कहकर आत्मविद्या की उपेक्षा होना बतलाया है। सूत्रकाल में गृह्यसूत्र फिर उसी क्रियाकांड में समाज को बांधने का प्रयत्न करते हैं तो दूसरी ओर जैन, बौद्ध, आजीविक आदि के रूप में स्वतंत्र विचारधाराएं उसका विरोध करती हैं। महाभारत तथा पुराणों में सभी प्रकार के विचारों का संकलन है। मध्यकाल में श्रमण परम्परा के दो रूप हो गए हैं। पहला रूप जैन और बौद्ध धर्म के रूप में पल्लवित हुआ, जिसने वैदिक परम्परा का सर्वथा त्याग कर के स्वतंत्र विकास किया। दूसरा वेदान्त, सांख्ययोग, न्याय वैशेषिक आदि दर्शनों के रूप में प्रस्फटित हआ। जिन्होंने वेद पराण को मानते हुए भी आत्मसाधना को मुख्य लक्ष्य बनाया। जिन्होंने वैदिक क्रिया-कांड की या तो सर्वथा उपेक्षा कर दी या उसे चित्तशुद्धि मानकर आध्यात्मिक साधना का अङ्ग बना दिया। शंकराचार्य ने वेद-प्रामाण्य की रक्षा करते हुए जिस प्रकार अद्वैत का प्रतिपादन किया है, वह इसी मनोवृत्ति का सुन्दर निर्देशन है। श्री उपासक दशांग सूत्रम् / 26 / प्रस्तावना