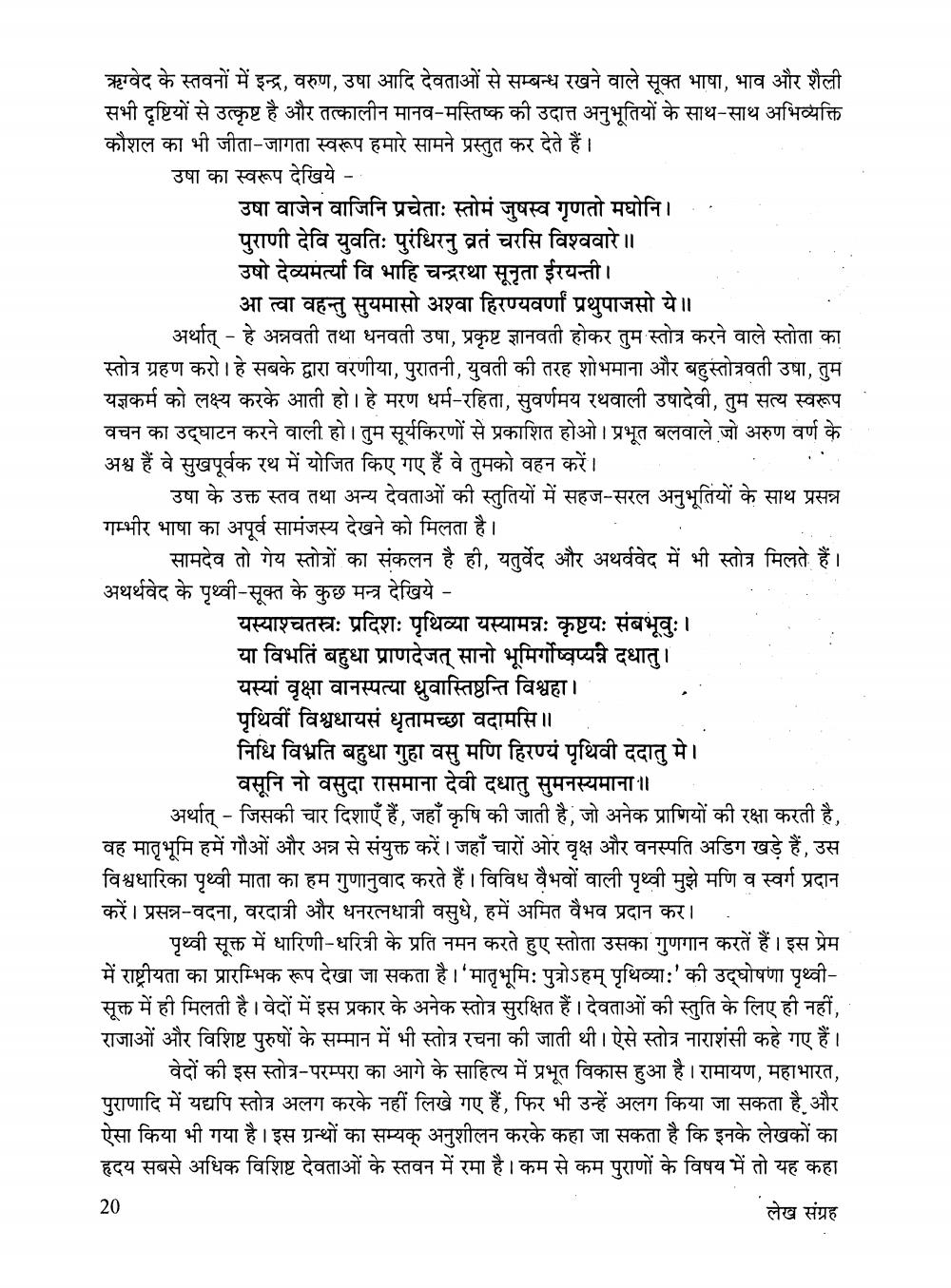________________ ऋग्वेद के स्तवनों में इन्द्र, वरुण, उषा आदि देवताओं से सम्बन्ध रखने वाले सूक्त भाषा, भाव और शैली सभी दृष्टियों से उत्कृष्ट है और तत्कालीन मानव-मस्तिष्क की उदात्त अनुभूतियों के साथ-साथ अभिव्यक्ति कौशल का भी जीता-जागता स्वरूप हमारे सामने प्रस्तुत कर देते हैं। उषा का स्वरूप देखिये - उषा वाजेन वाजिनि प्रचेताः स्तोमं जुषस्व गृणतो मघोनि। पुराणी देवि युवतिः पुरंधिरनु व्रतं चरसि विश्ववारे॥ उषो देव्यमा वि भाहि चन्द्ररथा सूनृता ईरयन्ती। आ त्वा वहन्तु सुयमासो अश्वा हिरण्यवर्णां प्रथुपाजसो ये॥ अर्थात् - हे अन्नवती तथा धनवती उषा, प्रकृष्ट ज्ञानवती होकर तुम स्तोत्र करने वाले स्तोता का स्तोत्र ग्रहण करो। हे सबके द्वारा वरणीया, पुरातनी, युवती की तरह शोभमाना और बहुस्तोत्रवती उषा, तुम यज्ञकर्म को लक्ष्य करके आती हो। हे मरण धर्म-रहिता, सुवर्णमय रथवाली उषादेवी, तुम सत्य स्वरूप वचन का उद्घाटन करने वाली हो। तुम सूर्यकिरणों से प्रकाशित होओ। प्रभूत बलवाले जो अरुण वर्ण के अश्व हैं वे सुखपूर्वक रथ में योजित किए गए हैं वे तुमको वहन करें। उषा के उक्त स्तव तथा अन्य देवताओं की स्तुतियों में सहज-सरल अनुभूतियों के साथ प्रसन्न गम्भीर भाषा का अपूर्व सामंजस्य देखने को मिलता है। सामदेव तो गेय स्तोत्रों का संकलन है ही, यतुर्वेद और अथर्ववेद में भी स्तोत्र मिलते हैं। अथर्थवेद के पृथ्वी-सूक्त के कुछ मन्त्र देखिये - यस्याश्चतस्त्रः प्रदिशः पृथिव्या यस्यामनः कृष्टयः संबभूवुः। या विभतिं बहुधा प्राणदेजत् सानो भूमिर्गोष्वप्यन्ने दधातु। यस्यां वृक्षा वानस्पत्या ध्रुवास्तिष्ठन्ति विश्वहा। पृथिवीं विश्वधायसं धृतामच्छा वदामसि॥ निधि विभ्रति बहुधा गुहा वसु मणि हिरण्यं पृथिवी ददातु मे। वसूनि नो वसुदा रासमाना देवी दधातु सुमनस्यमाना॥ अर्थात् - जिसकी चार दिशाएँ हैं, जहाँ कृषि की जाती है, जो अनेक प्राणियों की रक्षा करती है, वह मातृभूमि हमें गौओं और अन्न से संयुक्त करें। जहाँ चारों ओर वृक्ष और वनस्पति अडिग खड़े हैं, उस विश्वधारिका पृथ्वी माता का हम गुणानुवाद करते हैं। विविध वैभवों वाली पृथ्वी मुझे मणि व स्वर्ग प्रदान करें। प्रसन्न-वदना, वरदात्री और धनरत्नधात्री वसुधे, हमें अमित वैभव प्रदान कर। पृथ्वी सूक्त में धारिणी-धरित्री के प्रति नमन करते हुए स्तोता उसका गुणगान करतें हैं। इस प्रेम में राष्ट्रीयता का प्रारम्भिक रूप देखा जा सकता है। 'मातृभूमिः पुत्रोऽहम् पृथिव्याः' की उद्घोषणा पृथ्वीसूक्त में ही मिलती है। वेदों में इस प्रकार के अनेक स्तोत्र सुरक्षित हैं / देवताओं की स्तुति के लिए ही नहीं, राजाओं और विशिष्ट पुरुषों के सम्मान में भी स्तोत्र रचना की जाती थी। ऐसे स्तोत्र नाराशंसी कहे गए हैं। वेदों की इस स्तोत्र-परम्परा का आगे के साहित्य में प्रभूत विकास हुआ है। रामायण, महाभारत, पराणादि में यद्यपि स्तोत्र अलग करके नहीं लिखे गए हैं. फिर भी उन्हें अलग किया जा सकता है और ऐसा किया भी गया है। इस ग्रन्थों का सम्यक् अनुशीलन करके कहा जा सकता है कि इनके लेखकों का हृदय सबसे अधिक विशिष्ट देवताओं के स्तवन में रमा है। कम से कम पुराणों के विषय में तो यह कहा 20 लेख संग्रह