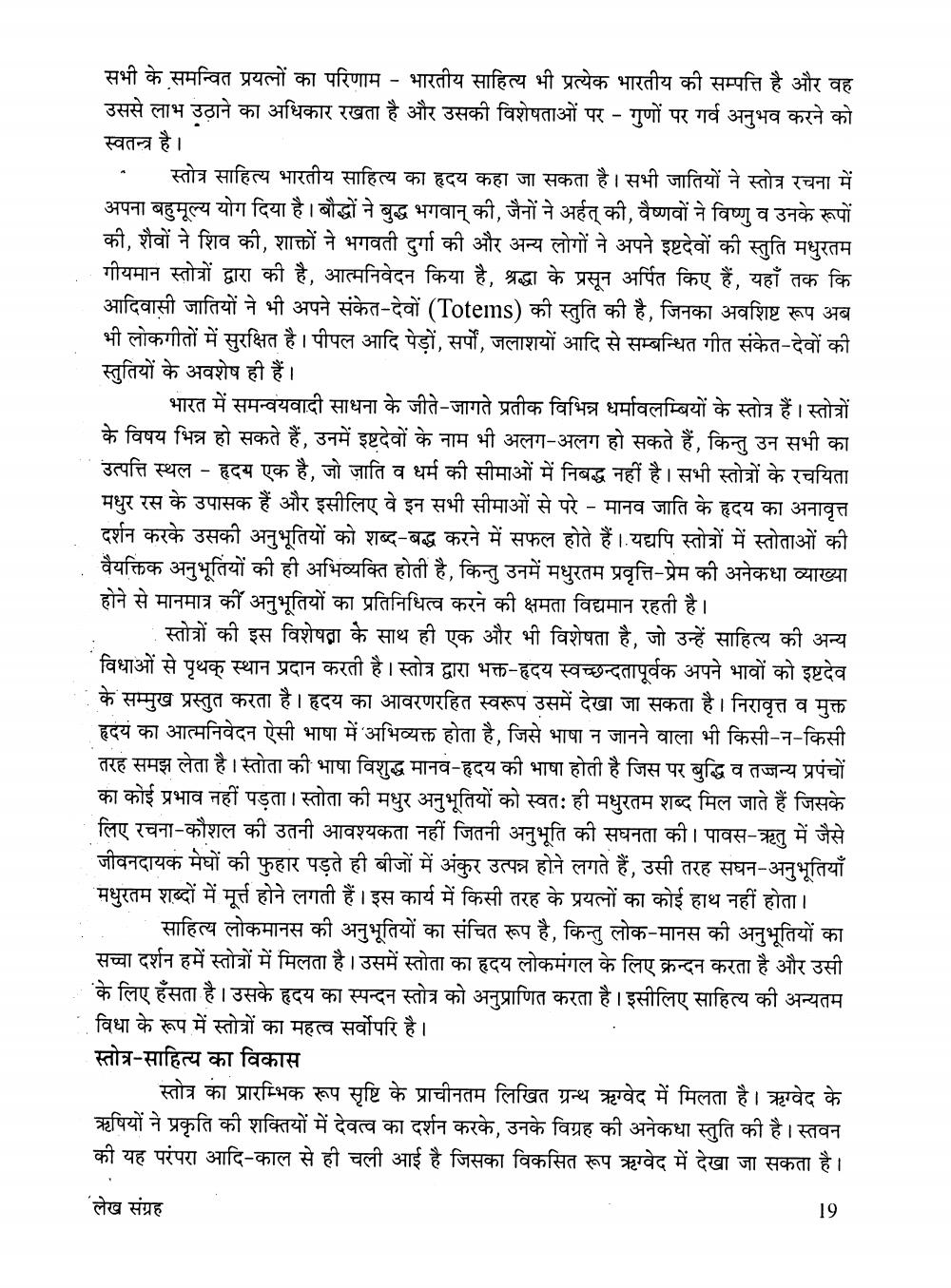________________ सभी के समन्वित प्रयत्नों का परिणाम - भारतीय साहित्य भी प्रत्येक भारतीय की सम्पत्ति है और वह उससे लाभ उठाने का अधिकार रखता है और उसकी विशेषताओं पर - गुणों पर गर्व अनुभव करने को स्वतन्त्र है। - स्तोत्र साहित्य भारतीय साहित्य का हृदय कहा जा सकता है। सभी जातियों ने स्तोत्र रचना में अपना बहुमूल्य योग दिया है। बौद्धों ने बुद्ध भगवान् की, जैनों ने अर्हत् की, वैष्णवों ने विष्णु व उनके रूपों की, शैवों ने शिव की, शाक्तों ने भगवती दुर्गा की और अन्य लोगों ने अपने इष्टदेवों की स्तुति मधुरतम गीयमान स्तोत्रों द्वारा की है, आत्मनिवेदन किया है, श्रद्धा के प्रसून अर्पित किए हैं, यहाँ तक कि आदिवासी जातियों ने भी अपने संकेत-देवों (Totems) की स्तुति की है, जिनका अवशिष्ट रूप अब भी लोकगीतों में सुरक्षित है। पीपल आदि पेड़ों, सर्पो, जलाशयों आदि से सम्बन्धित गीत संकेत-देवों की स्तुतियों के अवशेष ही हैं। __ भारत में समन्वयवादी साधना के जीते-जागते प्रतीक विभिन्न धर्मावलम्बियों के स्तोत्र हैं। स्तोत्रों के विषय भिन्न हो सकते हैं, उनमें इष्टदेवों के नाम भी अलग-अलग हो सकते हैं, किन्तु उन सभी का उत्पत्ति स्थल - हृदय एक है, जो जाति व धर्म की सीमाओं में निबद्ध नहीं है। सभी स्तोत्रों के रचयिता मधुर रस के उपासक हैं और इसीलिए वे इन सभी सीमाओं से परे - मानव जाति के हृदय का अनावृत्त दर्शन करके उसकी अनुभूतियों को शब्द-बद्ध करने में सफल होते हैं। यद्यपि स्तोत्रों में स्तोताओं की वैयक्तिक अनुभूतियों की ही अभिव्यक्ति होती है, किन्तु उनमें मधुरतम प्रवृत्ति-प्रेम की अनेकधा व्याख्या होने से मानमात्र की अनुभूतियों का प्रतिनिधित्व करने की क्षमता विद्यमान रहती है। स्तोत्रों की इस विशेषता के साथ ही एक और भी विशेषता है, जो उन्हें साहित्य की अन्य विधाओं से पृथक् स्थान प्रदान करती है। स्तोत्र द्वारा भक्त-हृदय स्वच्छन्दतापूर्वक अपने भावों को इष्टदेव के सम्मुख प्रस्तुत करता है। हृदय का आवरणरहित स्वरूप उसमें देखा जा सकता है। निरावृत्त व मुक्त हृदयं का आत्मनिवेदन ऐसी भाषा में अभिव्यक्त होता है, जिसे भाषा न जानने वाला भी किसी-न-किसी तरह समझ लेता है। स्तोता की भाषा विशुद्ध मानव-हृदय की भाषा होती है जिस पर बुद्धि व तज्जन्य प्रपंचों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। स्तोता की मधुर अनुभूतियों को स्वतः ही मधुरतम शब्द मिल जाते हैं जिसके लिए रचना-कौशल की उतनी आवश्यकता नहीं जितनी अनुभूति की सघनता की। पावस-ऋतु में जैसे जीवनदायक मेघों की फुहार पड़ते ही बीजों में अंकुर उत्पन्न होने लगते हैं, उसी तरह सघन-अनुभूतियाँ मधुरतम शब्दों में मूर्त होने लगती हैं। इस कार्य में किसी तरह के प्रयत्नों का कोई हाथ नहीं होता। ___साहित्य लोकमानस की अनुभूतियों का संचित रूप है, किन्तु लोक-मानस की अनुभूतियों का सच्चा दर्शन हमें स्तोत्रों में मिलता है। उसमें स्तोता का हृदय लोकमंगल के लिए क्रन्दन करता है और उसी के लिए हँसता है। उसके हृदय का स्पन्दन स्तोत्र को अनुप्राणित करता है। इसीलिए साहित्य की अन्यतम विधा के रूप में स्तोत्रों का महत्व सर्वोपरि है। स्तोत्र-साहित्य का विकास स्तोत्र का प्रारम्भिक रूप सृष्टि के प्राचीनतम लिखित ग्रन्थ ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद के ऋषियों ने प्रकृति की शक्तियों में देवत्व का दर्शन करके, उनके विग्रह की अनेकधा स्तुति की है। स्तवन की यह परंपरा आदि-काल से ही चली आई है जिसका विकसित रूप ऋग्वेद में देखा जा सकता है। लेख संग्रह 19