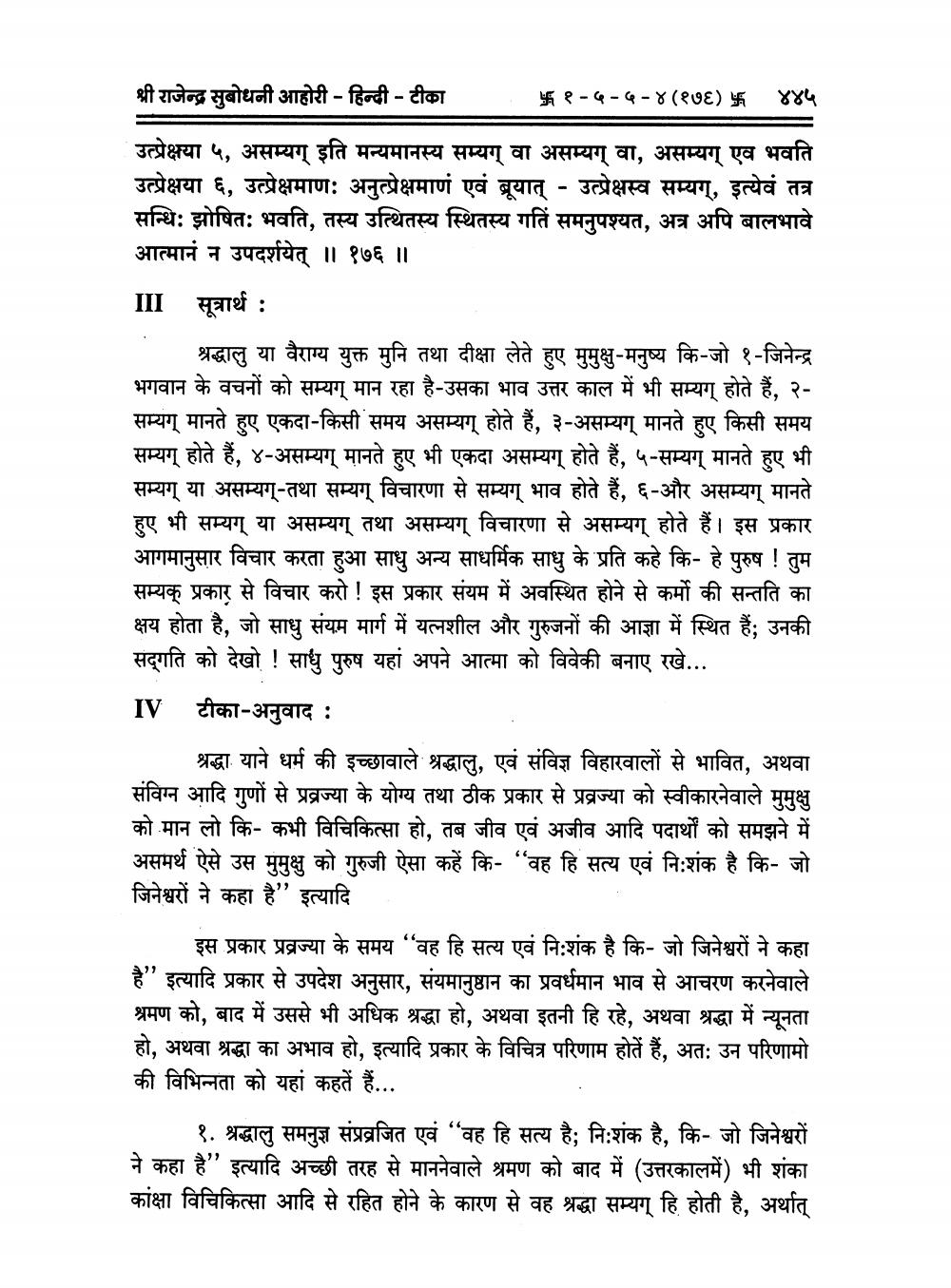________________ श्री राजेन्द्र सुबोधनी आहोरी - हिन्दी - टीका 1-5-5-4 (176) 445 उत्प्रेक्षया 5, असम्यग् इति मन्यमानस्य सम्यग् वा असम्यग् वा, असम्यग् एव भवति उत्प्रेक्षया 6, उत्प्रेक्षमाणः अनुत्प्रेक्षमाणं एवं ब्रूयात् - उत्प्रेक्षस्व सम्यग्, इत्येवं तत्र सन्धिः झोषित: भवति, तस्य उत्थितस्य स्थितस्य गतिं समनुपश्यत, अत्र अपि बालभावे आत्मानं न उपदर्शयेत् // 176 // III सूत्रार्थ : श्रद्धालु या वैराग्य युक्त मुनि तथा दीक्षा लेते हुए मुमुक्षु-मनुष्य कि-जो १-जिनेन्द्र भगवान के वचनों को सम्यग् मान रहा है-उसका भाव उत्तर काल में भी सम्यग् होते हैं, २सम्यग् मानते हुए एकदा-किसी समय असम्यग् होते हैं, ३-असम्यग् मानते हुए किसी समय सम्यग् होते हैं, ४-असम्यग् मानते हुए भी एकदा असम्यग् होते हैं, ५-सम्यग् मानते हुए भी सम्यग् या असम्यग्-तथा सम्यग् विचारणा से सम्यग् भाव होते हैं, ६-और असम्यग् मानते हुए भी सम्यग् या असम्यग् तथा असम्यग् विचारणा से असम्यग् होते हैं। इस प्रकार आगमानुसार विचार करता हुआ साधु अन्य साधर्मिक साधु के प्रति कहे कि- हे पुरुष ! तुम सम्यक् प्रकार से विचार करो ! इस प्रकार संयम में अवस्थित होने से कर्मो की सन्तति का क्षय होता है, जो साधु संयम मार्ग में यत्नशील और गुरुजनों की आज्ञा में स्थित हैं; उनकी सद्गति को देखो ! साधु पुरुष यहां अपने आत्मा को विवेकी बनाए रखे... IV टीका-अनुवाद : श्रद्धा याने धर्म की इच्छावाले श्रद्धालु, एवं संविज्ञ विहारवालों से भावित, अथवा संविग्न आदि गुणों से प्रव्रज्या के योग्य तथा ठीक प्रकार से प्रव्रज्या को स्वीकारनेवाले मुमुक्षु को मान लो कि- कभी विचिकित्सा हो, तब जीव एवं अजीव आदि पदार्थों को समझने में असमर्थ ऐसे उस मुमुक्षु को गुरुजी ऐसा कहें कि- “वह हि सत्य एवं नि:शंक है कि- जो जिनेश्वरों ने कहा है" इत्यादि इस प्रकार प्रव्रज्या के समय “वह हि सत्य एवं नि:शंक है कि- जो जिनेश्वरों ने कहा है" इत्यादि प्रकार से उपदेश अनुसार, संयमानुष्ठान का प्रवर्धमान भाव से आचरण करनेवाले श्रमण को, बाद में उससे भी अधिक श्रद्धा हो, अथवा इतनी हि रहे, अथवा श्रद्धा में न्यूनता हो, अथवा श्रद्धा का अभाव हो, इत्यादि प्रकार के विचित्र परिणाम होते हैं, अत: उन परिणामो की विभिन्नता को यहां कहतें हैं... 1. श्रद्धालु समनुज्ञ संप्रव्रजित एवं “वह हि सत्य है; निःशंक है, कि- जो जिनेश्वरों ने कहा है" इत्यादि अच्छी तरह से माननेवाले श्रमण को बाद में (उत्तरकालमें) भी शंका कांक्षा विचिकित्सा आदि से रहित होने के कारण से वह श्रद्धा सम्यग् हि होती है, अर्थात्