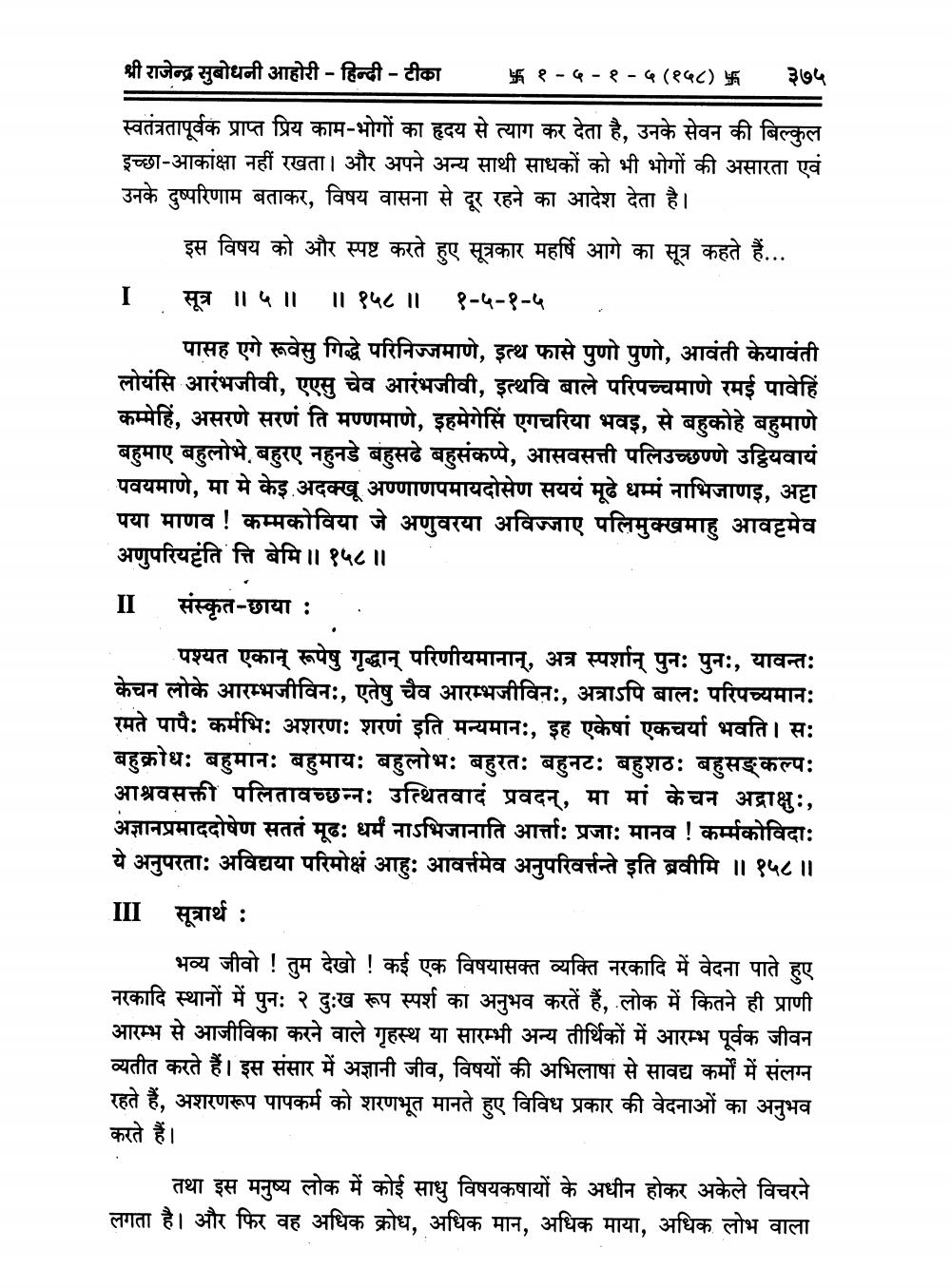________________ श्री राजेन्द्र सुबोधनी आहोरी - हिन्दी - टीका 1 - 5 - 1 - 5 (158) : 375 स्वतंत्रतापूर्वक प्राप्त प्रिय काम-भोगों का हृदय से त्याग कर देता है, उनके सेवन की बिल्कुल इच्छा-आकांक्षा नहीं रखता। और अपने अन्य साथी साधकों को भी भोगों की असारता एवं उनके दुष्परिणाम बताकर, विषय वासना से दूर रहने का आदेश देता है। इस विषय को और स्पष्ट करते हुए सूत्रकार महर्षि आगे का सूत्र कहते हैं... I सूत्र // 5 // // 158 // 1-5-1-5 पासह एगे रूवेसु गिद्धे परिनिज्जमाणे, इत्थ फासे पुणो पुणो, आवंती केयावंती लोयंसि आरंभजीवी, एएसु चेव आरंभजीवी, इत्थवि बाले परिपच्चमाणे रमई पावेहिं कम्मेहिं, असरणे सरणं ति मण्णमाणे, इहमेगेसिं एगचरिया भवइ, से बहुकोहे बहुमाणे बहुमाए बहुलोभे. बहुरए नहुनडे बहुसढे बहुसंकप्पे, आसवसत्ती पलिउच्छण्णे उट्ठियवायं पवयमाणे, मा मे केइ अदक्खू अण्णाणपमायदोसेण सययं मूढे धम्मं नाभिजाणइ, अट्टा पया माणव ! कम्मकोविया जे अणुवरया अविज्जाए पलिमुक्खमाहु आवट्टमेव अणुपरियटुंति त्ति बेमि // 158 // II संस्कृत-छाया : पश्यत एकान् रूपेषु गृद्धान् परिणीयमानान्, अत्र स्पर्शान् पुनः पुनः, यावन्तः केचन लोके आरम्भजीविनः, एतेषु चैव आरम्भजीविनः, अत्राऽपि बालः परिपच्यमान: रमते पापैः कर्मभिः अशरणः शरणं इति मन्यमानः, इह एकेषां एकचर्या भवति। सः बहुक्रोधः बहुमानः बहुमायः बहुलोभः बहुरतः बहुनटः बहुशठः बहुसङ्कल्प: आश्रवसक्ती पलितावच्छन्न: उत्थितवादं प्रवदन्, मा मां के चन अद्राक्षुः, अज्ञानप्रमाददोषेण सततं मूढः धर्मं नाऽभिजानाति आर्ताः प्रजाः मानव ! कर्मकोविदाः ये अनुपरताः अविद्यया परिमोक्षं आहुः आवर्तमेव अनुपरिवर्तन्ते इति ब्रवीमि // 158 // III सूत्रार्थ : भव्य जीवो ! तुम देखो ! कई एक विषयासक्त व्यक्ति नरकादि में वेदना पाते हुए नरकादि स्थानों में पुनः 2 दुःख रूप स्पर्श का अनुभव करतें हैं, लोक में कितने ही प्राणी आरम्भ से आजीविका करने वाले गृहस्थ या सारम्भी अन्य तीर्थिकों में आरम्भ पूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं। इस संसार में अज्ञानी जीव, विषयों की अभिलाषा से सावध कर्मों में संलग्न रहते हैं, अशरणरूप पापकर्म को शरणभूत मानते हुए विविध प्रकार की वेदनाओं का अनुभव करते हैं। तथा इस मनुष्य लोक में कोई साधु विषयकषायों के अधीन होकर अकेले विचरने लगता है। और फिर वह अधिक क्रोध, अधिक मान, अधिक माया, अधिक लोभ वाला