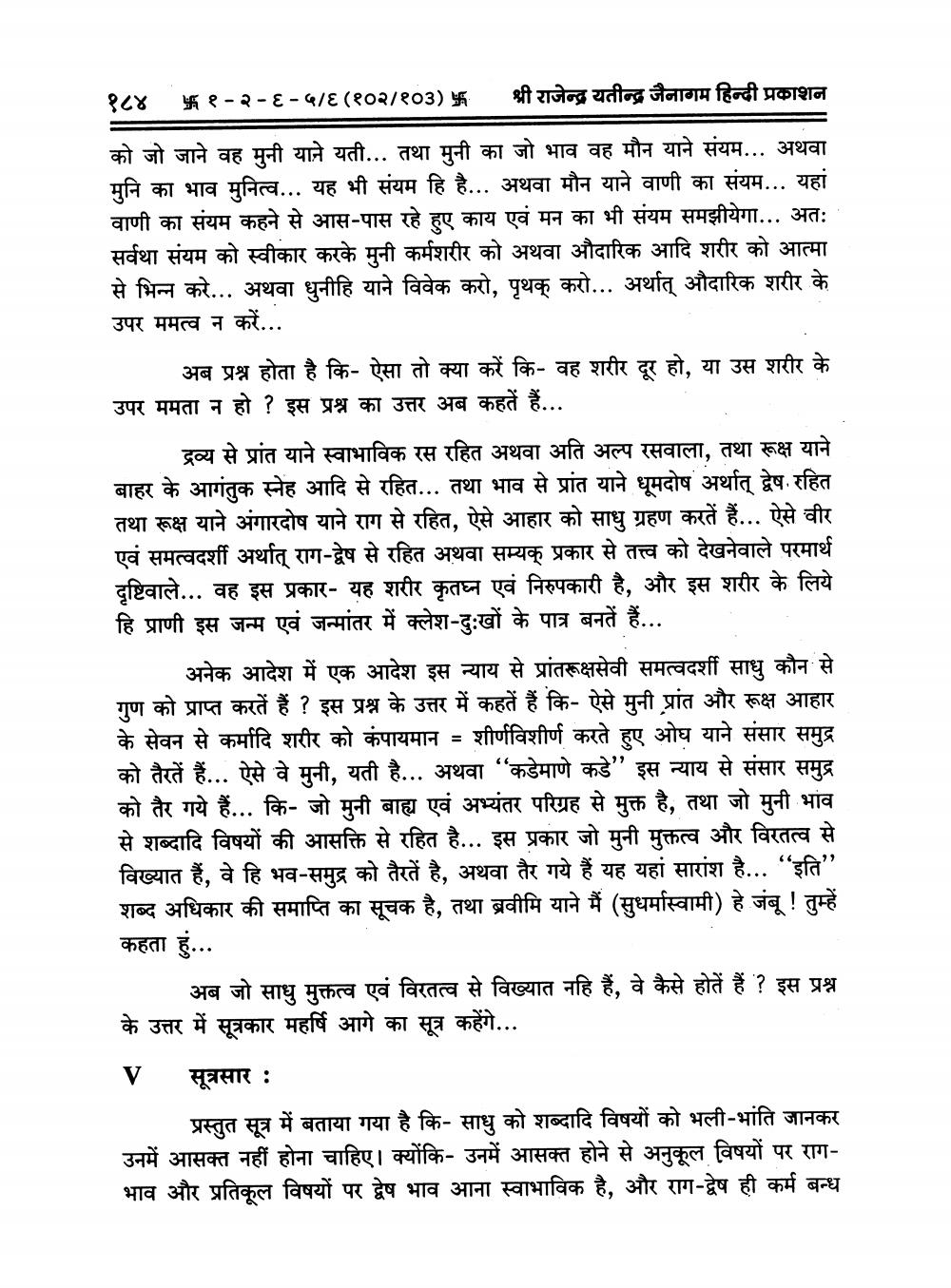________________ 1841 -2-6-5/6 (102/103) श्री राजेन्द्र यतीन्द्र जैनागम हिन्दी प्रकाशन को जो जाने वह मुनी याने यती... तथा मुनी का जो भाव वह मौन याने संयम... अथवा मुनि का भाव मुनित्व... यह भी संयम हि है... अथवा मौन याने वाणी का संयम... यहां वाणी का संयम कहने से आस-पास रहे हुए काय एवं मन का भी संयम समझीयेगा... अतः सर्वथा संयम को स्वीकार करके मुनी कर्मशरीर को अथवा औदारिक आदि शरीर को आत्मा से भिन्न करे... अथवा धुनीहि याने विवेक करो, पृथक् करो... अर्थात् औदारिक शरीर के उपर ममत्व न करें... अब प्रश्न होता है कि- ऐसा तो क्या करें कि- वह शरीर दूर हो, या उस शरीर के उपर ममता न हो ? इस प्रश्न का उत्तर अब कहतें हैं... द्रव्य से प्रांत याने स्वाभाविक रस रहित अथवा अति अल्प रसवाला, तथा रूक्ष याने बाहर के आगंतुक स्नेह आदि से रहित... तथा भाव से प्रांत याने धूमदोष अर्थात् द्वेष रहित तथा रूक्ष याने अंगारदोष याने राग से रहित, ऐसे आहार को साधु ग्रहण करतें हैं... ऐसे वीर एवं समत्वदर्शी अर्थात् राग-द्वेष से रहित अथवा सम्यक् प्रकार से तत्त्व को देखनेवाले परमार्थ दृष्टिवाले... वह इस प्रकार- यह शरीर कृतघ्न एवं निरुपकारी है, और इस शरीर के लिये हि प्राणी इस जन्म एवं जन्मांतर में क्लेश-दुःखों के पात्र बनतें हैं... अनेक आदेश में एक आदेश इस न्याय से प्रांतरूक्षसेवी समत्वदर्शी साधु कौन से गुण को प्राप्त करतें हैं ? इस प्रश्न के उत्तर में कहते हैं कि- ऐसे मुनी प्रांत और रूक्ष आहार के सेवन से कर्मादि शरीर को कंपायमान = शीर्णविशीर्ण करते हुए ओघ याने संसार समुद्र को तैरतें हैं... ऐसे वे मुनी, यती है... अथवा “कडेमाणे कडे" इस न्याय से संसार समुद्र को तैर गये हैं... कि- जो मुनी बाह्य एवं अभ्यंतर परिग्रह से मुक्त है, तथा जो मुनी भाव से शब्दादि विषयों की आसक्ति से रहित है... इस प्रकार जो मुनी मुक्तत्व और विरतत्व से विख्यात हैं, वे हि भव-समुद्र को तैरतें है, अथवा तैर गये हैं यह यहां सारांश है... “इति" शब्द अधिकार की समाप्ति का सूचक है, तथा ब्रवीमि याने मैं (सुधर्मास्वामी) हे जंबू ! तुम्हें कहता हुं... ___ अब जो साधु मुक्तत्व एवं विरतत्व से विख्यात नहि हैं, वे कैसे होते हैं ? इस प्रश्न के उत्तर में सूत्रकार महर्षि आगे का सूत्र कहेंगे... v सूत्रसार : प्रस्तुत सूत्र में बताया गया है कि- साधु को शब्दादि विषयों को भली-भांति जानकर उनमें आसक्त नहीं होना चाहिए। क्योंकि- उनमें आसक्त होने से अनुकूल विषयों पर रागभाव और प्रतिकूल विषयों पर द्वेष भाव आना स्वाभाविक है, और राग-द्वेष ही कर्म बन्ध