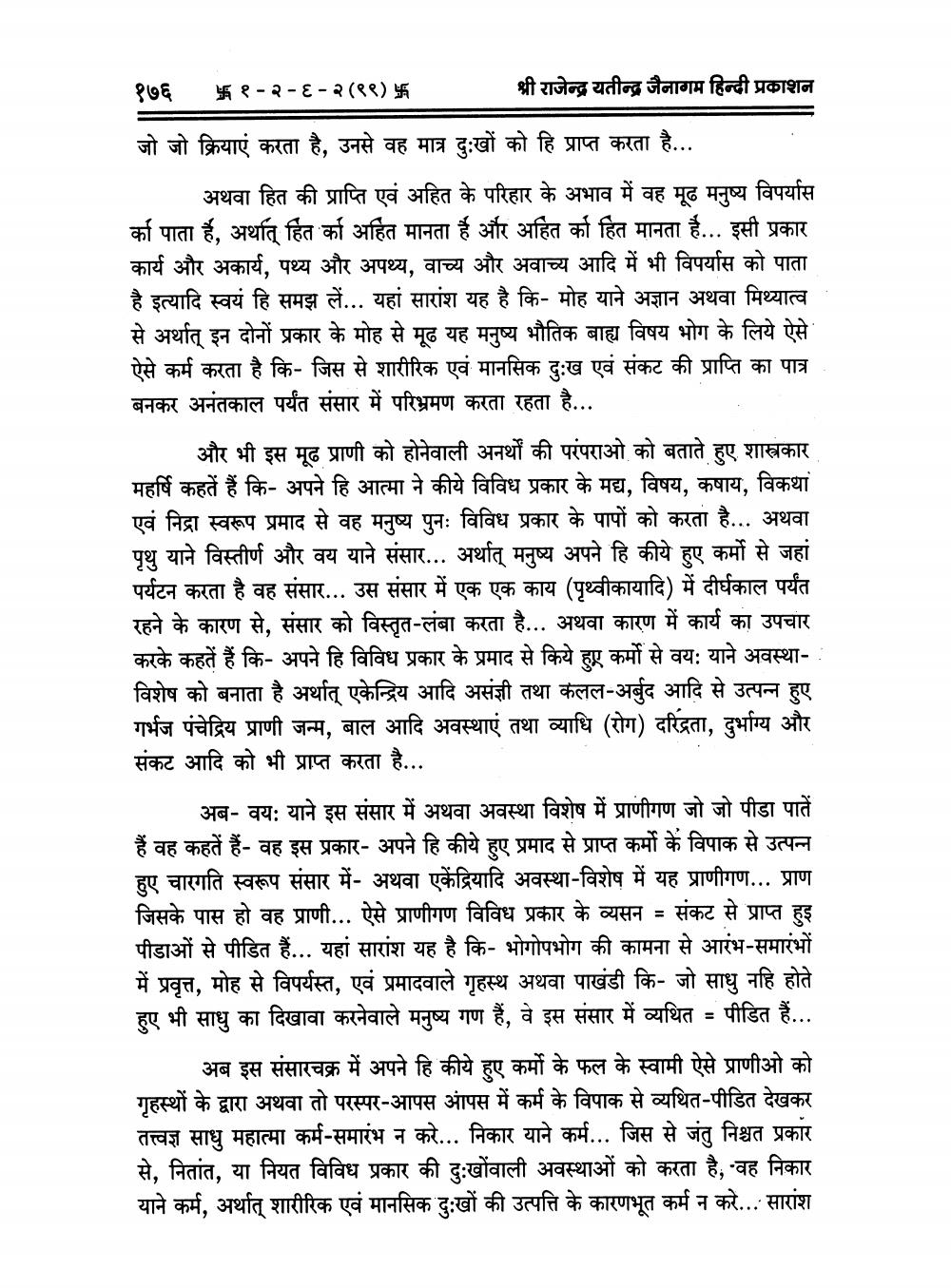________________ 176 1-2-6 - 2 (99) श्री राजेन्द्र यतीन्द्र जैनागम हिन्दी प्रकाशन जो जो क्रियाएं करता है, उनसे वह मात्र दुःखों को हि प्राप्त करता है... अथवा हित की प्राप्ति एवं अहित के परिहार के अभाव में वह मूढ मनुष्य विपर्यास कर्का पाता है, अर्थात् हित को अहित मानता है और अहित को हित मानता है... इसी प्रकार कार्य और अकार्य, पथ्य और अपथ्य, वाच्य और अवाच्य आदि में भी विपर्यास को पाता है इत्यादि स्वयं हि समझ लें... यहां सारांश यह है कि- मोह याने अज्ञान अथवा मिथ्यात्व से अर्थात् इन दोनों प्रकार के मोह से मूढ यह मनुष्य भौतिक बाह्य विषय भोग के लिये ऐसे ऐसे कर्म करता है कि- जिस से शारीरिक एवं मानसिक दुःख एवं संकट की प्राप्ति का पात्र बनकर अनंतकाल पर्यंत संसार में परिभ्रमण करता रहता है... और भी इस मूढ प्राणी को होनेवाली अनर्थों की परंपराओ को बताते हुए शास्त्रकार महर्षि कहते हैं कि- अपने हि आत्मा ने कीये विविध प्रकार के मद्य, विषय, कषाय, विकथा एवं निद्रा स्वरूप प्रमाद से वह मनुष्य पुनः विविध प्रकार के पापों को करता है... अथवा पृथु याने विस्तीर्ण और वय याने संसार... अर्थात् मनुष्य अपने हि कीये हुए कर्मो से जहां पर्यटन करता है वह संसार... उस संसार में एक एक काय (पृथ्वीकायादि) में दीर्घकाल पर्यंत रहने के कारण से, संसार को विस्तृत-लंबा करता है... अथवा कारण में कार्य का उपचार करके कहते हैं कि- अपने हि विविध प्रकार के प्रमाद से किये हुए कर्मो से वयः याने अवस्थाविशेष को बनाता है अर्थात् एकेन्द्रिय आदि असंज्ञी तथा कलल-अर्बुद आदि से उत्पन्न हुए गर्भज पंचेद्रिय प्राणी जन्म, बाल आदि अवस्थाएं तथा व्याधि (रोग) दरिद्रता, दुर्भाग्य और संकट आदि को भी प्राप्त करता है... अब- वयः याने इस संसार में अथवा अवस्था विशेष में प्राणीगण जो जो पीडा पातें हैं वह कहते हैं- वह इस प्रकार- अपने हि कीये हुए प्रमाद से प्राप्त कर्मो के विपाक से उत्पन्न हुए चारगति स्वरूप संसार में- अथवा एकेंद्रियादि अवस्था-विशेष में यह प्राणीगण... प्राण जिसके पास हो वह प्राणी... ऐसे प्राणीगण विविध प्रकार के व्यसन = संकट से प्राप्त हुइ पीडाओं से पीडित हैं... यहां सारांश यह है कि- भोगोपभोग की कामना से आरंभ-समारंभों में प्रवृत्त, मोह से विपर्यस्त, एवं प्रमादवाले गृहस्थ अथवा पाखंडी कि- जो साधु नहि होते हुए भी साधु का दिखावा करनेवाले मनुष्य गण हैं, वे इस संसार में व्यथित = पीडित हैं... अब इस संसारचक्र में अपने हि कीये हुए कर्मो के फल के स्वामी ऐसे प्राणीओ को गृहस्थों के द्वारा अथवा तो परस्पर-आपस आपस में कर्म के विपाक से व्यथित-पीडित देखकर तत्त्वज्ञ साधु महात्मा कर्म-समारंभ न करे... निकार याने कर्म... जिस से जंतु निश्चत प्रकार से, नितांत, या नियत विविध प्रकार की दु:खोंवाली अवस्थाओं को करता है, वह निकार याने कर्म, अर्थात् शारीरिक एवं मानसिक दु:खों की उत्पत्ति के कारणभूत कर्म न करे... सारांश