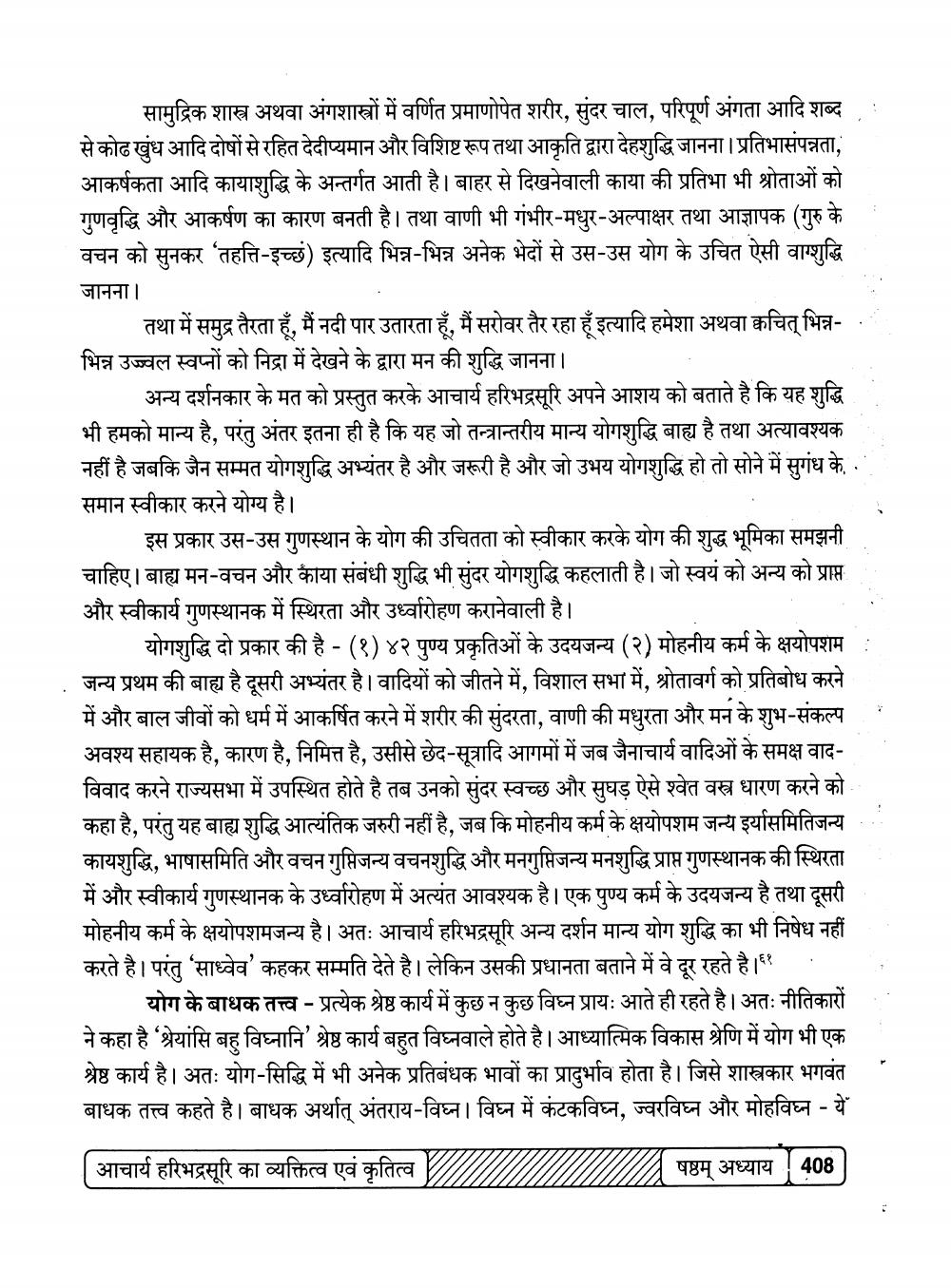________________ सामुद्रिक शास्त्र अथवा अंगशास्त्रों में वर्णित प्रमाणोपेत शरीर, सुंदर चाल, परिपूर्ण अंगता आदि शब्द : से कोढ खुंध आदि दोषों से रहित देदीप्यमान और विशिष्ट रूप तथा आकृति द्वारा देहशुद्धि जानना। प्रतिभासंपन्नता, आकर्षकता आदि कायाशुद्धि के अन्तर्गत आती है। बाहर से दिखनेवाली काया की प्रतिभा भी श्रोताओं को गुणवृद्धि और आकर्षण का कारण बनती है। तथा वाणी भी गंभीर-मधुर-अल्पाक्षर तथा आज्ञापक (गुरु के वचन को सुनकर तहत्ति-इच्छं) इत्यादि भिन्न-भिन्न अनेक भेदों से उस-उस योग के उचित ऐसी वाग्शुद्धि जानना। तथा में समुद्र तैरता हूँ, मैं नदी पार उतारता हूँ, मैं सरोवर तैर रहा हूँ इत्यादि हमेशा अथवा क्वचित् भिन्न- . भिन्न उज्ज्वल स्वप्नों को निद्रा में देखने के द्वारा मन की शुद्धि जानना। अन्य दर्शनकार के मत को प्रस्तुत करके आचार्य हरिभद्रसूरि अपने आशय को बताते है कि यह शुद्धि भी हमको मान्य है, परंतु अंतर इतना ही है कि यह जो तन्त्रान्तरीय मान्य योगशुद्धि बाह्य है तथा अत्यावश्यक नहीं है जबकि जैन सम्मत योगशुद्धि अभ्यंतर है और जरूरी है और जो उभय योगशुद्धि हो तो सोने में सुगंध के. . समान स्वीकार करने योग्य है। इस प्रकार उस-उस गुणस्थान के योग की उचितता को स्वीकार करके योग की शुद्ध भूमिका समझनी चाहिए। बाह्य मन-वचन और काया संबंधी शुद्धि भी सुंदर योगशुद्धि कहलाती है। जो स्वयं को अन्य को प्राप्त और स्वीकार्य गुणस्थानक में स्थिरता और उर्ध्वारोहण करानेवाली है। योगशुद्धि दो प्रकार की है - (1) 42 पुण्य प्रकृतिओं के उदयजन्य (2) मोहनीय कर्म के क्षयोपशम : जन्य प्रथम की बाह्य है दूसरी अभ्यंतर है। वादियों को जीतने में, विशाल सभा में, श्रोतावर्ग को प्रतिबोध करने में और बाल जीवों को धर्म में आकर्षित करने में शरीर की सुंदरता, वाणी की मधुरता और मन के शुभ-संकल्प अवश्य सहायक है, कारण है, निमित्त है, उसीसे छेद-सूत्रादि आगमों में जब जैनाचार्य वादिओं के समक्ष वादविवाद करने राज्यसभा में उपस्थित होते है तब उनको सुंदर स्वच्छ और सुघड़ ऐसे श्वेत वस्त्र धारण करने को कहा है, परंतु यह बाह्य शुद्धि आत्यंतिक जरुरी नहीं है, जब कि मोहनीय कर्म के क्षयोपशम जन्य इर्यासमितिजन्य कायशुद्धि, भाषासमिति और वचन गुप्तिजन्य वचनशुद्धि और मनगुप्तिजन्य मनशुद्धि प्राप्त गुणस्थानक की स्थिरता में और स्वीकार्य गुणस्थानक के उर्ध्वारोहण में अत्यंत आवश्यक है। एक पुण्य कर्म के उदयजन्य है तथा दूसरी मोहनीय कर्म के क्षयोपशमजन्य है। अतः आचार्य हरिभद्रसूरि अन्य दर्शन मान्य योग शुद्धि का भी निषेध नहीं करते है। परंतु 'साध्वेव' कहकर सम्मति देते है। लेकिन उसकी प्रधानता बताने में वे दूर रहते है।६१ . योग के बाधक तत्त्व - प्रत्येक श्रेष्ठ कार्य में कुछ न कुछ विघ्न प्रायः आते ही रहते है। अतः नीतिकारों ने कहा है 'श्रेयांसि बहु विघ्नानि' श्रेष्ठ कार्य बहुत विघ्नवाले होते है। आध्यात्मिक विकास श्रेणि में योग भी एक श्रेष्ठ कार्य है। अतः योग-सिद्धि में भी अनेक प्रतिबंधक भावों का प्रादुर्भाव होता है। जिसे शास्त्रकार भगवंत बाधक तत्त्व कहते है। बाधक अर्थात् अंतराय-विघ्न। विघ्न में कंटकविघ्न, ज्वरविघ्न और मोहविघ्न - ये | आचार्य हरिभद्रसूरि का व्यक्तित्व एवं कृतित्व VIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIA षष्ठम् अध्याय ! 408 |