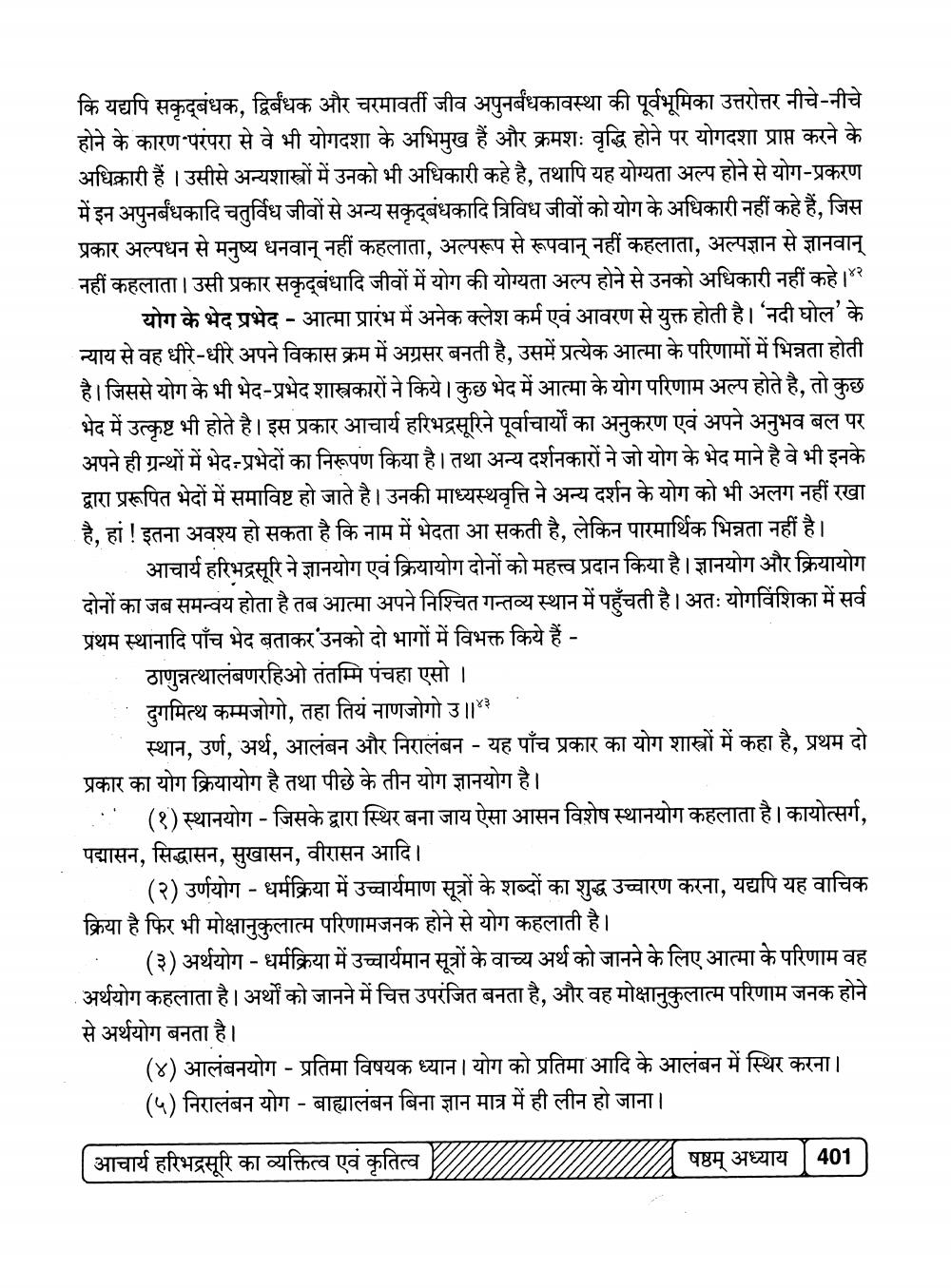________________ कि यद्यपि सकृबंधक, द्विबंधक और चरमावर्ती जीव अपुनर्बंधकावस्था की पूर्वभूमिका उत्तरोत्तर नीचे-नीचे होने के कारण परंपरा से वे भी योगदशा के अभिमुख हैं और क्रमशः वृद्धि होने पर योगदशा प्राप्त करने के अधिकारी हैं / उसीसे अन्यशास्त्रों में उनको भी अधिकारी कहे है, तथापि यह योग्यता अल्प होने से योग-प्रकरण में इन अपुनर्बंधकादि चतुर्विध जीवों से अन्य सकृबंधकादि त्रिविध जीवों को योग के अधिकारी नहीं कहे हैं, जिस प्रकार अल्पधन से मनुष्य धनवान् नहीं कहलाता, अल्परूप से रूपवान् नहीं कहलाता, अल्पज्ञान से ज्ञानवान् नहीं कहलाता। उसी प्रकार सकृबंधादि जीवों में योग की योग्यता अल्प होने से उनको अधिकारी नहीं कहे।४२ योग के भेद प्रभेद - आत्मा प्रारंभ में अनेक क्लेश कर्म एवं आवरण से युक्त होती है। नदी घोल' के न्याय से वह धीरे-धीरे अपने विकास क्रम में अग्रसर बनती है, उसमें प्रत्येक आत्मा के परिणामों में भिन्नता होती है। जिससे योग के भी भेद-प्रभेद शास्त्रकारों ने किये। कुछ भेद में आत्मा के योग परिणाम अल्प होते है, तो कुछ भेद में उत्कृष्ट भी होते है। इस प्रकार आचार्य हरिभद्रसूरिने पूर्वाचार्यों का अनुकरण एवं अपने अनुभव बल पर अपने ही ग्रन्थों में भेद-प्रभेदों का निरूपण किया है। तथा अन्य दर्शनकारों ने जो योग के भेद माने है वे भी इनके द्वारा प्ररूपित भेदों में समाविष्ट हो जाते है। उनकी माध्यस्थवृत्ति ने अन्य दर्शन के योग को भी अलग नहीं रखा है, हां ! इतना अवश्य हो सकता है कि नाम में भेदता आ सकती है, लेकिन पारमार्थिक भिन्नता नहीं है। _____ आचार्य हरिभद्रसूरि ने ज्ञानयोग एवं क्रियायोग दोनों को महत्त्व प्रदान किया है। ज्ञानयोग और क्रियायोग दोनों का जब समन्वय होता है तब आत्मा अपने निश्चित गन्तव्य स्थान में पहुँचती है। अतः योगविंशिका में सर्व प्रथम स्थानादि पाँच भेद बताकर उनको दो भागों में विभक्त किये हैं - ठाणुन्नत्थालंबणरहिओ तंतम्मि पंचहा एसो।। दुगमित्थ कम्मजोगो, तहा तियं नाणजोगो उ॥४३ स्थान, उर्ण, अर्थ, आलंबन और निरालंबन - यह पाँच प्रकार का योग शास्त्रों में कहा है, प्रथम दो प्रकार का योग क्रियायोग है तथा पीछे के तीन योग ज्ञानयोग है। ...' (1) स्थानयोग - जिसके द्वारा स्थिर बना जाय ऐसा आसन विशेष स्थानयोग कहलाता है। कायोत्सर्ग, पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन, वीरासन आदि। (2) उर्णयोग - धर्मक्रिया में उच्चार्यमाण सूत्रों के शब्दों का शुद्ध उच्चारण करना, यद्यपि यह वाचिक क्रिया है फिर भी मोक्षानुकुलात्म परिणामजनक होने से योग कहलाती है। - (3) अर्थयोग - धर्मक्रिया में उच्चार्यमान सूत्रों के वाच्य अर्थ को जानने के लिए आत्मा के परिणाम वह अर्थयोग कहलाता है। अर्थों को जानने में चित्त उपरंजित बनता है, और वह मोक्षानुकुलात्म परिणाम जनक होने से अर्थयोग बनता है। (4) आलंबनयोग - प्रतिमा विषयक ध्यान / योग को प्रतिमा आदि के आलंबन में स्थिर करना। (5) निरालंबन योग - बाह्यालंबन बिना ज्ञान मात्र में ही लीन हो जाना। आचार्य हरिभद्रसूरि का व्यक्तित्व एवं कृतित्व VIIIII IA षष्ठम् अध्याय 401