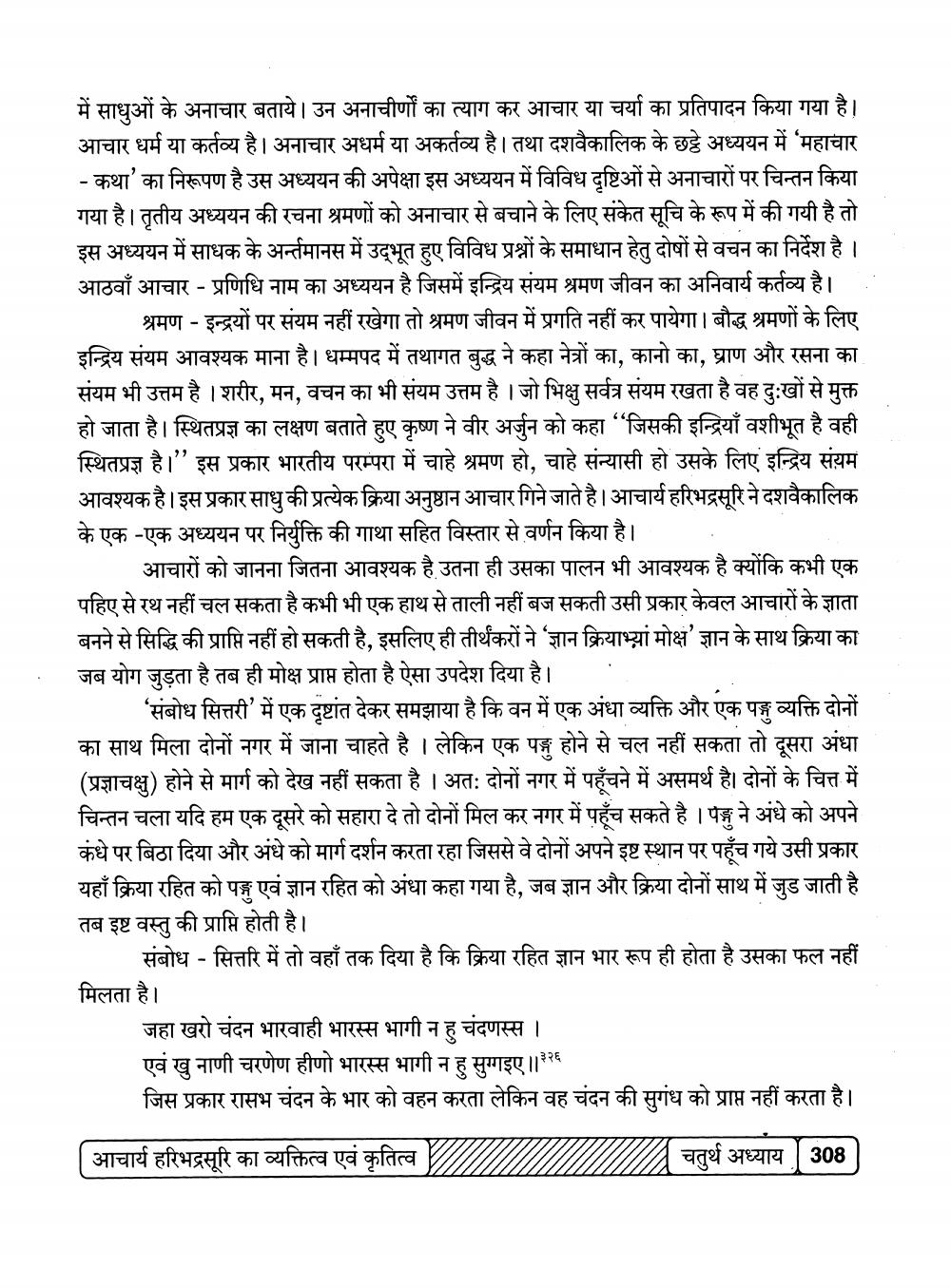________________ में साधुओं के अनाचार बताये। उन अनाची) का त्याग कर आचार या चर्या का प्रतिपादन किया गया है। आचार धर्म या कर्तव्य है। अनाचार अधर्म या अकर्तव्य है। तथा दशवैकालिक के छठे अध्ययन में ‘महाचार - कथा' का निरूपण है उस अध्ययन की अपेक्षा इस अध्ययन में विविध दृष्टिओं से अनाचारों पर चिन्तन किया गया है। तृतीय अध्ययन की रचना श्रमणों को अनाचार से बचाने के लिए संकेत सूचि के रूप में की गयी है तो इस अध्ययन में साधक के अर्तमानस में उद्भूत हुए विविध प्रश्नों के समाधान हेतु दोषों से वचन का निर्देश है / आठवाँ आचार - प्रणिधि नाम का अध्ययन है जिसमें इन्द्रिय संयम श्रमण जीवन का अनिवार्य कर्तव्य है। श्रमण - इन्द्रयों पर संयम नहीं रखेगा तो श्रमण जीवन में प्रगति नहीं कर पायेगा। बौद्ध श्रमणों के लिए इन्द्रिय संयम आवश्यक माना है। धम्मपद में तथागत बुद्ध ने कहा नेत्रों का, कानो का, घ्राण और रसना का संयम भी उत्तम है / शरीर, मन, वचन का भी संयम उत्तम है / जो भिक्षु सर्वत्र संयम रखता है वह दु:खों से मुक्त हो जाता है। स्थितप्रज्ञ का लक्षण बताते हुए कृष्ण ने वीर अर्जुन को कहा “जिसकी इन्द्रियाँ वशीभूत है वही स्थितप्रज्ञ है।" इस प्रकार भारतीय परम्परा में चाहे श्रमण हो, चाहे संन्यासी हो उसके लिए इन्द्रिय संयम आवश्यक है। इस प्रकार साधु की प्रत्येक क्रिया अनुष्ठान आचार गिने जाते है। आचार्य हरिभद्रसूरि ने दशवैकालिक के एक -एक अध्ययन पर नियुक्ति की गाथा सहित विस्तार से वर्णन किया है। आचारों को जानना जितना आवश्यक है उतना ही उसका पालन भी आवश्यक है क्योंकि कभी एक पहिए से रथ नहीं चल सकता है कभी भी एक हाथ से ताली नहीं बज सकती उसी प्रकार केवल आचारों के ज्ञाता बनने से सिद्धि की प्राप्ति नहीं हो सकती है, इसलिए ही तीर्थंकरों ने ज्ञान क्रियाभ्यां मोक्ष' ज्ञान के साथ क्रिया का जब योग जुड़ता है तब ही मोक्ष प्राप्त होता है ऐसा उपदेश दिया है। ___'संबोध सित्तरी' में एक दृष्टांत देकर समझाया है कि वन में एक अंधा व्यक्ति और एक पङ्गु व्यक्ति दोनों का साथ मिला दोनों नगर में जाना चाहते है / लेकिन एक पङ्गु होने से चल नहीं सकता तो दूसरा अंधा (प्रज्ञाचक्षु) होने से मार्ग को देख नहीं सकता है / अत: दोनों नगर में पहुँचने में असमर्थ है। दोनों के चित्त में चिन्तन चला यदि हम एक दूसरे को सहारा दे तो दोनों मिल कर नगर में पहुँच सकते है / पङ्गु ने अंधे को अपने कंधे पर बिठा दिया और अंधे को मार्ग दर्शन करता रहा जिससे वे दोनों अपने इष्ट स्थान पर पहुँच गये उसी प्रकार यहाँ क्रिया रहित को पङ्गु एवं ज्ञान रहित को अंधा कहा गया है, जब ज्ञान और क्रिया दोनों साथ में जुड़ जाती है तब इष्ट वस्तु की प्राप्ति होती है। संबोध - सित्तरि में तो वहाँ तक दिया है कि क्रिया रहित ज्ञान भार रूप ही होता है उसका फल नहीं मिलता है। जहा खरो चंदन भारवाही भारस्स भागी न हु चंदणस्स / एवं खु नाणी चरणेण हीणो भारस्स भागी न हु सुग्गइए // 326 जिस प्रकार रासभ चंदन के भार को वहन करता लेकिन वह चंदन की सुगंध को प्राप्त नहीं करता है। आचार्य हरिभद्रसूरि का व्यक्तित्व एवं कृतित्व VIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIA चतुर्थ अध्याय 308 )