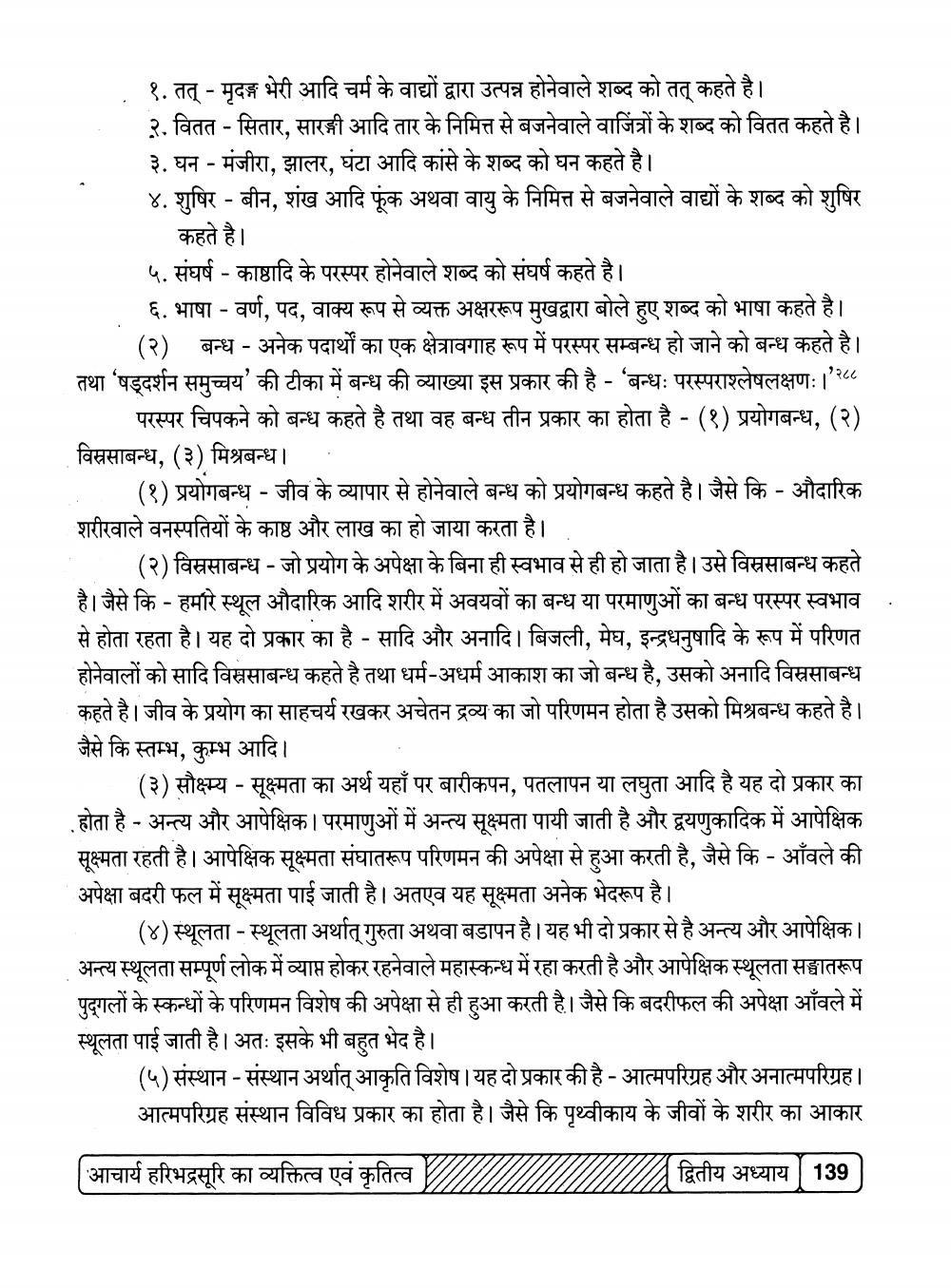________________ 1. तत् - मृदङ्ग भेरी आदि चर्म के वाद्यों द्वारा उत्पन्न होनेवाले शब्द को तत् कहते है। 2. वितत - सितार, सारङ्गी आदि तार के निमित्त से बजनेवाले वाजिंत्रों के शब्द को वितत कहते है। 3. घन - मंजीरा, झालर, घंटा आदि कांसे के शब्द को घन कहते है। 4. शुषिर - बीन, शंख आदि फूंक अथवा वायु के निमित्त से बजनेवाले वाद्यों के शब्द को शुषिर ___ कहते है। 5. संघर्ष - काष्ठादि के परस्पर होनेवाले शब्द को संघर्ष कहते है। 6. भाषा - वर्ण, पद, वाक्य रूप से व्यक्त अक्षररूप मुखद्वारा बोले हुए शब्द को भाषा कहते है। (2) बन्ध - अनेक पदार्थों का एक क्षेत्रावगाह रूप में परस्पर सम्बन्ध हो जाने को बन्ध कहते है। तथा षड्दर्शन समुच्चय' की टीका में बन्ध की व्याख्या इस प्रकार की है - ‘बन्धः परस्पराश्लेषलक्षणः / 288 परस्पर चिपकने को बन्ध कहते है तथा वह बन्ध तीन प्रकार का होता है - (1) प्रयोगबन्ध, (2) विस्रसाबन्ध, (3) मिश्रबन्ध। . (1) प्रयोगबन्ध - जीव के व्यापार से होनेवाले बन्ध को प्रयोगबन्ध कहते है। जैसे कि - औदारिक शरीरवाले वनस्पतियों के काष्ठ और लाख का हो जाया करता है। (2) विस्रसाबन्ध - जो प्रयोग के अपेक्षा के बिना ही स्वभाव से ही हो जाता है। उसे विस्रसाबन्ध कहते है। जैसे कि - हमारे स्थूल औदारिक आदि शरीर में अवयवों का बन्ध या परमाणुओं का बन्ध परस्पर स्वभाव . से होता रहता है। यह दो प्रकार का है - सादि और अनादि। बिजली, मेघ, इन्द्रधनुषादि के रूप में परिणत होनेवालों को सादि विस्रसाबन्ध कहते है तथा धर्म-अधर्म आकाश का जो बन्ध है, उसको अनादि विस्रसाबन्ध कहते है। जीव के प्रयोग का साहचर्य रखकर अचेतन द्रव्य का जो परिणमन होता है उसको मिश्रबन्ध कहते है। जैसे कि स्तम्भ, कुम्भ आदि। (3) सौक्ष्म्य - सूक्ष्मता का अर्थ यहाँ पर बारीकपन, पतलापन या लघुता आदि है यह दो प्रकार का होता है - अन्त्य और आपेक्षिक। परमाणुओं में अन्त्य सूक्ष्मता पायी जाती है और द्वयणुकादिक में आपेक्षिक सूक्ष्मता रहती है। आपेक्षिक सूक्ष्मता संघातरूप परिणमन की अपेक्षा से हुआ करती है, जैसे कि - आँवले की अपेक्षा बदरी फल में सूक्ष्मता पाई जाती है। अतएव यह सूक्ष्मता अनेक भेदरूप है। (4) स्थूलता - स्थूलता अर्थात् गुरुता अथवा बडापन है। यह भी दो प्रकार से है अन्त्य और आपेक्षिक। अन्त्य स्थूलता सम्पूर्ण लोक में व्याप्त होकर रहनेवाले महास्कन्ध में रहा करती है और आपेक्षिक स्थूलता सङ्घातरूप पुद्गलों के स्कन्धों के परिणमन विशेष की अपेक्षा से ही हुआ करती है। जैसे कि बदरीफल की अपेक्षा आँवले में स्थूलता पाई जाती है। अतः इसके भी बहुत भेद है। (5) संस्थान - संस्थान अर्थात् आकृति विशेष / यह दो प्रकार की है - आत्मपरिग्रह और अनात्मपरिग्रह / आत्मपरिग्रह संस्थान विविध प्रकार का होता है। जैसे कि पृथ्वीकाय के जीवों के शरीर का आकार | आचार्य हरिभद्रसूरि का व्यक्तित्व एवं कृतित्व VII IA द्वितीय अध्याय | 139