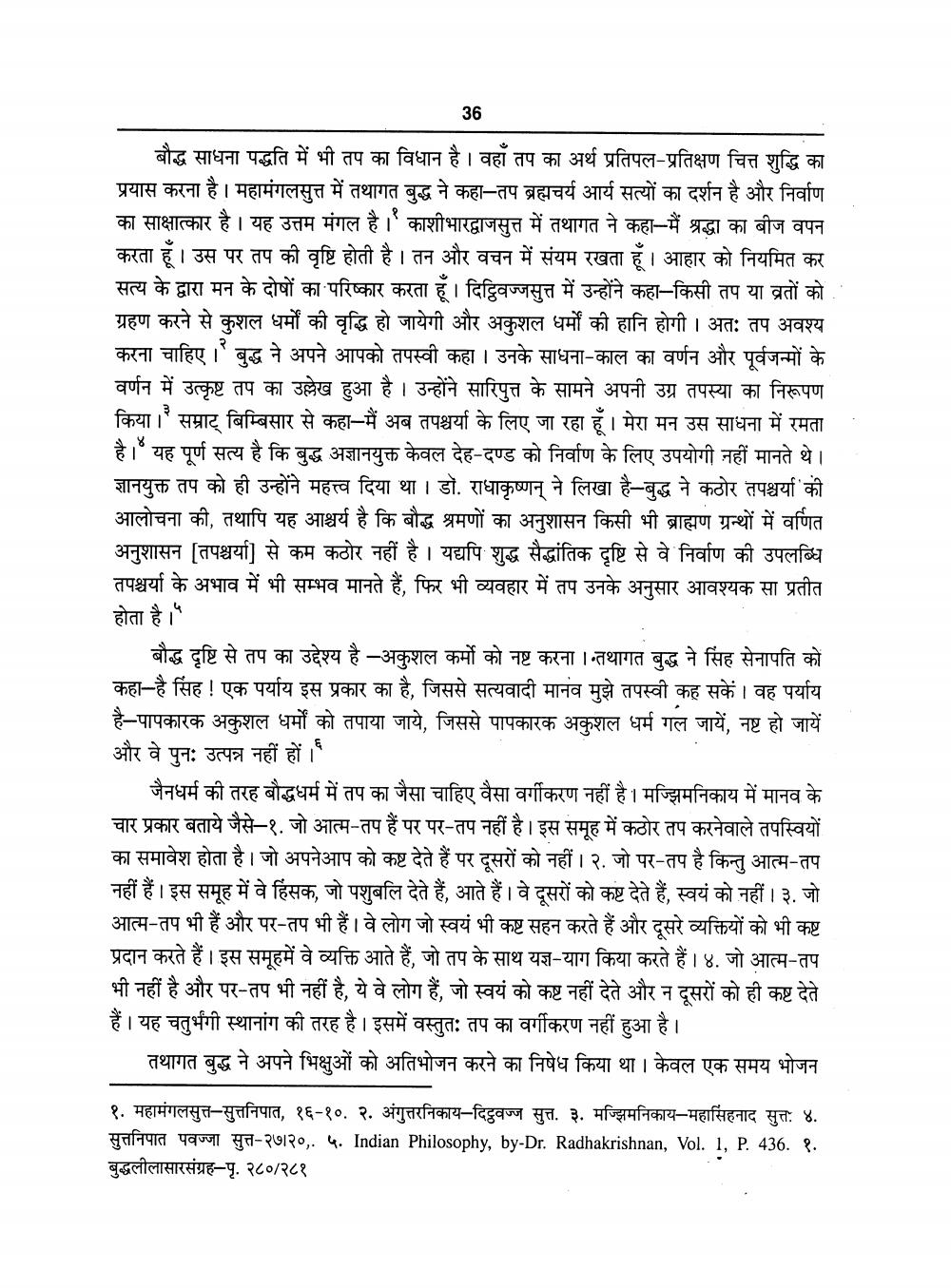________________ 36 बौद्ध साधना पद्धति में भी तप का विधान है। वहाँ तप का अर्थ प्रतिपल-प्रतिक्षण चित्त शुद्धि का प्रयास करना है। महामंगलसुत्त में तथागत बुद्ध ने कहा-तप ब्रह्मचर्य आर्य सत्यों का दर्शन है और निर्वाण का साक्षात्कार है। यह उत्तम मंगल है। काशीभारद्वाजसुत्त में तथागत ने कहा-मैं श्रद्धा का बीज वपन करता हूँ। उस पर तप की वृष्टि होती है। तन और वचन में संयम रखता हूँ। आहार को नियमित कर सत्य के द्वारा मन के दोषों का परिष्कार करता हूँ। दिट्ठिवज्जसुत्त में उन्होंने कहा-किसी तप या व्रतों को ग्रहण करने से कुशल धर्मों की वृद्धि हो जायेगी और अकुशल धर्मों की हानि होगी। अतः तप अवश्य करना चाहिए / बुद्ध ने अपने आपको तपस्वी कहा / उनके साधना-काल का वर्णन और पूर्वजन्मों के वर्णन में उत्कृष्ट तप का उल्लेख हुआ है / उन्होंने सारिपुत्त के सामने अपनी उग्र तपस्या का निरूपण किया। सम्राट् बिम्बिसार से कहा-मैं अब तपश्चर्या के लिए जा रहा हूँ। मेरा मन उस साधना में रमता है। यह पूर्ण सत्य है कि बुद्ध अज्ञानयुक्त केवल देह-दण्ड को निर्वाण के लिए उपयोगी नहीं मानते थे। ज्ञानयुक्त तप को ही उन्होंने महत्त्व दिया था। डॉ. राधाकृष्णन् ने लिखा है-बुद्ध ने कठोर तपश्चर्या की आलोचना की, तथापि यह आश्चर्य है कि बौद्ध श्रमणों का अनुशासन किसी भी ब्राह्मण ग्रन्थों में वर्णित अनुशासन [तपश्चर्या] से कम कठोर नहीं है / यद्यपि शुद्ध सैद्धांतिक दृष्टि से वे निर्वाण की उपलब्धि तपश्चर्या के अभाव में भी सम्भव मानते हैं. फिर भी व्यवहार में तप उनके अनुसार आवश्यक सा प्रतीत होता है। बौद्ध दृष्टि से तप का उद्देश्य है -अकुशल कर्मो को नष्ट करना / तथागत बुद्ध ने सिंह सेनापति को कहा है सिंह ! एक पर्याय इस प्रकार का है, जिससे सत्यवादी मानव मुझे तपस्वी कह सकें। वह पर्याय है-पापकारक अकुशल धर्मों को तपाया जाये, जिससे पापकारक अकुशल धर्म गल जायें, नष्ट हो जायें और वे पुनः उत्पन्न नहीं हों। जैनधर्म की तरह बौद्धधर्म में तप का जैसा चाहिए वैसा वर्गीकरण नहीं है। मज्झिमनिकाय में मानव के चार प्रकार बताये जैसे-१. जो आत्म-तप हैं पर पर-तप नहीं है। इस समूह में कठोर तप करनेवाले तपस्वियों का समावेश होता है। जो अपनेआप को कष्ट देते हैं पर दूसरों को नहीं / 2. जो पर-तप है किन्तु आत्म-तप नहीं हैं। इस समूह में वे हिंसक, जो पशुबलि देते हैं, आते हैं। वे दूसरों को कष्ट देते हैं, स्वयं को नहीं / 3. जो आत्म-तप भी हैं और पर-तप भी हैं। वे लोग जो स्वयं भी कष्ट सहन करते हैं और दूसरे व्यक्तियों को भी कष्ट प्रदान करते हैं। इस समूहमें वे व्यक्ति आते हैं, जो तप के साथ यज्ञ-याग किया करते हैं। 4. जो आत्म-तप भी नहीं है और पर-तप भी नहीं है, ये वे लोग हैं, जो स्वयं को कष्ट नहीं देते और न दूसरों को ही कष्ट देते हैं। यह चतुर्भगी स्थानांग की तरह है। इसमें वस्तुतः तप का वर्गीकरण नहीं हुआ है। तथागत बुद्ध ने अपने भिक्षुओं को अतिभोजन करने का निषेध किया था। केवल एक समय भोजन 1. महामंगलसुत्त-सुत्तनिपात, 16-10. 2. अंगुत्तरनिकाय-दिट्ठवज्ज सुत्त. 3. मज्झिमनिकाय-महासिंहनाद सुत्त: 4. सुत्तनिपात पवज्जा सुत्त-२७।२०,. 5. Indian Philosophy, by-Dr. Radhakrishnan, Vol. 1, P. 436. 1. बुद्धलीलासारसंग्रह-पृ. 280/281