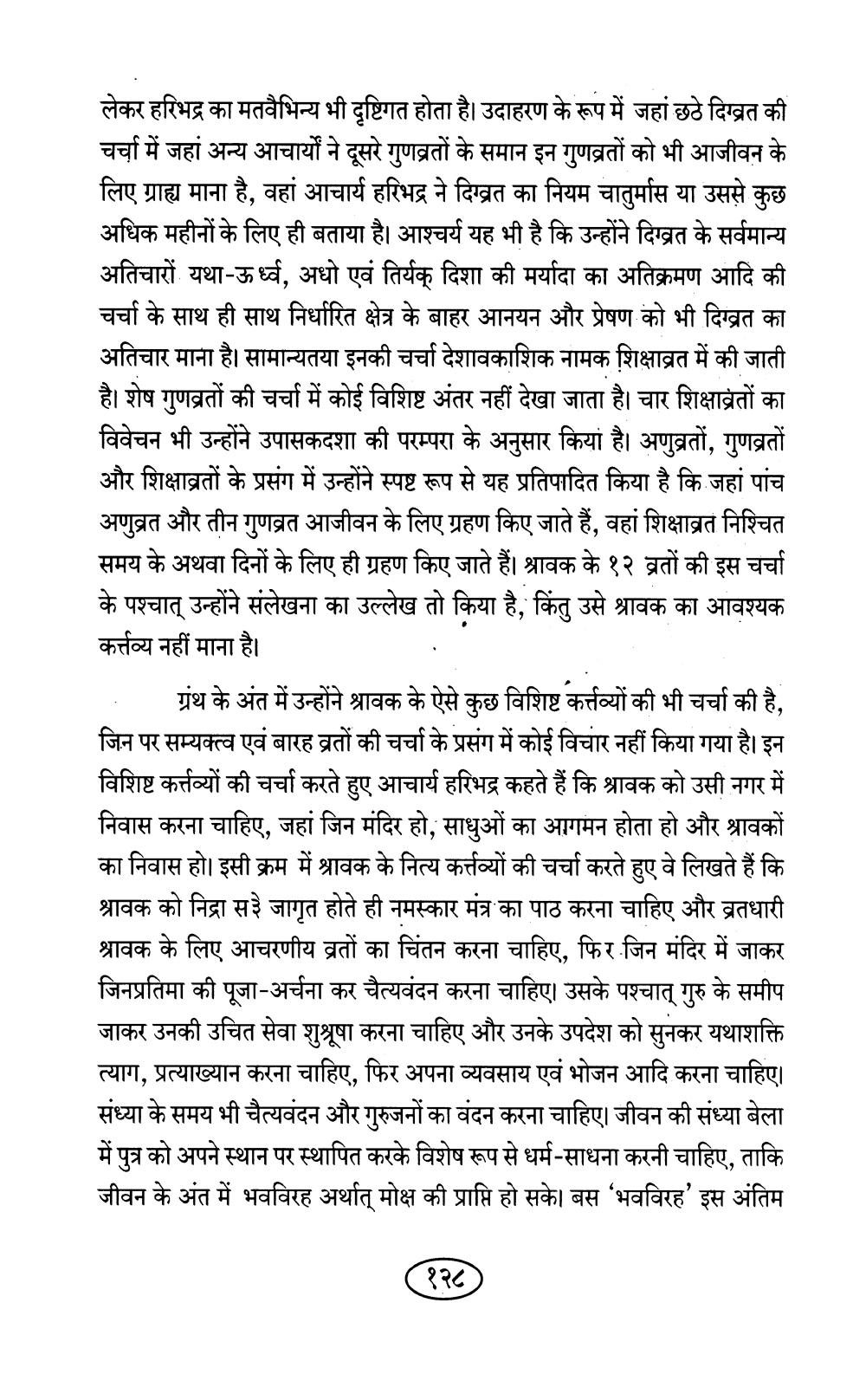________________ लेकर हरिभद्र का मतवैभिन्य भी दृष्टिगत होता है। उदाहरण के रूप में जहां छठे दिग्वत की चर्चा में जहां अन्य आचार्यों ने दूसरे गुणव्रतों के समान इन गुणव्रतों को भी आजीवन के लिए ग्राह्य माना है, वहां आचार्य हरिभद्र ने दिव्रत का नियम चातुर्मास या उससे कुछ अधिक महीनों के लिए ही बताया है। आश्चर्य यह भी है कि उन्होंने दिव्रत के सर्वमान्य अतिचारों यथा-ऊर्ध्व, अधो एवं तिर्यक् दिशा की मर्यादा का अतिक्रमण आदि की चर्चा के साथ ही साथ निर्धारित क्षेत्र के बाहर आनयन और प्रेषण को भी दिग्व्रत का अतिचार माना है। सामान्यतया इनकी चर्चा देशावकाशिक नामक शिक्षाव्रत में की जाती है। शेष गुणव्रतों की चर्चा में कोई विशिष्ट अंतर नहीं देखा जाता है। चार शिक्षाव्रतों का विवेचन भी उन्होंने उपासकदशा की परम्परा के अनुसार किया है। अणुव्रतों, गुणव्रतों और शिक्षाव्रतों के प्रसंग में उन्होंने स्पष्ट रूप से यह प्रतिपादित किया है कि जहां पांच अणुव्रत और तीन गुणव्रत आजीवन के लिए ग्रहण किए जाते हैं, वहां शिक्षाव्रत निश्चित समय के अथवा दिनों के लिए ही ग्रहण किए जाते हैं। श्रावक के 12 व्रतों की इस चर्चा के पश्चात् उन्होंने संलेखना का उल्लेख तो किया है, किंतु उसे श्रावक का आवश्यक कर्त्तव्य नहीं माना है। ग्रंथ के अंत में उन्होंने श्रावक के ऐसे कुछ विशिष्ट कर्त्तव्यों की भी चर्चा की है, जिन पर सम्यक्त्व एवं बारह व्रतों की चर्चा के प्रसंग में कोई विचार नहीं किया गया है। इन विशिष्ट कर्त्तव्यों की चर्चा करते हुए आचार्य हरिभद्र कहते हैं कि श्रावक को उसी नगर में निवास करना चाहिए, जहां जिन मंदिर हो, साधुओं का आगमन होता हो और श्रावकों का निवास हो। इसी क्रम में श्रावक के नित्य कर्तव्यों की चर्चा करते हुए वे लिखते हैं कि श्रावक को निद्रा सरे जागृत होते ही नमस्कार मंत्र का पाठ करना चाहिए और व्रतधारी श्रावक के लिए आचरणीय व्रतों का चिंतन करना चाहिए, फिर जिन मंदिर में जाकर जिनप्रतिमा की पूजा-अर्चना कर चैत्यवंदन करना चाहिए। उसके पश्चात् गुरु के समीप जाकर उनकी उचित सेवा शुश्रूषा करना चाहिए और उनके उपदेश को सुनकर यथाशक्ति त्याग, प्रत्याख्यान करना चाहिए, फिर अपना व्यवसाय एवं भोजन आदि करना चाहिए। संध्या के समय भी चैत्यवंदन और गुरुजनों का वंदन करना चाहिए। जीवन की संध्या बेला में पुत्र को अपने स्थान पर स्थापित करके विशेष रूप से धर्म-साधना करनी चाहिए, ताकि जीवन के अंत में भवविरह अर्थात् मोक्ष की प्राप्ति हो सके। बस ‘भवविरह' इस अंतिम (128)