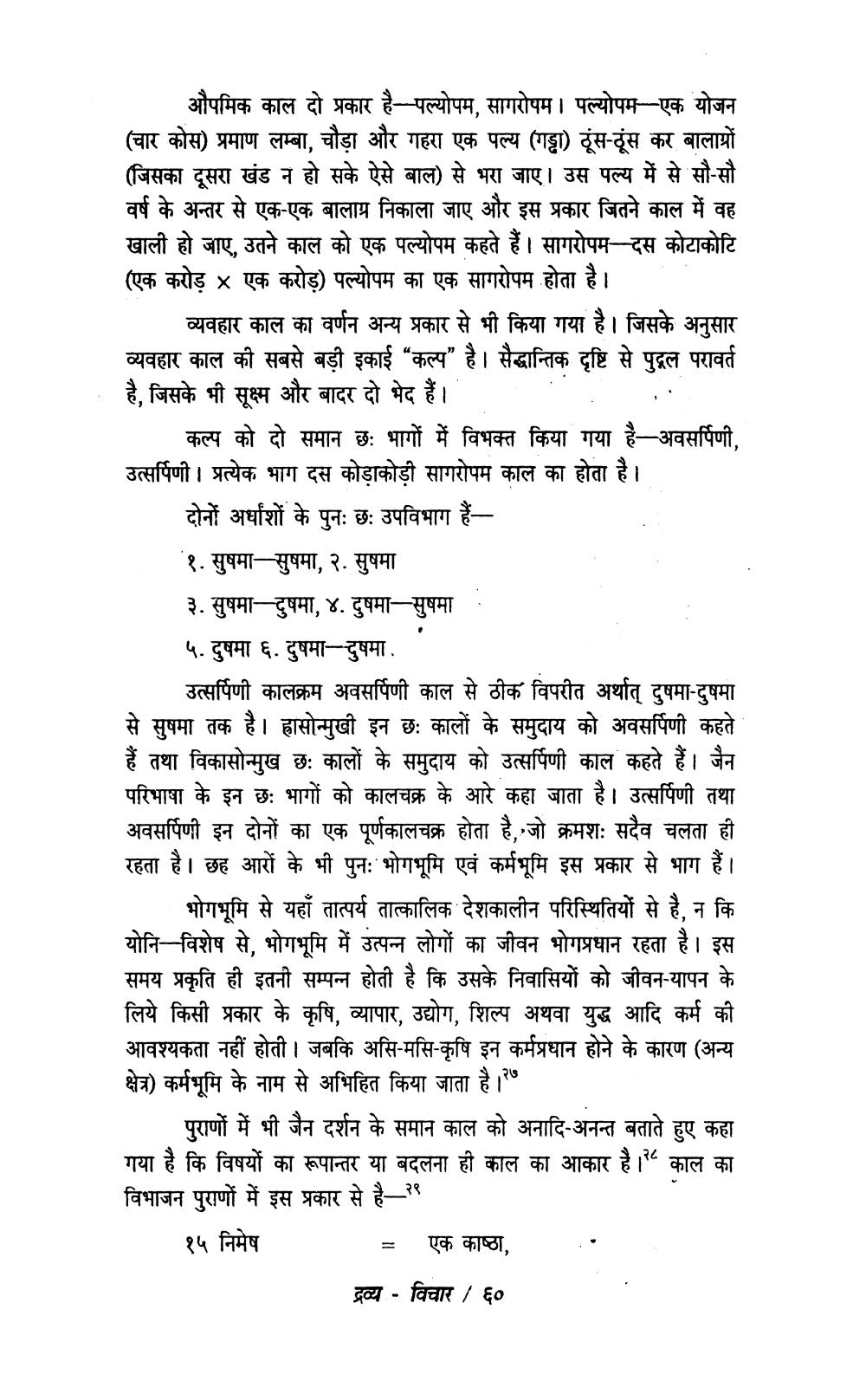________________ औपमिक काल दो प्रकार है-पल्योपम, सागरोपम। पल्योपम-एक योजन (चार कोस) प्रमाण लम्बा, चौड़ा और गहरा एक पल्य (गड्डा) ढूंस-ढूंस कर बालानों (जिसका दूसरा खंड न हो सके ऐसे बाल) से भरा जाए। उस पल्य में से सौ-सौ वर्ष के अन्तर से एक-एक बालाग्र निकाला जाए और इस प्रकार जितने काल में वह खाली हो जाए, उतने काल को एक पल्योपम कहते हैं। सागरोपम-दस कोटाकोटि (एक करोड़ x एक करोड़) पल्योपम का एक सागरोपम होता है। व्यवहार काल का वर्णन अन्य प्रकार से भी किया गया है। जिसके अनुसार व्यवहार काल की सबसे बड़ी इकाई “कल्प” है। सैद्धान्तिक दृष्टि से पुद्गल परावर्त है, जिसके भी सूक्ष्म और बादर दो भेद हैं। कल्प को दो समान छ: भागों में विभक्त किया गया है-अवसर्पिणी, उत्सर्पिणी। प्रत्येक भाग दस कोड़ाकोड़ी सागरोपम काल का होता है। दोनों अर्धांशों के पुनः छः उपविभाग हैं१. सुषमा सुषमा, 2. सुषमा 3. सुषमा दुषमा, 4. दुषमा-सुषमा 5. दुषमा 6. दुषमा-दुषमा. उत्सर्पिणी कालक्रम अवसर्पिणी काल से ठीक विपरीत अर्थात् दुषमा-दुषमा से सुषमा तक है। हासोन्मुखी इन छ: कालों के समुदाय को अवसर्पिणी कहते हैं तथा विकासोन्मुख छ: कालों के समुदाय को उत्सर्पिणी काल कहते हैं। जैन परिभाषा के इन छ: भागों को कालचक्र के आरे कहा जाता है। उत्सर्पिणी तथा अवसर्पिणी इन दोनों का एक पूर्णकालचक्र होता है, जो क्रमशः सदैव चलता ही रहता है। छह आरों के भी पुनः भोगभूमि एवं कर्मभूमि इस प्रकार से भाग हैं। भोगभूमि से यहाँ तात्पर्य तात्कालिक देशकालीन परिस्थितियों से है, न कि योनि-विशेष से, भोगभूमि में उत्पन्न लोगों का जीवन भोगप्रधान रहता है। इस समय प्रकृति ही इतनी सम्पन्न होती है कि उसके निवासियों को जीवन-यापन के लिये किसी प्रकार के कृषि, व्यापार, उद्योग, शिल्प अथवा युद्ध आदि कर्म की आवश्यकता नहीं होती। जबकि असि-मसि-कृषि इन कर्मप्रधान होने के कारण (अन्य क्षेत्र) कर्मभूमि के नाम से अभिहित किया जाता है।२७ पुराणों में भी जैन दर्शन के समान काल को अनादि-अनन्त बताते हुए कहा गया है कि विषयों का रूपान्तर या बदलना ही काल का आकार है। काल का विभाजन पुराणों में इस प्रकार से है-२९ 15 निमेष = एक काष्ठा, द्रव्य - विचार / 60