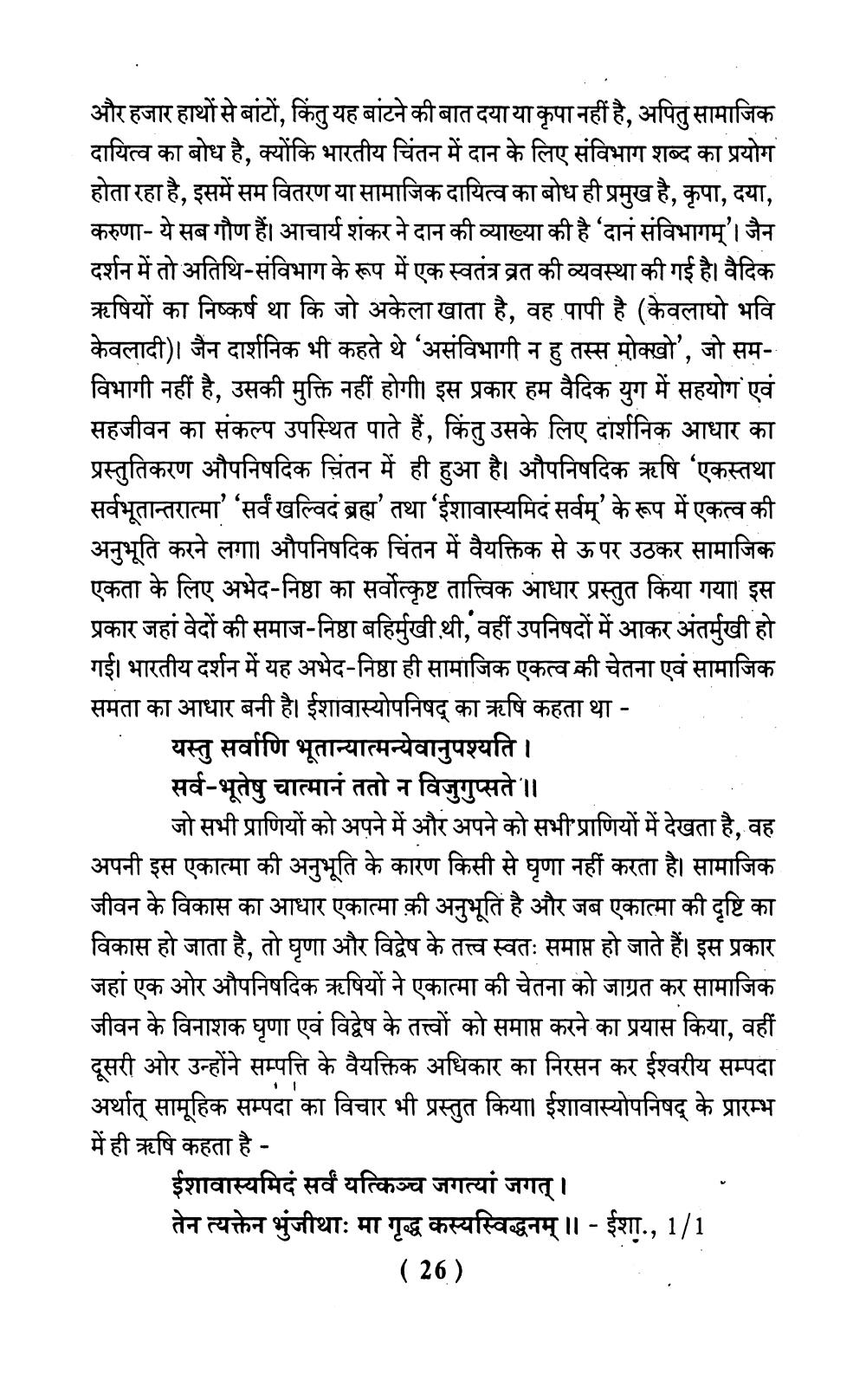________________ और हजार हाथों से बांटों, किंतु यह बांटने की बात दया या कृपा नहीं है, अपितु सामाजिक दायित्व का बोध है, क्योंकि भारतीय चिंतन में दान के लिए संविभाग शब्द का प्रयोग होता रहा है, इसमें सम वितरण या सामाजिक दायित्व का बोध ही प्रमुख है, कृपा, दया, करुणा- ये सब गौण हैं। आचार्य शंकर ने दान की व्याख्या की है ‘दानं संविभागम्'। जैन दर्शन में तो अतिथि-संविभाग के रूप में एक स्वतंत्र व्रत की व्यवस्था की गई है। वैदिक ऋषियों का निष्कर्ष था कि जो अकेला खाता है, वह पापी है (केवलाघो भवि केवलादी)। जैन दार्शनिक भी कहते थे 'असंविभागी न हु तस्स मोक्खो', जो समविभागी नहीं है, उसकी मुक्ति नहीं होगी। इस प्रकार हम वैदिक युग में सहयोग एवं सहजीवन का संकल्प उपस्थित पाते हैं, किंतु उसके लिए दार्शनिक आधार का प्रस्तुतिकरण औपनिषदिक चिंतन में ही हुआ है। औपनिषदिक ऋषि ‘एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा' 'सर्वं खल्विदं ब्रह्म' तथा ईशावास्यमिदं सर्वम्' के रूप में एकत्व की अनुभूति करने लगा। औपनिषदिक चिंतन में वैयक्तिक से ऊपर उठकर सामाजिक एकता के लिए अभेद-निष्ठा का सर्वोत्कृष्ट तात्त्विक आधार प्रस्तुत किया गया। इस प्रकार जहां वेदों की समाज-निष्ठा बहिर्मुखी थी, वहीं उपनिषदों में आकर अंतर्मुखी हो गई। भारतीय दर्शन में यह अभेद-निष्ठा ही सामाजिक एकत्व की चेतना एवं सामाजिक समता का आधार बनी है। ईशावास्योपनिषद् का ऋषि कहता था - यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्येवानुपश्यति / सर्व-भूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते॥ जो सभी प्राणियों को अपने में और अपने को सभी प्राणियों में देखता है, वह अपनी इस एकात्मा की अनुभूति के कारण किसी से घृणा नहीं करता है। सामाजिक जीवन के विकास का आधार एकात्मा की अनुभूति है और जब एकात्मा की दृष्टि का विकास हो जाता है, तो घृणा और विद्वेष के तत्त्व स्वतः समाप्त हो जाते हैं। इस प्रकार जहां एक ओर औपनिषदिक ऋषियों ने एकात्मा की चेतना को जाग्रत कर सामाजिक जीवन के विनाशक घृणा एवं विद्वेष के तत्त्वों को समाप्त करने का प्रयास किया, वहीं दूसरी ओर उन्होंने सम्पत्ति के वैयक्तिक अधिकार का निरसन कर ईश्वरीय सम्पदा अर्थात् सामूहिक सम्पदा का विचार भी प्रस्तुत किया। ईशावास्योपनिषद् के प्रारम्भ में ही ऋषि कहता है - ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् / तेन त्यक्तेन भुंजीथाः मा गृद्ध कस्यस्विद्धनम् / / - ईशा., 1/1 (26)