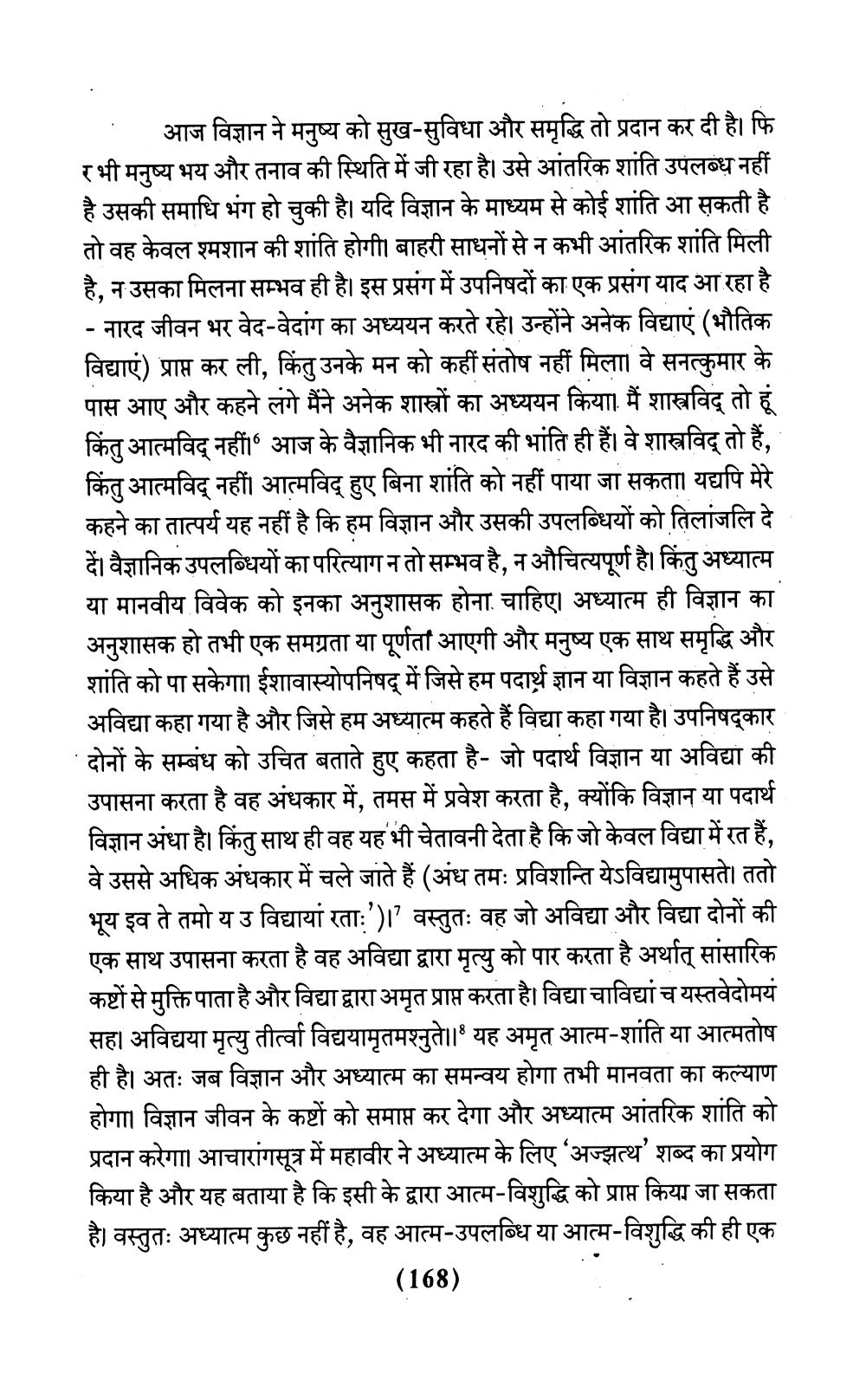________________ - आज विज्ञान ने मनुष्य को सुख-सुविधा और समृद्धि तो प्रदान कर दी है। फि र भी मनुष्य भय और तनाव की स्थिति में जी रहा है। उसे आंतरिक शांति उपलब्ध नहीं है उसकी समाधि भंग हो चुकी है। यदि विज्ञान के माध्यम से कोई शांति आ सकती है तो वह केवल श्मशान की शांति होगी। बाहरी साधनों से न कभी आंतरिक शांति मिली है, न उसका मिलना सम्भव ही है। इस प्रसंग में उपनिषदों का एक प्रसंग याद आ रहा है - नारद जीवन भर वेद-वेदांग का अध्ययन करते रहे। उन्होंने अनेक विद्याएं (भौतिक विद्याएं) प्राप्त कर ली, किंतु उनके मन को कहीं संतोष नहीं मिला। वे सनत्कुमार के पास आए और कहने लगे मैंने अनेक शास्त्रों का अध्ययन किया। मैं शास्त्रविद् तो हूं किंतु आत्मविद् नहीं। आज के वैज्ञानिक भी नारद की भांति ही हैं। वे शास्त्रविद् तो हैं, किंतु आत्मविद् नहीं। आत्मविद् हुए बिना शांति को नहीं पाया जा सकता। यद्यपि मेरे कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि हम विज्ञान और उसकी उपलब्धियों को तिलांजलि दे दें। वैज्ञानिक उपलब्धियों का परित्याग न तो सम्भव है, न औचित्यपूर्ण है। किंतु अध्यात्म या मानवीय विवेक को इनका अनुशासक होना चाहिए। अध्यात्म ही विज्ञान का अनुशासक हो तभी एक समग्रता या पूर्णता आएगी और मनुष्य एक साथ समृद्धि और शांति को पा सकेगा। ईशावास्योपनिषद् में जिसे हम पदार्थ ज्ञान या विज्ञान कहते हैं उसे अविद्या कहा गया है और जिसे हम अध्यात्म कहते हैं विद्या कहा गया है। उपनिषद्कार दोनों के सम्बंध को उचित बताते हुए कहता है- जो पदार्थ विज्ञान या अविद्या की उपासना करता है वह अंधकार में, तमस में प्रवेश करता है, क्योंकि विज्ञान या पदार्थ विज्ञान अंधा है। किंतु साथ ही वह यह भी चेतावनी देता है कि जो केवल विद्या में रत हैं, वे उससे अधिक अंधकार में चले जाते हैं (अंध तमः प्रविशन्ति येऽविद्यामुपासते। ततो भूय इव ते तमो य उ विद्यायां रताः')।' वस्तुतः वह जो अविद्या और विद्या दोनों की एक साथ उपासना करता है वह अविद्या द्वारा मृत्यु को पार करता है अर्थात् सांसारिक कष्टों से मुक्ति पाता है और विद्या द्वारा अमृत प्राप्त करता है। विद्या चाविद्यां च यस्तवेदोमयं सह। अविद्यया मृत्यु तीा विद्ययामृतमश्नुते।।' यह अमृत आत्म-शांति या आत्मतोष ही है। अतः जब विज्ञान और अध्यात्म का समन्वय होगा तभी मानवता का कल्याण होगा। विज्ञान जीवन के कष्टों को समाप्त कर देगा और अध्यात्म आंतरिक शांति को प्रदान करेगा। आचारांगसूत्र में महावीर ने अध्यात्म के लिए 'अज्झत्थ' शब्द का प्रयोग किया है और यह बताया है कि इसी के द्वारा आत्म-विशुद्धि को प्राप्त किया जा सकता है। वस्तुतः अध्यात्म कुछ नहीं है, वह आत्म-उपलब्धि या आत्म-विशुद्धि की ही एक (168)