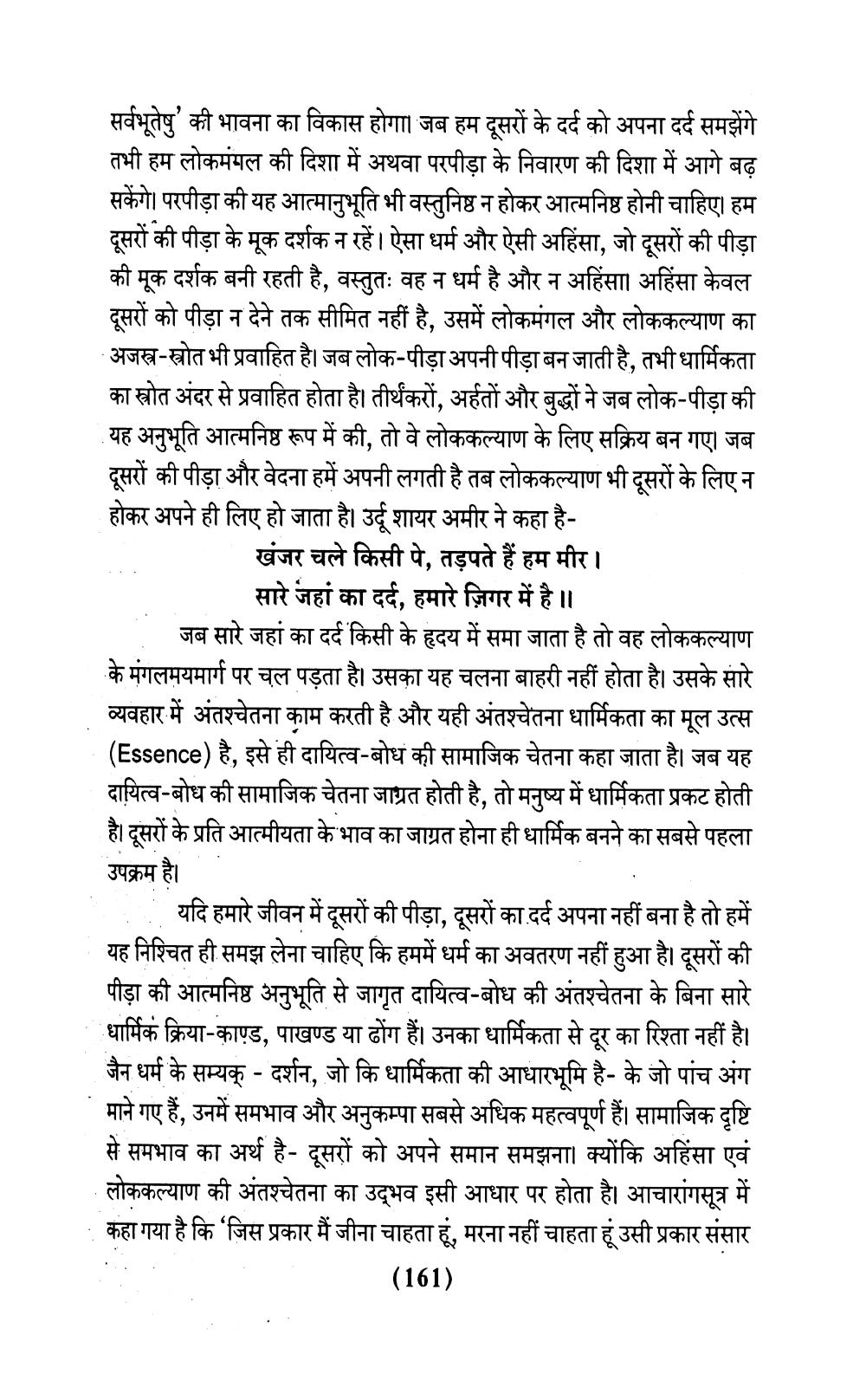________________ सर्वभूतेषु' की भावना का विकास होगा। जब हम दूसरों के दर्द को अपना दर्द समझेंगे तभी हम लोकमंगल की दिशा में अथवा परपीड़ा के निवारण की दिशा में आगे बढ़ सकेंगे। परपीड़ा की यह आत्मानुभूति भी वस्तुनिष्ठ न होकर आत्मनिष्ठ होनी चाहिए। हम दूसरों की पीड़ा के मूक दर्शक न रहें। ऐसा धर्म और ऐसी अहिंसा, जो दूसरों की पीड़ा की मूक दर्शक बनी रहती है, वस्तुतः वह न धर्म है और न अहिंसा। अहिंसा केवल दूसरों को पीड़ा न देने तक सीमित नहीं है, उसमें लोकमंगल और लोककल्याण का अजस्त्र-स्त्रोत भी प्रवाहित है। जब लोक-पीड़ा अपनी पीड़ा बन जाती है, तभी धार्मिकता का स्त्रोत अंदर से प्रवाहित होता है। तीर्थंकरों, अर्हतों और बुद्धों ने जब लोक-पीड़ा की यह अनुभूति आत्मनिष्ठ रूप में की, तो वे लोककल्याण के लिए सक्रिय बन गए। जब दूसरों की पीड़ा और वेदना हमें अपनी लगती है तब लोककल्याण भी दूसरों के लिए न होकर अपने ही लिए हो जाता है। उर्दू शायर अमीर ने कहा है खंजर चले किसी पे, तड़पते हैं हम मीर। सारे जहां का दर्द, हमारे ज़िगर में है। .. जब सारे जहां का दर्द किसी के हृदय में समा जाता है तो वह लोककल्याण के मंगलमयमार्ग पर चल पड़ता है। उसका यह चलना बाहरी नहीं होता है। उसके सारे व्यवहार में अंतश्चेतना काम करती है और यही अंतश्चेतना धार्मिकता का मूल उत्स (Essence) है, इसे ही दायित्व-बोध की सामाजिक चेतना कहा जाता है। जब यह दायित्व-बोध की सामाजिक चेतना जाग्रत होती है, तो मनुष्य में धार्मिकता प्रकट होती है। दूसरों के प्रति आत्मीयता के भाव का जाग्रत होना ही धार्मिक बनने का सबसे पहला उपक्रम है। यदि हमारे जीवन में दूसरों की पीड़ा, दूसरों का दर्द अपना नहीं बना है तो हमें यह निश्चित ही समझ लेना चाहिए कि हममें धर्म का अवतरण नहीं हुआ है। दूसरों की पीड़ा की आत्मनिष्ठ अनुभूति से जागृत दायित्व-बोध की अंतश्चेतना के बिना सारे धार्मिक क्रिया-काण्ड, पाखण्ड या ढोंग हैं। उनका धार्मिकता से दूर का रिश्ता नहीं है। जैन धर्म के सम्यक् - दर्शन, जो कि धार्मिकता की आधारभूमि है- के जो पांच अंग माने गए हैं, उनमें समभाव और अनुकम्पा सबसे अधिक महत्वपूर्ण हैं। सामाजिक दृष्टि से समभाव का अर्थ है- दूसरों को अपने समान समझना। क्योंकि अहिंसा एवं लोककल्याण की अंतश्चेतना का उद्भव इसी आधार पर होता है। आचारांगसूत्र में कहा गया है कि जिस प्रकार मैं जीना चाहता हूं, मरना नहीं चाहता हूं उसी प्रकार संसार (161)