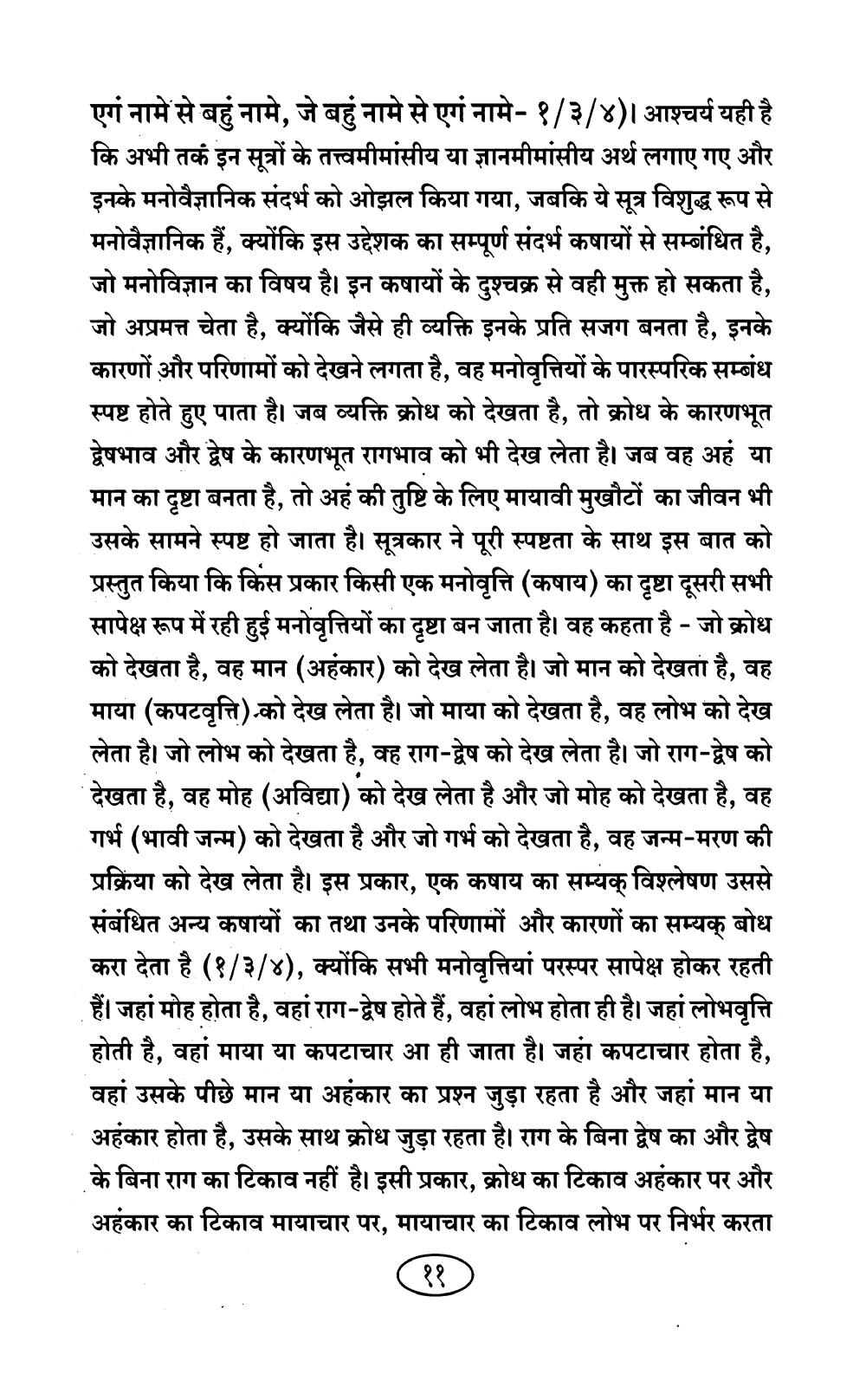________________ एगं नामें से बहुं नामे, जे बहुं नामे से एगं नामे- 1/3/4) / आश्चर्य यही है कि अभी तकं इन सूत्रों के तत्त्वमीमांसीय या ज्ञानमीमांसीय अर्थ लगाए गए और इनके मनोवैज्ञानिक संदर्भ को ओझल किया गया, जबकि ये सूत्र विशुद्ध रूप से मनोवैज्ञानिक हैं, क्योंकि इस उद्देशक का सम्पूर्ण संदर्भ कषायों से सम्बंधित है, जो मनोविज्ञान का विषय है। इन कषायों के दुश्चक्र से वही मुक्त हो सकता है, जो अप्रमत्त चेता है, क्योंकि जैसे ही व्यक्ति इनके प्रति सजग बनता है, इनके कारणों और परिणामों को देखने लगता है, वह मनोवृत्तियों के पारस्परिक सम्बंध स्पष्ट होते हुए पाता है। जब व्यक्ति क्रोध को देखता है, तो क्रोध के कारणभूत द्वेषभाव और द्वेष के कारणभूत रागभाव को भी देख लेता है। जब वह अहं या मान का दृष्टा बनता है, तो अहं की तुष्टि के लिए मायावी मुखौटों का जीवन भी उसके सामने स्पष्ट हो जाता है। सूत्रकार ने पूरी स्पष्टता के साथ इस बात को प्रस्तुत किया कि किस प्रकार किसी एक मनोवृत्ति (कषाय) का दृष्टा दूसरी सभी सापेक्ष रूप में रही हुई मनोवृत्तियों का दृष्टा बन जाता है। वह कहता है - जो क्रोध को देखता है, वह मान (अहंकार) को देख लेता है। जो मान को देखता है, वह माया (कपटवृत्ति) को देख लेता है। जो माया को देखता है, वह लोभ को देख लेता है। जो लोभ को देखता है, वह राग-द्वेष को देख लेता है। जो राग-द्वेष को देखता है, वह मोह (अविद्या) को देख लेता है और जो मोह को देखता है, वह गर्भ (भावी जन्म) को देखता है और जो गर्भ को देखता है, वह जन्म-मरण की प्रक्रिया को देख लेता है। इस प्रकार, एक कषाय का सम्यक् विश्लेषण उससे संबंधित अन्य कषायों का तथा उनके परिणामों और कारणों का सम्यक् बोध करा देता है (1/3/4), क्योंकि सभी मनोवृत्तियां परस्पर सापेक्ष होकर रहती हैं। जहां मोह होता है, वहां राग-द्वेष होते हैं, वहां लोभ होता ही है। जहां लोभवृत्ति होती है, वहां माया या कपटाचार आ ही जाता है। जहां कपटाचार होता है, वहां उसके पीछे मान या अहंकार का प्रश्न जुड़ा रहता है और जहां मान या अहंकार होता है, उसके साथ क्रोध जुड़ा रहता है। राग के बिना द्वेष का और द्वेष के बिना राग का टिकाव नहीं है। इसी प्रकार, क्रोध का टिकाव अहंकार पर और अहंकार का टिकाव मायाचार पर, मायाचार का टिकाव लोभ पर निर्भर करता (11)