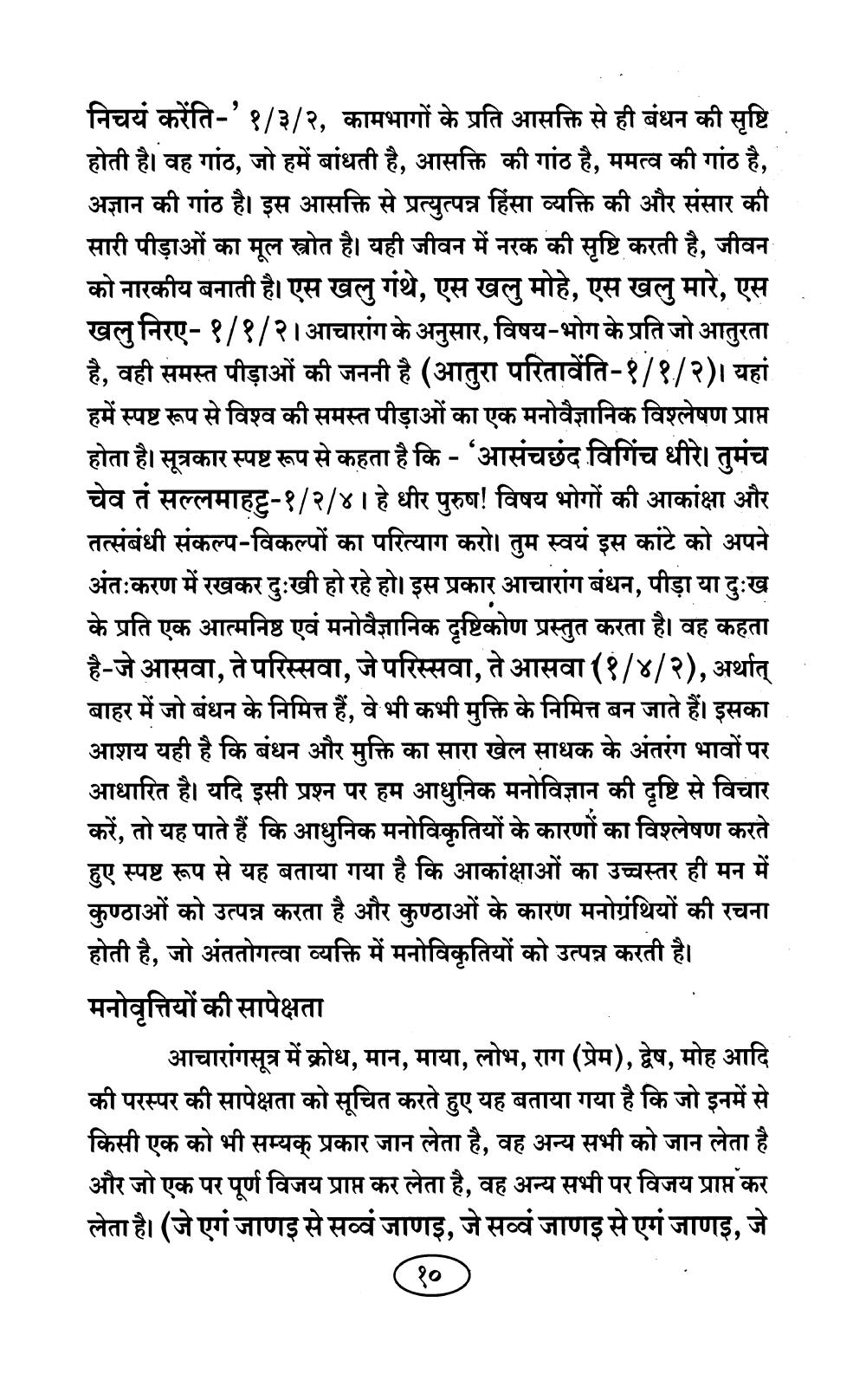________________ निचयं करेंति-' 1/3/2, कामभागों के प्रति आसक्ति से ही बंधन की सृष्टि होती है। वह गांठ, जो हमें बांधती है, आसक्ति की गांठ है, ममत्व की गांठ है, अज्ञान की गांठ है। इस आसक्ति से प्रत्युत्पन्न हिंसा व्यक्ति की और संसार की सारी पीड़ाओं का मूल स्त्रोत है। यही जीवन में नरक की सृष्टि करती है, जीवन को नारकीय बनाती है। एस खलु गंथे, एस खलु मोहे, एस खलु मारे, एस खलु निरए- १/१/२।आचारांग के अनुसार, विषय-भोग के प्रति जो आतुरता है, वही समस्त पीड़ाओं की जननी है (आतुरा परितावेंति-१/१/२)। यहां हमें स्पष्ट रूप से विश्व की समस्त पीड़ाओं का एक मनोवैज्ञानिक विश्लेषण प्राप्त होता है। सूत्रकार स्पष्ट रूप से कहता है कि - ‘आसंचछंद विगिंच धीरे। तुमंच चेव तं सल्लमाहटु-१/२/४ / हे धीर पुरुष! विषय भोगों की आकांक्षा और तत्संबंधी संकल्प-विकल्पों का परित्याग करो। तुम स्वयं इस कांटे को अपने अंतःकरण में रखकर दुःखी हो रहे हो। इस प्रकार आचारांग बंधन, पीड़ा या दुःख के प्रति एक आत्मनिष्ठ एवं मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। वह कहता है-जे आसवा, ते परिस्सवा, जे परिस्सवा, ते आसवा (1/4/2), अर्थात् बाहर में जो बंधन के निमित्त हैं, वे भी कभी मुक्ति के निमित्त बन जाते हैं। इसका आशय यही है कि बंधन और मुक्ति का सारा खेल साधक के अंतरंग भावों पर आधारित है। यदि इसी प्रश्न पर हम आधुनिक मनोविज्ञान की दृष्टि से विचार करें, तो यह पाते हैं कि आधुनिक मनोविकृतियों के कारणों का विश्लेषण करते हुए स्पष्ट रूप से यह बताया गया है कि आकांक्षाओं का उच्चस्तर ही मन में कुण्ठाओं को उत्पन्न करता है और कुण्ठाओं के कारण मनोग्रंथियों की रचना होती है, जो अंततोगत्वा व्यक्ति में मनोविकृतियों को उत्पन्न करती है। मनोवृत्तियों की सापेक्षता आचारांगसूत्र में क्रोध, मान, माया, लोभ, राग (प्रेम), द्वेष, मोह आदि की परस्पर की सापेक्षता को सूचित करते हुए यह बताया गया है कि जो इनमें से किसी एक को भी सम्यक् प्रकार जान लेता है, वह अन्य सभी को जान लेता है और जो एक पर पूर्ण विजय प्राप्त कर लेता है, वह अन्य सभी पर विजय प्राप्त कर लेता है। (जे एगंजाणइसे सव्वं जाणइ, जे सव्वं जाणइसे एगजाणइ, जे (10)