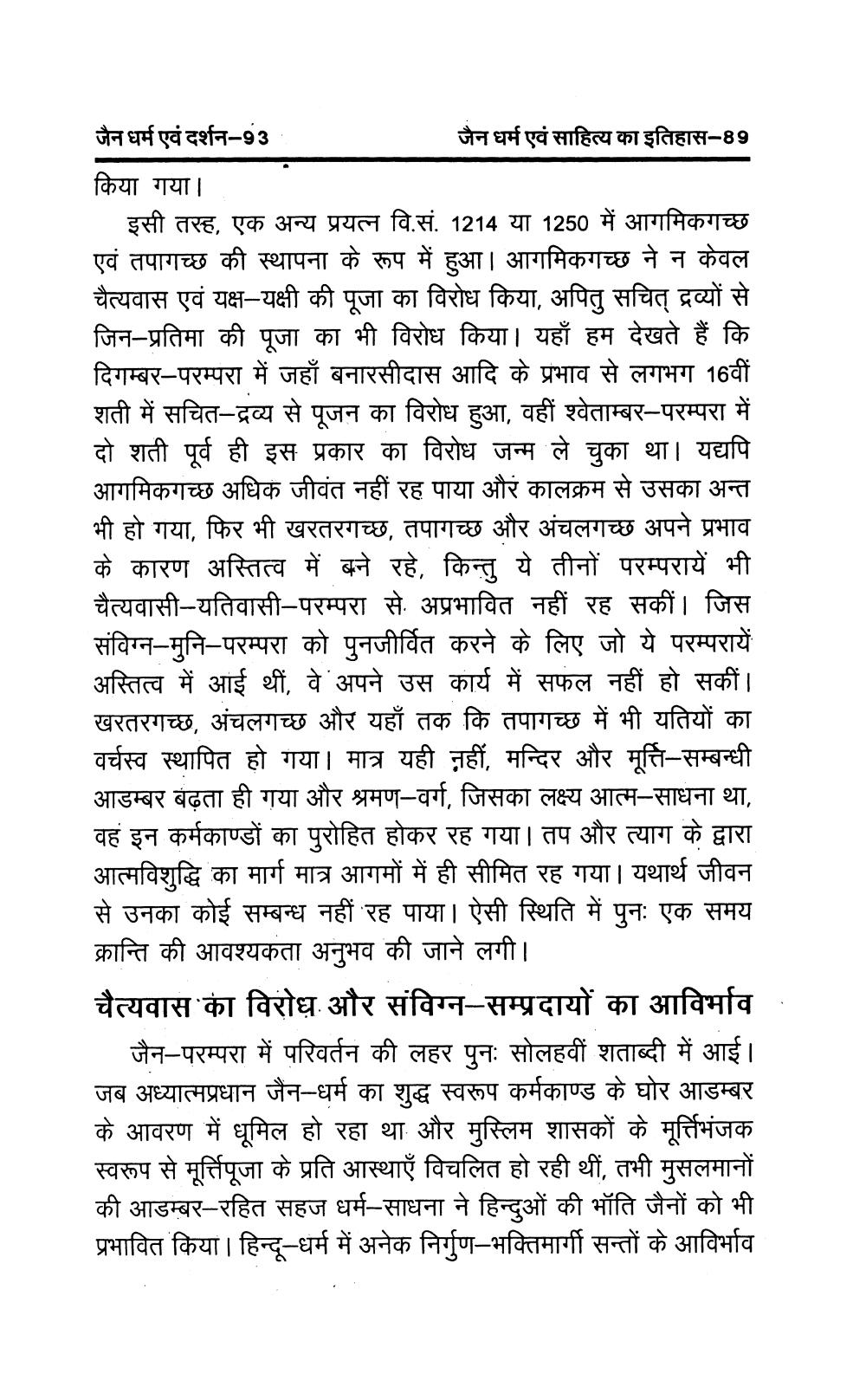________________ जैन धर्म एवं दर्शन-93 जैन धर्म एवं साहित्य का इतिहास-89 किया गया। __ इसी तरह, एक अन्य प्रयत्न वि.सं. 1214 या 1250 में आगमिकगच्छ एवं तपागच्छ की स्थापना के रूप में हुआ। आगमिकगच्छ ने न केवल चैत्यवास एवं यक्ष-यक्षी की पूजा का विरोध किया, अपितु सचित् द्रव्यों से जिन-प्रतिमा की पूजा का भी विरोध किया। यहाँ हम देखते हैं कि दिगम्बर-परम्परा में जहाँ बनारसीदास आदि के प्रभाव से लगभग 16वीं शती में सचित-द्रव्य से पूजन का विरोध हुआ, वहीं श्वेताम्बर-परम्परा में दो शती पूर्व ही इस प्रकार का विरोध जन्म ले चुका था। यद्यपि आगमिकगच्छ अधिक जीवंत नहीं रह पाया और कालक्रम से उसका अन्त भी हो गया, फिर भी खरतरगच्छ, तपागच्छ और अंचलगच्छ अपने प्रभाव के कारण अस्तित्व में बने रहे, किन्तु ये तीनों परम्परायें भी चैत्यवासी-यतिवासी-परम्परा से. अप्रभावित नहीं रह सकीं। जिस संविग्न-मुनि-परम्परा को पुनजीर्वित करने के लिए जो ये परम्परायें अस्तित्व में आई थीं, वे अपने उस कार्य में सफल नहीं हो सकीं। खरतरगच्छ, अंचलगच्छ और यहाँ तक कि तपागच्छ में भी यतियों का वर्चस्व स्थापित हो गया। मात्र यही नहीं, मन्दिर और मूर्ति-सम्बन्धी आडम्बर बढ़ता ही गया और श्रमण-वर्ग, जिसका लक्ष्य आत्म-साधना था, वह इन कर्मकाण्डों का पुरोहित होकर रह गया। तप और त्याग के द्वारा आत्मविशुद्धि का मार्ग मात्र आगमों में ही सीमित रह गया। यथार्थ जीवन से उनका कोई सम्बन्ध नहीं रह पाया। ऐसी स्थिति में पुनः एक समय क्रान्ति की आवश्यकता अनुभव की जाने लगी। चैत्यवास का विरोध और संविग्न-सम्प्रदायों का आविर्भाव . जैन-परम्परा में परिवर्तन की लहर पुनः सोलहवीं शताब्दी में आई। जब अध्यात्मप्रधान जैन-धर्म का शुद्ध स्वरूप कर्मकाण्ड के घोर आडम्बर के आवरण में धूमिल हो रहा था और मुस्लिम शासकों के मूर्तिभंजक स्वरूप से मूर्तिपूजा के प्रति आस्थाएँ विचलित हो रही थीं, तभी मुसलमानों की आडम्बर-रहित सहज धर्म-साधना ने हिन्दुओं की भॉति जैनों को भी प्रभावित किया। हिन्दू धर्म में अनेक निर्गुण भक्तिमार्गी सन्तों के आविर्भाव