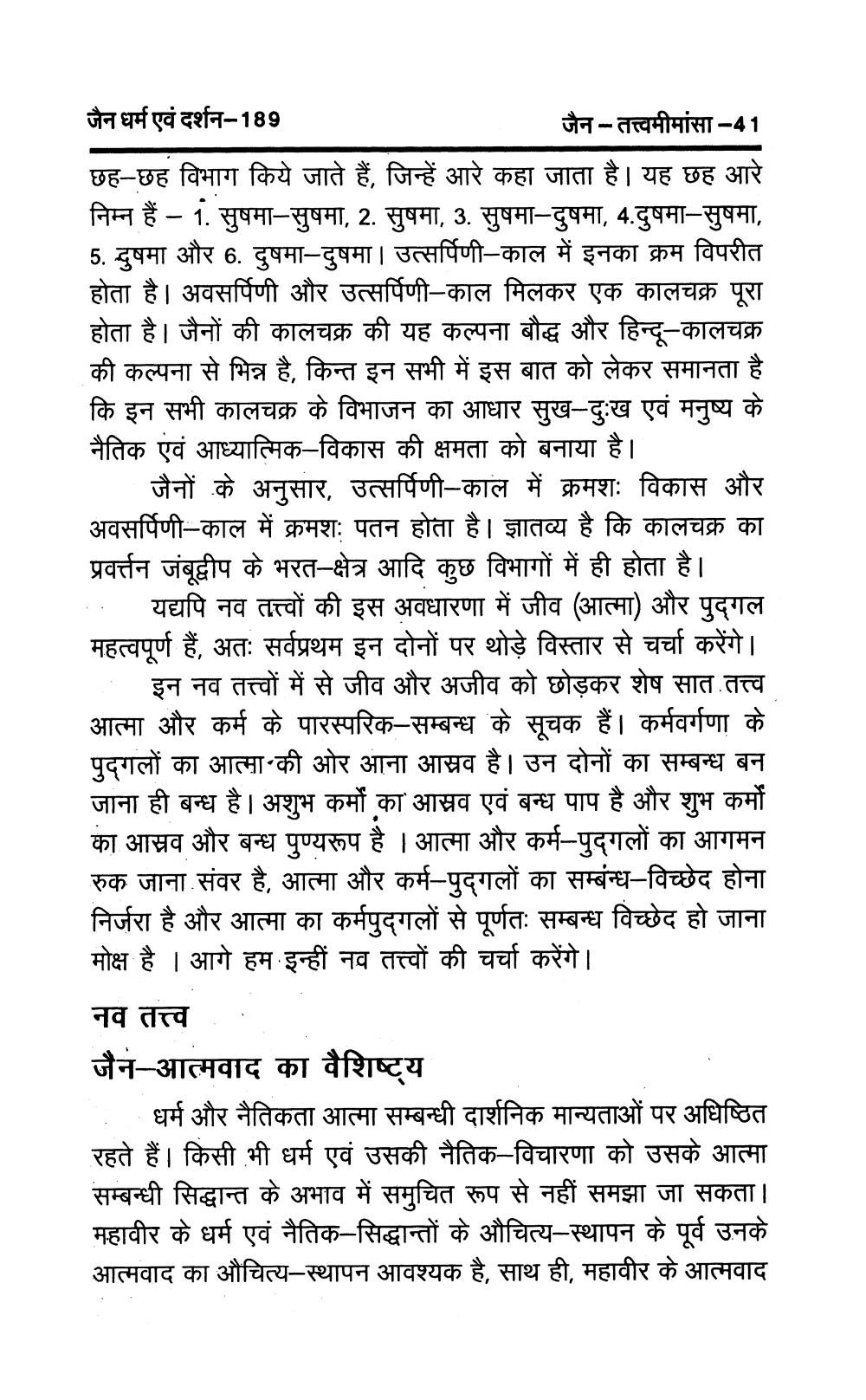________________ जैन धर्म एवं दर्शन-189 जैन- तत्त्वमीमांसा -41 छह-छह विभाग किये जाते हैं, जिन्हें आरे कहा जाता है। यह छह आरे निम्न हैं - 1. सुषमा-सुषमा, 2. सुषमा, 3. सुषमा-दुषमा, 4.दुषमा-सुषमा, 5. दुषमा और 6. दुषमा-दुषमा / उत्सर्पिणी-काल में इनका क्रम विपरीत होता है। अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी-काल मिलकर एक कालचक्र पूरा होता है। जैनों की कालचक्र की यह कल्पना बौद्ध और हिन्दू-कालचक्र की कल्पना से भिन्न है, किन्त इन सभी में इस बात को लेकर समानता है कि इन सभी कालचक्र के विभाजन का आधार सुख-दुःख एवं मनुष्य के नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास की क्षमता को बनाया है। ___जैनों के अनुसार, उत्सर्पिणी-काल में क्रमशः विकास और अवसर्पिणी-काल में क्रमश: पतन होता है। ज्ञातव्य है कि कालचक्र का प्रवर्तन जंबूद्वीप के भरत-क्षेत्र आदि कुछ विभागों में ही होता है। यद्यपि नव तत्त्वों की इस अवधारणा में जीव (आत्मा) और पुदगल महत्वपूर्ण हैं, अतः सर्वप्रथम इन दोनों पर थोड़े विस्तार से चर्चा करेंगे। इन नव तत्त्वों में से जीव और अजीव को छोड़कर शेष सात तत्त्व आत्मा और कर्म के पारस्परिक सम्बन्ध के सूचक हैं। कर्मवर्गणा के पुद्गलों का आत्मा की ओर आना आस्रव है। उन दोनों का सम्बन्ध बन जाना ही बन्ध है। अशुभ कर्मों का आस्रव एवं बन्ध पाप है और शुभ कर्मों का आस्रव और बन्ध पुण्यरूप है / आत्मा और कर्म-पुद्गलों का आगमन रुक जाना संवर है, आत्मा और कर्म-पुद्गलों का सम्बन्ध विच्छेद होना निर्जरा है और आत्मा का कर्मपुदगलों से पूर्णतः सम्बन्ध विच्छेद हो जाना मोक्ष है / आगे हम इन्हीं नव तत्त्वों की चर्चा करेंगे। नव तत्त्व . जैन-आत्मवाद का वैशिष्ट्य धर्म और नैतिकता आत्मा सम्बन्धी दार्शनिक मान्यताओं पर अधिष्ठित रहते हैं। किसी भी धर्म एवं उसकी नैतिक-विचारणा को उसके आत्मा सम्बन्धी सिद्धान्त के अभाव में समुचित रूप से नहीं समझा जा सकता। महावीर के धर्म एवं नैतिक-सिद्धान्तों के औचित्य-स्थापन के पूर्व उनके आत्मवाद का औचित्य-स्थापन आवश्यक है, साथ ही, महावीर के आत्मवाद