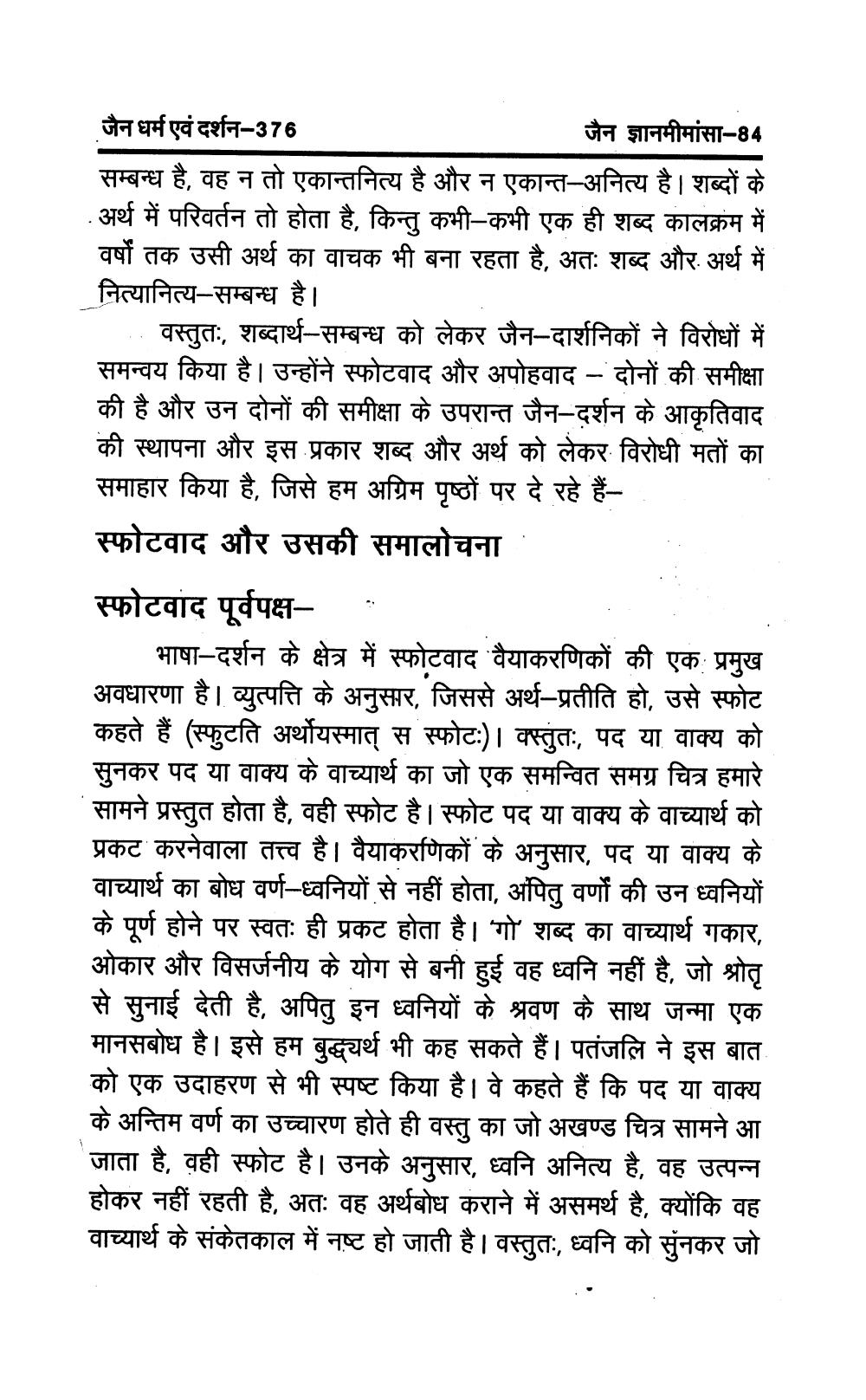________________ जैन धर्म एवं दर्शन-376 जैन ज्ञानमीमांसा-84 सम्बन्ध है, वह न तो एकान्तनित्य है और न एकान्त-अनित्य है। शब्दों के अर्थ में परिवर्तन तो होता है, किन्तु कभी-कभी एक ही शब्द कालक्रम में वर्षों तक उसी अर्थ का वाचक भी बना रहता है, अतः शब्द और. अर्थ में नित्यानित्य-सम्बन्ध है। .. वस्तुतः, शब्दार्थ-सम्बन्ध को लेकर जैन-दार्शनिकों ने विरोधों में समन्वय किया है। उन्होंने स्फोटवाद और अपोहवाद - दोनों की समीक्षा की है और उन दोनों की समीक्षा के उपरान्त जैन-दर्शन के आकृतिवाद की स्थापना और इस प्रकार शब्द और अर्थ को लेकर विरोधी मतों का समाहार किया है, जिसे हम अग्रिम पृष्ठों पर दे रहे हैंस्फोटवाद और उसकी समालोचना स्फोटवाद पूर्वपक्ष- . भाषा-दर्शन के क्षेत्र में स्फोटवाद वैयाकरणिकों की एक प्रमुख अवधारणा है। व्युत्पत्ति के अनुसार, जिससे अर्थ-प्रतीति हो, उसे स्फोट कहते हैं (स्फुटति अर्थोयस्मात् स स्फोट:)। वस्तुतः, पद या वाक्य को सुनकर पद या वाक्य के वाच्यार्थ का जो एक समन्वित समग्र चित्र हमारे सामने प्रस्तुत होता है, वही स्फोट है। स्फोट पद या वाक्य के वाच्यार्थ को प्रकट करनेवाला तत्त्व है। वैयाकरणिकों के अनुसार, पद या वाक्य के वाच्यार्थ का बोध वर्ण-ध्वनियों से नहीं होता, अपितु वर्णों की उन ध्वनियों के पूर्ण होने पर स्वतः ही प्रकट होता है। 'गो' शब्द का वाच्यार्थ गकार, ओकार और विसर्जनीय के योग से बनी हुई वह ध्वनि नहीं है, जो श्रोतृ से सुनाई देती है, अपितु इन ध्वनियों के श्रवण के साथ जन्मा एक मानसबोध है। इसे हम बुद्ध्यर्थ भी कह सकते हैं। पतंजलि ने इस बात को एक उदाहरण से भी स्पष्ट किया है। वे कहते हैं कि पद या वाक्य के अन्तिम वर्ण का उच्चारण होते ही वस्तु का जो अखण्ड चित्र सामने आ जाता है, वही स्फोट है। उनके अनुसार, ध्वनि अनित्य है, वह उत्पन्न होकर नहीं रहती है, अतः वह अर्थबोध कराने में असमर्थ है, क्योंकि वह वाच्यार्थ के संकेतकाल में नष्ट हो जाती है। वस्तुतः, ध्वनि को सुनकर जो