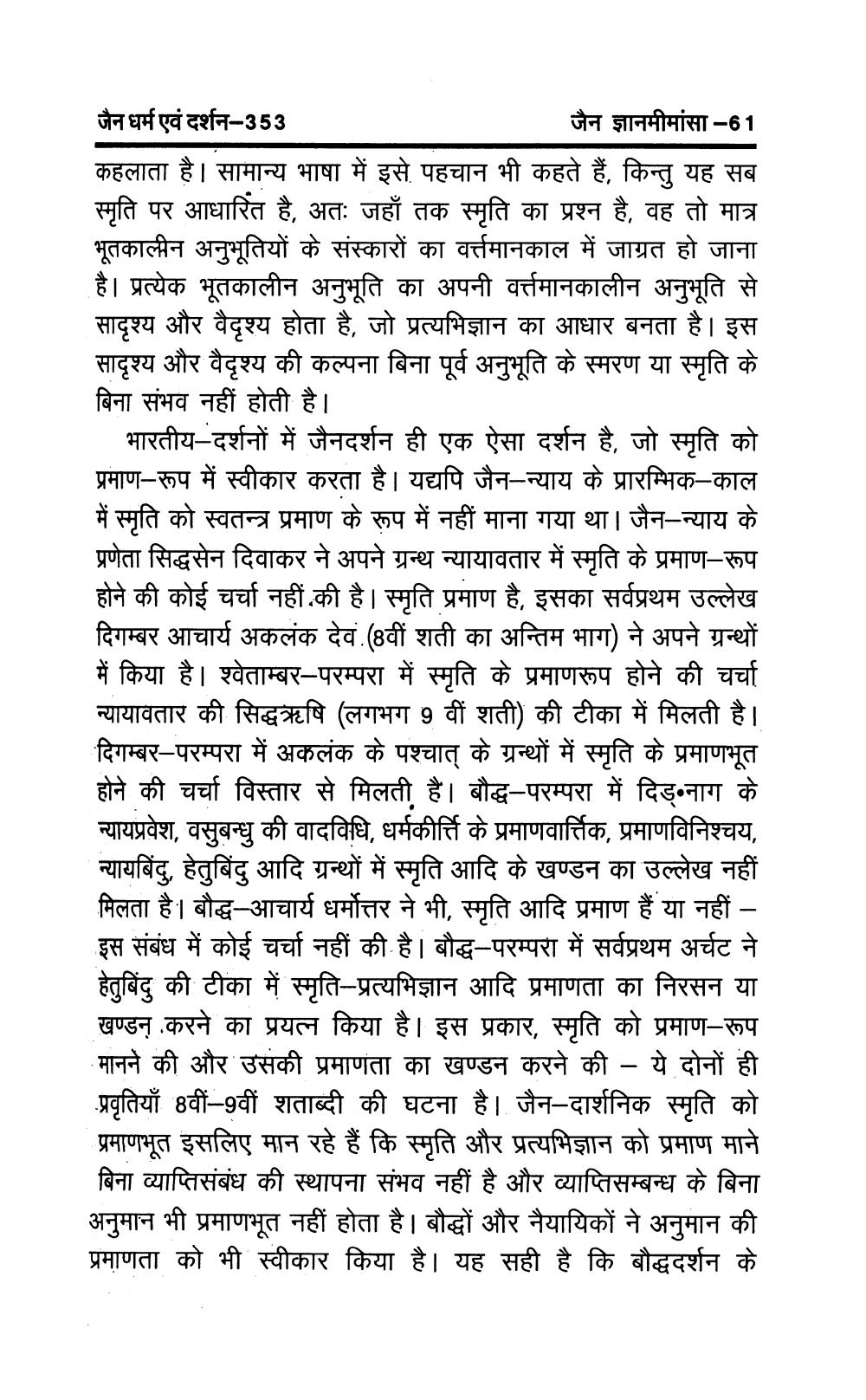________________ जैन धर्म एवं दर्शन-353 जैन ज्ञानमीमांसा-61 कहलाता है। सामान्य भाषा में इसे पहचान भी कहते हैं, किन्तु यह सब स्मृति पर आधारित है, अतः जहाँ तक स्मृति का प्रश्न है, वह तो मात्र भूतकालीन अनुभूतियों के संस्कारों का वर्तमानकाल में जाग्रत हो जाना है। प्रत्येक भूतकालीन अनुभूति का अपनी वर्तमानकालीन अनुभूति से सादृश्य और वैदृश्य होता है, जो प्रत्यभिज्ञान का आधार बनता है। इस सादृश्य और वैदृश्य की कल्पना बिना पूर्व अनुभूति के स्मरण या स्मृति के बिना संभव नहीं होती है। भारतीय-दर्शनों में जैनदर्शन ही एक ऐसा दर्शन है, जो स्मृति को प्रमाण-रूप में स्वीकार करता है। यद्यपि जैन-न्याय के प्रारम्भिक-काल में स्मृति को स्वतन्त्र प्रमाण के रूप में नहीं माना गया था। जैन-न्याय के प्रणेता सिद्धसेन दिवाकर ने अपने ग्रन्थ न्यायावतार में स्मृति के प्रमाण-रूप होने की कोई चर्चा नहीं की है। स्मृति प्रमाण है, इसका सर्वप्रथम उल्लेख दिगम्बर आचार्य अकलंक देवं.(8वीं शती का अन्तिम भाग) ने अपने ग्रन्थों में किया है। श्वेताम्बर-परम्परा में स्मृति के प्रमाणरूप होने की चर्चा न्यायावतार की सिद्धऋषि (लगभग 9 वीं शती) की टीका में मिलती है। दिगम्बर-परम्परा में अकलंक के पश्चात् के ग्रन्थों में स्मृति के प्रमाणभूत होने की चर्चा विस्तार से मिलती है। बौद्ध-परम्परा में दिड्-नाग के न्यायप्रवेश, वसुबन्धु की वादविधि, धर्मकीर्ति के प्रमाणवार्त्तिक, प्रमाणविनिश्चय, न्यायबिंदु, हेतुबिंदु आदि ग्रन्थों में स्मृति आदि के खण्डन का उल्लेख नहीं मिलता है। बौद्ध-आचार्य धर्मोत्तर ने भी, स्मृति आदि प्रमाण हैं या नहीं - इस संबंध में कोई चर्चा नहीं की है। बौद्ध-परम्परा में सर्वप्रथम अर्चट ने हेतुबिंदु की टीका में स्मृति-प्रत्यभिज्ञान आदि प्रमाणता का निरसन या खण्डन करने का प्रयत्न किया है। इस प्रकार, स्मृति को प्रमाण-रूप मानने की और उसकी प्रमाणता का खण्डन करने की - ये दोनों ही प्रवृतियाँ 8वीं-9वीं शताब्दी की घटना है। जैन-दार्शनिक स्मृति को प्रमाणभूत इसलिए मान रहे हैं कि स्मृति और प्रत्यभिज्ञान को प्रमाण माने बिना व्याप्तिसंबंध की स्थापना संभव नहीं है और व्याप्तिसम्बन्ध के बिना अनुमान भी प्रमाणभूत नहीं होता है। बौद्धों और नैयायिकों ने अनुमान की प्रमाणता को भी स्वीकार किया है। यह सही है कि बौद्धदर्शन के