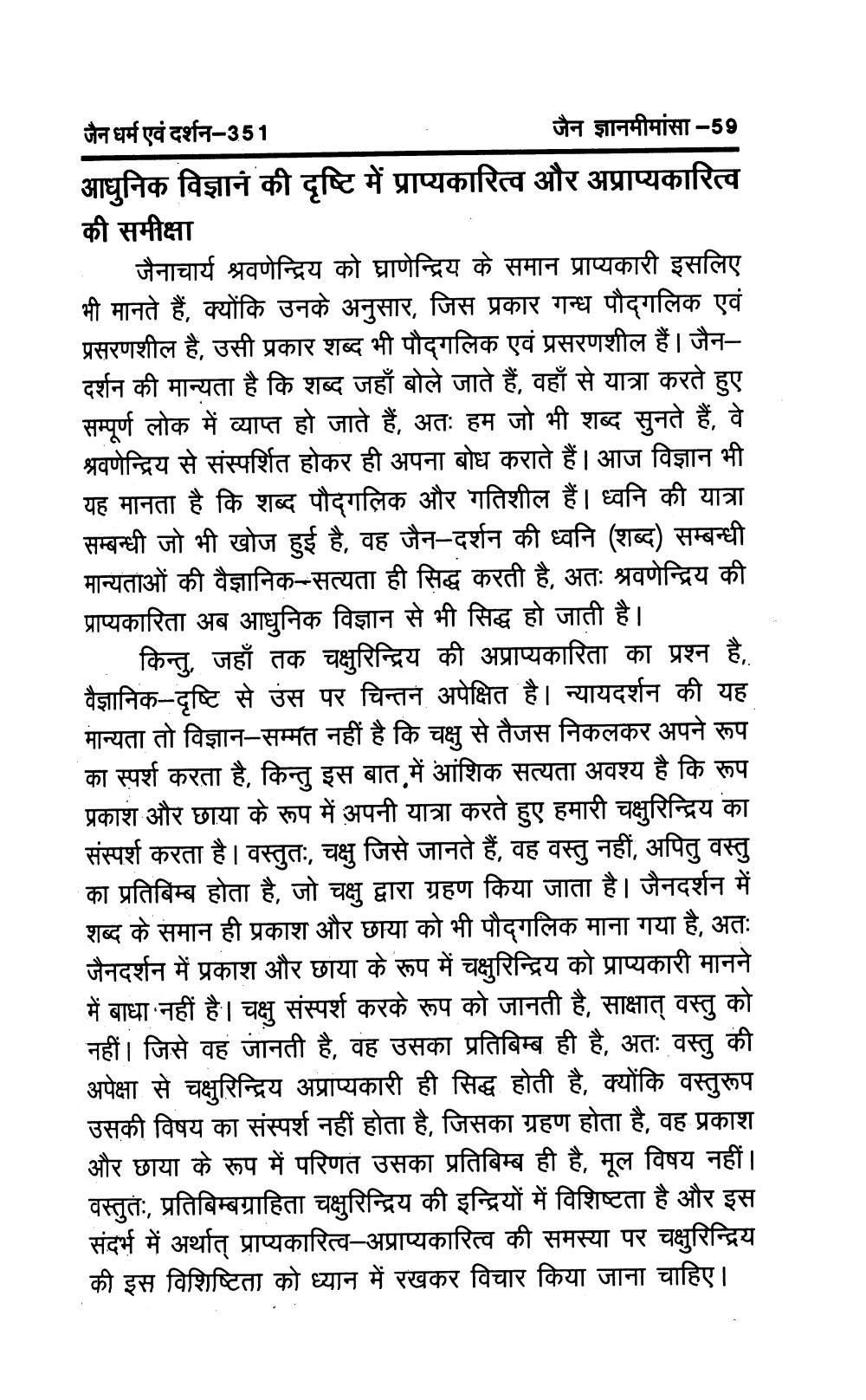________________ जैन धर्म एवं दर्शन-351 जैन ज्ञानमीमांसा-59 आधुनिक विज्ञान की दृष्टि में प्राप्यकारित्व और अप्राप्यकारित्व की समीक्षा जैनाचार्य श्रवणेन्द्रिय को घ्राणेन्द्रिय के समान प्राप्यकारी इसलिए भी मानते हैं, क्योंकि उनके अनुसार, जिस प्रकार गन्ध पौद्गलिक एवं प्रसरणशील है, उसी प्रकार शब्द भी पौद्गलिक एवं प्रसरणशील हैं। जैनदर्शन की मान्यता है कि शब्द जहाँ बोले जाते हैं, वहाँ से यात्रा करते हुए सम्पूर्ण लोक में व्याप्त हो जाते हैं, अतः हम जो भी शब्द सुनते हैं, वे श्रवणेन्द्रिय से संस्पर्शित होकर ही अपना बोध कराते हैं। आज विज्ञान भी यह मानता है कि शब्द पौद्गलिक और गतिशील हैं। ध्वनि की यात्रा सम्बन्धी जो भी खोज हुई है, वह जैन-दर्शन की ध्वनि (शब्द) सम्बन्धी मान्यताओं की वैज्ञानिक-सत्यता ही सिद्ध करती है, अतः श्रवणेन्द्रिय की प्राप्यकारिता अब आधुनिक विज्ञान से भी सिद्ध हो जाती है। . किन्तु, जहाँ तक चक्षुरिन्द्रिय की अप्राप्यकारिता का प्रश्न है, वैज्ञानिक-दृष्टि से उस पर चिन्तन अपेक्षित है। न्यायदर्शन की यह मान्यता तो विज्ञान-सम्मत नहीं है कि चक्षु से तैजस निकलकर अपने रूप का स्पर्श करता है, किन्तु इस बात में आंशिक सत्यता अवश्य है कि रूप प्रकाश और छाया के रूप में अपनी यात्रा करते हुए हमारी चक्षुरिन्द्रिय का संस्पर्श करता है। वस्तुतः, चक्षु जिसे जानते हैं, वह वस्तु नहीं, अपितु वस्तु का प्रतिबिम्ब होता है, जो चक्षु द्वारा ग्रहण किया जाता है। जैनदर्शन में शब्द के समान ही प्रकाश और छाया को भी पौद्गलिक माना गया है, अतः जैनदर्शन में प्रकाश और छाया के रूप में चक्षुरिन्द्रिय को प्राप्यकारी मानने में बाधा नहीं है। चक्षु संस्पर्श करके रूप को जानती है, साक्षात् वस्तु को नहीं। जिसे वह जानती है, वह उसका प्रतिबिम्ब ही है, अतः वस्तु की अपेक्षा से चक्षुरिन्द्रिय अप्राप्यकारी ही सिद्ध होती है, क्योंकि वस्तुरूप उसकी विषय का संस्पर्श नहीं होता है, जिसका ग्रहण होता है, वह प्रकाश और छाया के रूप में परिणत उसका प्रतिबिम्ब ही है, मूल विषय नहीं। वस्तुतः, प्रतिबिम्बग्राहिता चक्षुरिन्द्रिय की इन्द्रियों में विशिष्टता है और इस संदर्भ में अर्थात् प्राप्यकारित्व–अप्राप्यकारित्व की समस्या पर चक्षुरिन्द्रिय की इस विशिष्टिता को ध्यान में रखकर विचार किया जाना चाहिए।