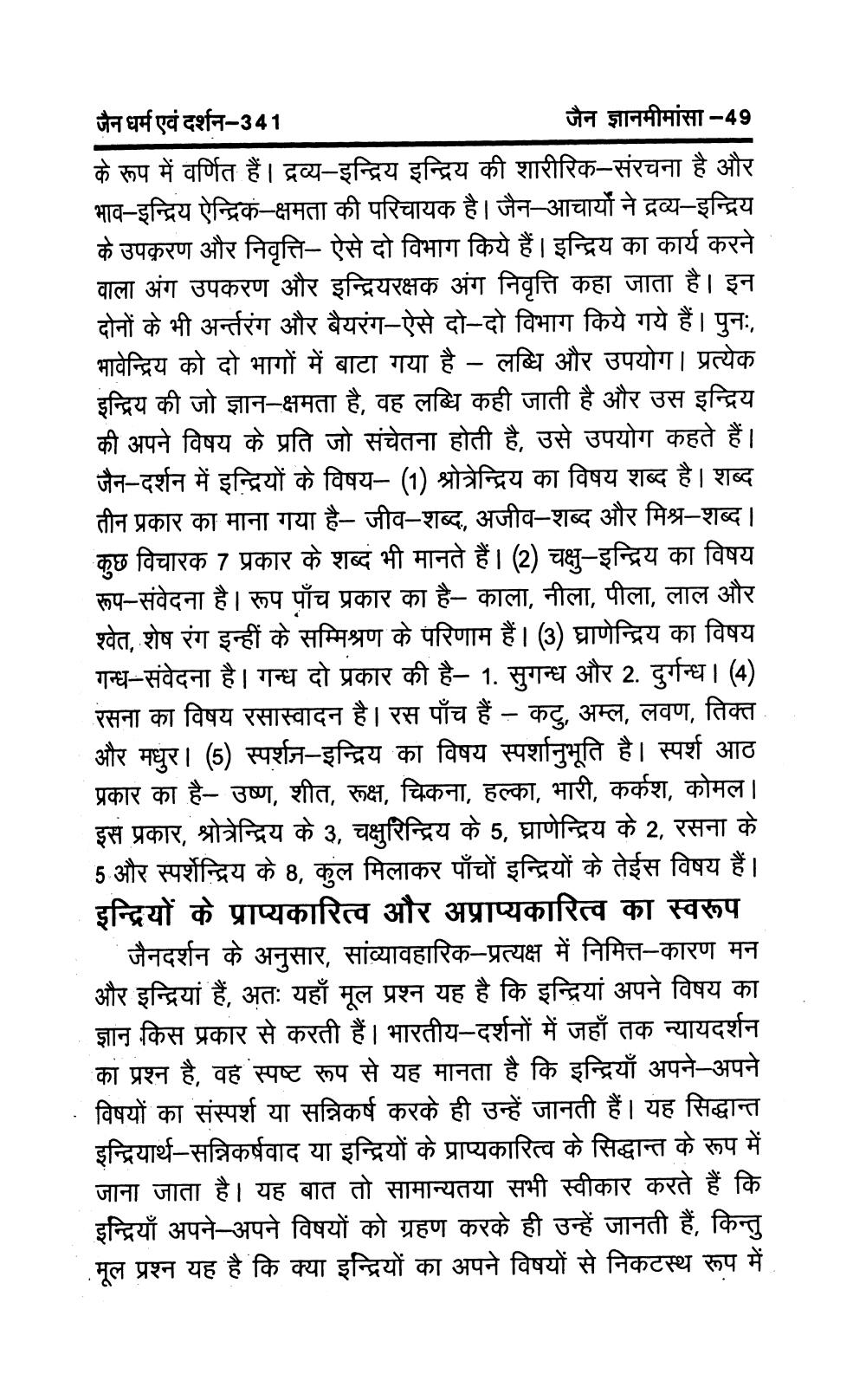________________ जैन धर्म एवं दर्शन-341 जैन ज्ञानमीमांसा -49 के रूप में वर्णित हैं। द्रव्य-इन्द्रिय इन्द्रिय की शारीरिक-संरचना है और भाव-इन्द्रिय ऐन्द्रिक क्षमता की परिचायक है। जैन आचार्यों ने द्रव्य-इन्द्रिय के उपकरण और निवृत्ति- ऐसे दो विभाग किये हैं। इन्द्रिय का कार्य करने वाला अंग उपकरण और इन्द्रियरक्षक अंग निवृत्ति कहा जाता है। इन दोनों के भी अतरंग और बैयरंग-ऐसे दो-दो विभाग किये गये हैं। पुनः, भावेन्द्रिय को दो भागों में बाटा गया है - लब्धि और उपयोग / प्रत्येक इन्द्रिय की जो ज्ञान-क्षमता है, वह लब्धि कही जाती है और उस इन्द्रिय की अपने विषय के प्रति जो संचेतना होती है, उसे उपयोग कहते हैं। जैन-दर्शन में इन्द्रियों के विषय- (1) श्रोत्रेन्द्रिय का विषय शब्द है। शब्द तीन प्रकार का माना गया है- जीव-शब्द, अजीव-शब्द और मिश्र-शब्द / कछ विचारक 7 प्रकार के शब्द भी मानते हैं। (2) चक्ष-इन्द्रिय का विषय रूप-संवेदना है। रूप पाँच प्रकार का है- काला, नीला, पीला, लाल और श्वेत, शेष रंग इन्हीं के सम्मिश्रण के परिणाम हैं। (3) घ्राणेन्द्रिय का विषय गन्ध-संवेदना है। गन्ध दो प्रकार की है- 1. सुगन्ध और 2. दुर्गन्ध / (4) रसना का विषय रसास्वादन है। रस पाँच हैं - कटु, अम्ल, लवण, तिक्त और मधुर। (5) स्पर्शन-इन्द्रिय का विषय स्पर्शानुभूति है। स्पर्श आठ प्रकार का है- उष्ण, शीत, रूक्ष, चिकना, हल्का, भारी, कर्कश, कोमल / इस प्रकार, श्रोत्रेन्द्रिय के 3, चक्षुरिन्द्रिय के 5, घ्राणेन्द्रिय के 2, रसना के 5 और स्पर्शेन्द्रिय के 8, कुल मिलाकर पाँचों इन्द्रियों के तेईस विषय हैं। इन्द्रियों के प्राप्यकारित्व और अप्राप्यकारित्व का स्वरूप जैनदर्शन के अनुसार, सांव्यावहारिक-प्रत्यक्ष में निमित्त-कारण मन और इन्द्रियां हैं, अतः यहाँ मूल प्रश्न यह है कि इन्द्रियां अपने विषय का ज्ञान किस प्रकार से करती हैं। भारतीय-दर्शनों में जहाँ तक न्यायदर्शन का प्रश्न है, वह स्पष्ट रूप से यह मानता है कि इन्द्रियाँ अपने-अपने विषयों का संस्पर्श या सन्निकर्ष करके ही उन्हें जानती हैं। यह सिद्धान्त इन्द्रियार्थ-सन्निकर्षवाद या इन्द्रियों के प्राप्यकारित्व के सिद्धान्त के रूप में जाना जाता है। यह बात तो सामान्यतया सभी स्वीकार करते हैं कि इन्द्रियाँ अपने-अपने विषयों को ग्रहण करके ही उन्हें जानती हैं, किन्तु मूल प्रश्न यह है कि क्या इन्द्रियों का अपने विषयों से निकटस्थ रूप में